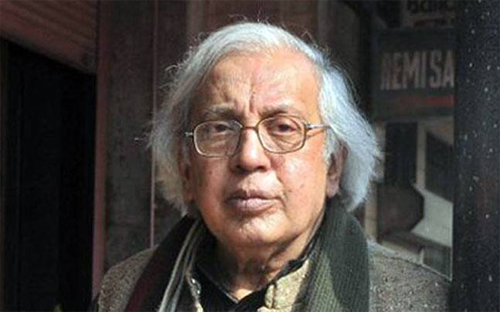जब बाज़ार, धर्म, राजनीति और मीडिया एक होकर लगातार नये ‘दूसरे’ गढ़ रहे हों, साहित्य और कलाएं ही वे जगहें हैं जहां किसी दूसरे को नष्ट करने का हिंसक उत्साह नहीं है।
केरल के कुछ कलाकार मित्रों ने याद दिलाया कि इस महीने हीरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम बरसाने के 75 वर्ष हो रहे हैं. उन्होंने भारत की सीमा पर चीनी घुसपैठ को भी ध्यान में रखते हुए व्हाइट रोज़ कला समूह द्वारा इस अवसर पर ‘ब्लू स्काई: शेडोज़ आव् हीरोशिमा’ कला-प्रदर्शनी आयोजित की है, ऑनलाइन. मुझसे ऑनलाइन वक्तव्य द्वारा उसका उद्घाटन करने का आग्रह किया. मुझसे पहले बोलते हुए केरल के राजनेता एमए बेबीने याद दिलाया कि जिन दो विमानों से बम बरसाये गये थे उनके नाम थे ‘ग्रेट आर्टिस्ट’ और ‘नैसेसरी ईविल’.
संयोगवश इसी समय हमारे पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध को भी 21 वर्ष पूरे हुए. मैंने यह कहने की कोशिश की कि दूसरे महायुद्ध के बाद, शीत युद्ध के भी बाद से संसार तरह-तरह से युद्धग्रस्त रहा है. कई तरह की बगावतें, सशस्त्र विद्रोह, सिविल युद्ध आदि आज भी लगातार हो रहे हैं. यह व्याप्ति इतनी है कि हम युद्ध शब्द का इस्तेमाल संज्ञा और रूपक की तरह करने के अभ्यस्त हो गये हैं. वर्तमान कोरोना प्रकोप के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसे युद्ध कहा जा रहा है और उससे निपटने-जूझने में लगे कर्मियों को कोरोना-योद्धा.
याद आता है कि प्राचीन और मध्यकालीन समय में युद्धरत सेनाएं अपने साथ कविता-संगीत-तमाशा आदि लेकर चलती थीं. याद यह भी करना चाहिये कि हमारे एक महाकाव्य ‘महाभारत’ में जो धर्मयुद्ध लड़ा गया वह अन्ततः, पाण्डवों की विजय के बावजूद, व्यर्थ सिद्ध हुआ. साहित्य और कलाओं में जहां युद्ध की वीरगाथाएं बखानी-गायीं-चित्रित की गयी हैं, वहां दूसरी ओर युद्ध की अन्ततः, विफलता और व्यर्थता का भी सत्यापन होता रहा है. दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व शान्ति के लिए एक बड़ा अभियान चला था जिसमें अनेक मूर्धन्य चिन्तकों, वैज्ञानिकों, लेखकों-कलाकारों आदि ने भाग लिया था.
यूनेस्को के एक प्रसिद्ध आप्तवाक्य में यह अवधारणा की गयी थी कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में उपजते और लड़े जाते हैं और उनसे मनुष्य को मुक्त कराने का प्रयत्न होना चाहिये. युद्ध प्रायः ‘दूसरों’ को नष्ट करने, उनसे ज़मीन और साधन छीनने, उनको पराजित करने के लिए किये जाते हैं. हमारे देश में, कोरोना प्रकोप की आड़ में, एक और अघोषित युद्ध चल रहा है: लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता, असहमति, न्याय की मांग, समता के आग्रह आदि के विरूद्ध जिसमें कई संवैधानिक संस्थाएं तक शामिल दीख पड़ रही हैं.
इस भयावह स्थिति में जब बाज़ार, धर्म, राजनीति, मीडिया आदि एक अनोखे गठबन्धन में लगातार नये ‘दूसरे’ गढ़, उन्हें बाधित-प्रताड़ित कर रहे हैं, साहित्य और कलाएं ही वे जगहें हैं जहां कोई ‘दूसरे’ नहीं हैं, किसी दूसरे को नष्ट करने का हिंसक उत्साह नहीं है. जहां नील नभ के नीचे, बिना भेदभाव के, हम स्वतंत्र, स्वायत्त, संवादरत महसूस कर सकते हैं.
हड़बड़ी का मौसम
इन दिनों काफ़ी लोगों के पास समय की कमी नहीं, अक्सर समय काटे नहीं कटता. कोरोना वायरस ने राजनीति छोड़कर सबको धीरज का पाठ सिखा दिया है. बस राजनीति में ही उठापटक की अधीरता कम नहीं हुई है. इसलिए कि काफ़ी समय है, फेसबुकिया लोग काफ़ी तेज़ी से इन दिनों तरह-तरह के झटपटिया आकलन में व्यस्त और सक्रिय हैं. सूक्तिपरक निर्णय और साहित्यिक फ़तवे जारी किये जा रहे हैं. इसका एक लाभ यह है कि ऐसे कई साहित्यकार चर्चा में हैं जिन पर अन्यथा विचार करने का विशेष अवसर न होता.
संयोगवश हिन्दी के दो मूर्धन्य और लोकप्रिय साहित्यकारों को इस समय इस आकस्मिक ध्यान की पात्रता मिली है – तुलसीदास और प्रेमचन्द. किसी कृति या किसी लेखक की किसी या कुछ रचनाओं को कूड़ा कहकर खारिज़ करने की हालिया शुरूआत नामवर सिंह ने की थी जब उन्होंने सुमित्रानन्दन पन्त की अधिकांश रचनाओं को कूड़ा कहा था. अब एक संपादक ने प्रेमचन्द की अधिकांश कहानियों को कूड़ा क़रार दिया है. तुलसीदास को दशकों पहले प्रगतिशीलों ने प्रतिक्रियावादी क़रार दिया था. बीच में उन्होंने भूल-सुधार किया. अब फिर तथाकथित जनधर्मी तुलसीदास को कुछ जुमलेबाज़ी कर अवमूल्यित करने की नयी कोशिश कर रहे हैं. इनमें से कोई भी बिना चुनौती के नहीं जाने दिया जा रहा है. इन सभी का प्रत्याख्यान भी सदलबल फ़ेसबुक पर हो रहा है.
यह नोट करना दिलचस्प है कि जो लेखक फ़ेसबुक पर इतने सक्रिय हैं और तरह-तरह के अवमूल्यन कर रहे हैं वे विधिवत् लिखकर इन स्थापनाओं को अधिकांशतः प्रमाण और तर्क के साथ, प्रस्तुत नहीं करते. साहित्य में एक वर्ग हमेशा ऐसा रहा है कि जो साहित्य को बल्कि आलोचना को अभिमत में घटाता रहा है. फ़ेसबुक की सुविधा ने इस वर्ग की सदस्य-संख्या कई गुना कर दी लगती है. कभी किसी मीर ने अपने को ही पगड़ी सम्हालने की हिदायत दी थी क्योंकि ‘शहर दिल्ली है’. अब लगता है कि हम सभी पगड़ी उछालने, उन पर कीचड़ फेंकने में एक तरह का नीच आनन्द पाते हैं. कइयों पर इसी कारण ध्यान जाता है वरना उनकी व्यापक परिदृश्य में कोई जगह या मौजूदगी नहीं है.
पर, यह भी कहना होगा कि हिन्दी में अपने बड़े लेखकों या कुछ कृतियों को लेकर जो रन्ध्रहीन भक्तिभाव है उसे भी आलोचनात्मक मूल्यांकन से उपजा नहीं कहा-माना जा सकता. सब कुछ आलोच्य है यह साहित्य के जनतन्त्र की बुनियादी मान्यता होती है और जो झटपटिया अवमूल्यन हो रहा है उसका यह आशय या संकेत है कि हिन्दी में अधिक निर्भीक आलोचना की ज़रूरत है, उसकी जगह होना चाहिये, उसे गम्भीरता से किया जाये और उतनी ही गम्भीरता से वह ज़ेरे-बहस हो. ऐसे वाद-विवाद-संवाद से साहित्य और आलोचना दोनों लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ते हैं.
रंगवितान
भारत भवन के अन्तर्गत मूर्धन्य रंगकर्मी बव कारन्त ने जो मध्यप्रदेश रंगमण्डल गठित किया था वह किसी राज्य द्वारा स्थापित पहली रिपर्टरी कम्पनी भर न थी. उसमें रंगप्रशिक्षण, रंग-व्यापार, रंगप्रयोग, रंगचिन्तन इन सभी पहलुओं को बहुत कल्पनाशील ढंग से नियोजित किया गया था. रंगमण्डल में बाक़ायदा रंगप्रशिक्षित कलाकारों के साथ लोक कलाकार भी शामिल किये गये थे. प्रसिद्ध निष्णात लोक कलाकारों को प्रशिक्षण देने बुलाया जाता था. लोक और आधुनिक का ऐसा लगातार संवाद और सहकार शायद ही इससे पहले हुआ था और बाद में कभी इस गहराई और निरन्तरता का कहीं और हुआ हो. इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ और विविध रंग-कर्मी प्रशिक्षण देने शायद ही किसी और रंगसंस्थान में आये होंगे जब कि रंगमण्डल प्रशिक्षण का संस्थान नहीं था. इनमें पीटर बुक, जान मार्टिन, बादल सरकार, रुद्रप्रसाद सेनगुप्त, श्यामा नन्द जालान, प्रसन्ना, इरशाद पंजतन आदि शामिल थे.
याद यह भी आता है कि कारन्त नहीं चाहते थे कि रंगमण्डल सिर्फ़ उनकी शैली में काम करे. उन्होंने बड़ी संख्या में अतिथि निर्देशक आमंत्रित किये जिन्होंने रंगमंडल के अन्तर्गत कई नाट्य प्रस्तुतियां तैयार कीं. तीन विदेशी निर्देशक पूर्वी जर्मनी, इंगलैण्ड और फ्रांस के आये थे. यह याद करने योग्य है कि इनमें से किसी को हिन्दी भाषा नहीं आती थी. फ्रिट्ज बेनेविट्ज ने शेक्सपीयर के कई नाटक हिन्दी में ‘बगरो बसन्त है’, ‘राजा लीयर’, ‘तो सम पुरुरव न मो सम नारी’ और बर्तोल्त ब्रेख़्त का ‘इन्साफ़ का घेरा’ तैयार कराये. ब्रिटिश जान मार्टिन ने रंगकार्यशाला तो ली ही, तीन ग्रीक दुखान्त’ – यूरीपिडीज़ और एस्किलस के, ‘पोलिस में हफ़ीजीनिया’, ‘ट्रोजन औरतें’ और ‘अग्मेनान’ निर्देशित किये. 1990 में फ्रांस के एक अत्यन्त प्रयोगशील रंगनिर्देशक जार्ज लवादों ने रासीन की क्लैसिक कृति ‘फ़ेद्रा’, कृष्ण बलदेव वेद के हिन्दी अनुवाद में, तैयार की. पूरी प्रस्तुति मुख्य मंच पर नहीं, ग्रीनरूम को रंगमंच में बदलकर की गयी थी.
हिन्दी की रंगसम्भावनाओं का इतना गहन अन्वेषण शायद ही पहले या बाद में कहीं और हुआ हो. कोई भारत भवन के पहले दशक का विस्तृत इतिहास लिखे तो पता चलेगा कि वहां कितना नवाचार अनेक कलाओं में पूरी निर्भीकता और कल्पनाशीलता के साथ किया गया था. कारन्त जैसा अथक रंगकर्मठ भी फिर दूसरा नहीं हुआ. न विभा मिश्र, द्वारका प्रसाद जैसे अभिनेता.
(लेखक आईएस अधिकारी रहे हैं , मध्य प्रदेश के संस्कृति सचिव के रूप में लोक संस्कृति, साहित्य और लोककला को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है)
साभार- https://satyagrah.scroll.in/ से