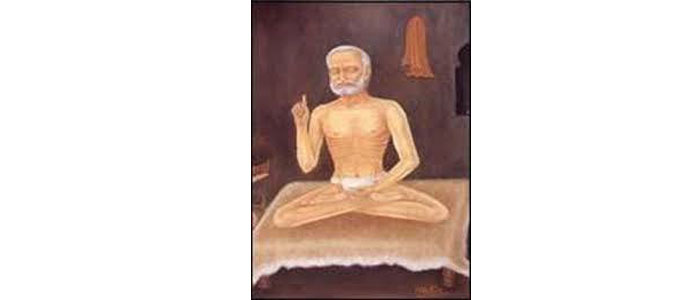स्वामी दस्यानंद सरस्वती जी को महर्षि बनाने वाले, विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में स्थान पाने वाले दण्डी गुरु विरजानंद जी सरस्वती जी का जन्म पंजाब के करतारपुर नामक स्थान के निकटवर्ती गाँव गंगापुर में संवत् १८३५ विक्रमी तदनुसार सन् १७७८ ईस्वी को हुआ| आपके पिता पंडित नारायणदत्त जी सारस्वत ब्राहमण थे| आप अभी मात्र केवल पांच वर्ष के ही थे, जब आप को चेचक का रोग हुआ और इस रोग ने आपकी ऑंखें छीन लीं| आपके पिताजी ने आपको घर पर ही संस्कृत की शिक्षा दी किन्तु अभी आप अल्पायु में ही थे जब माता और पिता दोनों ही आपका साथ छोड़कर सदा सदा के लिए विदा हो गए| आपके भाई तथा आपकी भावज दोनों का ही आपसे अच्छा व्यवहार नहीं था, इस कारण एक दिन आपने घर को त्याग दिया और पहले ऋषिकेश तथा फिर कनखल जा कर रहने लगे| कनखल में स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से आपने संन्यास की दिक्षा ली और अब से आपका नाम स्वामी विरजा नंद सरस्वति हो गया|
आपने कुछ काल कनखल में निवास किया और फिर काशी चले गए| काशी में रहते हुए आपने पंडित विद्याधर जी से उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त की| इसके तदन्तर आपने यहाँ से प्रस्थान किया और गया (बिहार)जाकर स्वयं के लिए अध्ययन और दूसरों के लिए अध्यापन क कार्य करने लगे| यहाँ भी आप अधिक समय नहीं टिक पाए और यहाँ से आगे क्रमश: कलकत्ता, सोरों, गडियाघाट आदि स्थानों पर जाकर निवास किया| यहां एक दिन आप मन्त्र पाठ का कार्य कर रहे थे कि वहां पधारे अलवर के राजा की दृष्टि आप पर पड गई| उन्होंने आपको अलवर चलने का आग्रह किया| आप इस शर्त पर अलवर जाने के लिए तैयार हुए कि महाराज प्रतिदिन स्वामी जी से संस्कृत की शिक्षा लेते रहेंगे और यदि किसी दिन वह संस्कृत पढ़ने के लिए किसी भी कारण नहीं आ पाए तो वह उसी दिन अलवर से विदा हो आवेंगे| महाराज को शीघ्र ही संस्कृत का ज्ञान हो सके, इसके लिए स्वामी जी ने “शब्द बोध” नामक पुस्तक की रचना की| एक दिन दरबारी राग रंग में अलवर नरेश ऐसे मस्त हुए कि संस्कृत की शिक्षा पाने के लिए वह गुरु जी की कुटिया में जाना भूल गए| फिर क्या था स्वामी जी ने लिए गए वचनों का पालन करते हुए उसी दिन अलवर का त्याग कर, वहां से प्रस्थान किया और पुन: सोरों के गडियाघाट जा विराजे|
गडियाघट रहते हुए स्वामी जी को एक भयंकर रोग ने आ घेरा किन्तु स्वामी जी शिष्यों ने अपनी अत्यधिक सेवा के बल से उन्हें मौत के मुंह से खींच पाने में सफलता प्राप्त की| स्वस्थ होने पर स्वामी जी ने यहाँ से भी प्रस्थान किया और यहाँ से मुरसान, भरतपुर आदि स्थानों से होते हुए मथुरा जा पहुंचे| मथुरा पहुँचने पर स्वामी जी ने एक पाठशाला आरम्भ की तथा इस पाठशाला के माध्यम से नियमित रूप से शिक्षा का दान करने लगे| उन दिनों काशी शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था किन्तु स्वामी जी के पढ़ाने की इतनी उत्तम विधि थी कि शिक्षार्थियों का एक अच्छा सा झुण्ड स्वामी जी की पाठशाला में लग गया और इस झुण्ड में काशी के शिक्षार्थी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे|
यह प्रज्ञाचक्षु संन्यासी देशभक्ति से लबालब भरा हुआ था तथा देश को स्वाधीन करवा कर एक बार फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाने के स्वप्न देखा करता था| वह यह भली प्रकार से जानते थे कि यदि राजा सुधर जावेगा तो उसकी प्रजा तो स्वयमेव ही राजा की अनुगामी होने के कारण सुधर जावेगी| इस दृष्टि को सामने रखते हुए आपने राजाओं की उत्तम शिक्षा की और विशेष ध्यान दिया| आपको मथुरा में रहते हुए शास्त्रार्थ की चुनौती भी मिली, इसे आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया किन्तु यह शास्त्रार्थ किसी निर्णय पर न पहुँच कर कुटिलता की भेंट चढ़ गया|
स्वामी जी की मान्यता के अनुसार अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य नामक यह दो ग्रन्थ ही आर्ष ग्रन्थ थे, जिन के द्वारा उत्तम शिक्षा प्राप्त की जा सकती है| इसं दो के अतिरिक्त अन्य सब ग्रंथों को स्वामी जी धूर्त लोगों की कृति मानते थे| उनका मानना था कि यदि धूर्तों के लिखे ग्रंथों को शिक्षा का आधार बनाया जाए तो इस शिक्षा से धूर्त ही पैदा होंगे| इसलिए स्वामी जी आर्ष ग्रंथों का ही प्रचार व प्रसार करते थे और इन ग्रंधों के माध्यम से ही अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे|
सन् १८५७ ईस्वी में भारत को स्वाधीन करवाने के लिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम से अंग्रेज के साथ एक युद्ध लड़ा गया| इस युद्ध के जनक अर्थात् इस युद्ध की भूमिका तैयार करने वाले आप ही थे| इस योजना को बनाने के लिए आपको संन्यास देने वाले आपके संन्यास गुरु स्वामी पूर्णानंद जी का आदेश हुआ था| इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए आपके सब शिष्य, जो शासक वर्ग से आते थे, ने अमल करते हुए विद्रोह अथवा यूं कहें कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए झंडा उठा लिया|
स्वामी जी एक धर्म सभा बुलाने के इच्छुक थे, जिस के माध्यम से पूरे देश को एक संगठन में बांधा जा सके किन्तु जयपुर के राजा रामसिंह के इस सम्बन्ध में रूचि न लेने के कारण यह सभा संभव न हो सकी| स्वामी जी द्वारा दी जा रही सर्वोत्तम शिक्षा के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फ़ैल गई किन्तु उन्हें अब तक भी आर्ष ग्रंथों का प्रसार करने वाला कोई शिष्य नहीं मिला था, जिसकी उन्हें निरंतर प्रतीक्षा थी| इन्हीं दिनों परमात्मा के आदेश से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ( जो आपके गुरु स्वामी पूर्णानंद जी से ही संन्यास लेकर , उन्ही के आदेश के कारण आपके पास आये थे) आपको शिष्य स्वरूप मिले|
सन् १९१७ विक्रमी तदनुसार १८६० ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुरु जी की इच्छा को शिरोधार्य करते हुए उनकी ही छत्रछाया में आर्ष ग्रंथों का अध्ययन आरम्भ किया| शिष्य की लगन ने गुरु का उत्साह भी बढ़ा दिया, परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी अपने सरीखा अद्वितीय विद्वान् बना दिया| अब उन्हें वह सच्चा शिष्य मिल गया था, जिस पर वह सब प्रकार से विश्वास कर सकते थे| अत: उन्होंने अपना वह बोझ, जो उन्होंने वेद धर्म के प्रचार और देश को स्वाधीन करवाने की इच्छा के रूप में अपने कंधों पर ले रखा था, को उतार कर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कन्धों पर लाद दिया| इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी अथवा यूँ कहें कि अपना उत्ताराधिकारी बना कर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई| वह इस बात से प्रसन्न थे कि जैसे शिष्य के लिए वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वैसा शिष्य दयानंद के रूप में उन्हें जीवन के अंतिम क्षणों में मिल ही गया|
अश्विन वदी त्रयोदशी संवत् १९२५ विक्रमी तदनुसार सितम्बर सन १८६८ ईस्वी को, सोमवार के नाम से जाना गया, आप सब प्रकार से निश्चिन्त होकर, अपने सब उत्तरदायित्व स्वामी दयानद सरस्वती जी के कन्धों पर छोड़ इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए| आपके देहावसान का समाचार सुनते ही स्वामी दयानद सरस्वती जी के मुख से यह शब्द निकले “ आज व्याकरण का सूर्य आस्त हो गया है”| गुरु विरजा नन्द जी का जीवन आर्ष ग्रंथों के प्रचार तथा प्रसार को समर्पित रहा| इस मार्ग को ही स्वामी दयानंद जी आजीवन अपनाए रहे| जब तक यह सृष्टि रहेगी, स्वामी विरजानंद दण्डी जी का नाम सूर्य के समान चमकते हुए संसार को आर्ष ज्ञान से प्रकाषित करता रहेगा|
डॉ. अशोक आर्य
पाकेट १/६१ रामप्रस्थ ग्रीन से.७ वैशाली
२०१०१२ गाजियाबाद उ.प्र.भारत
चलभाष ९३५४८४५४२६ व्ह्तास एप्प ९७१८५२८०६८
E Mail ashokarya1944@rediffmail.com