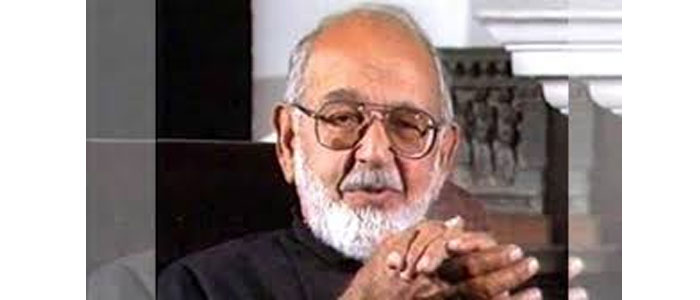भारत की आत्मा सनातन है, भारतीयता केवल एक भौगोलिक परिवृत्ति की छाप नहीं, एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण है, जो भारतीय को सारे संसार से पृथक करता है। भारतीयता मानवीयता का निचोड़ है, उस की हृदय मणि है, उस का शिर सावतंस है, उस के नाक का बेसर है..
आप कहते चले जाइए, सो श्रोताओं में से एक को- नहीं, आप को हजार श्रोता मिलें तो हजार में से एक को छोड़ कर बाकी सब आप के शब्द गट-गट पी जाएँगे, एक हल्की सी तन्द्रा, एक सुखालस पिनक सी उन पर छा जावेगी, कितना अच्छा है यह सुनना कि भारतीयता मानवीयता के नाक का बेसर है, क्योंकि निस्संदेह भारतीयता के नाक का बेसर मैं स्वयं हूँ..
तब वह जो में एक-या हजार में एक है, उसे पकड़ लीजिए उसे इंगित कर के बाकी सभा से कहिए, ‘देखिए, यह आदमी शाश्वत भारतीयता को नहीं जानता मानता। अपनी संस्कृति से, मानवीयता के श्रेष्ठ दाय से, यह अपरिचित है, भारत की सनातन आत्मा से इस ने अपने को तोड़ लिया है…’ सब लोग उस की ओर दया भरी दृष्टि से देखने लगेंगे – अरे, बिचारा, अभागा, अज्ञान-मोहान्धकारग्रस्त कहीं का। और कुछ कदाचित् अवहेलना और हिकारत की दृष्टि से उसे देख कर मुँह फेर लेंगे कमबख्त परंपरा द्वेषी, परमुखापेक्षी, सदियों की गुलामी से इस की आत्मा गुलाम हो गई है।
ठीक इस मौके पर आप मुड़ कर उन नौ सौ निन्यानबे श्रद्धालु आत्मरत श्रोताओं से वह प्रश्न पूछ बैठें जो उन्हें पहले ही आप से पूछना चाहिए था कि भारतीय आखिर है क्या? भारत की आत्मा का वैशिष्टय किस में है? तो वे अचकचा जावेंगे। फिर खिसियानी सी हँसी हँस देंगे। हें-हें, यह भी भला कोई पूछने की बात है, आप तो मजाक करते हैं, भारत की आत्मा माने हाँ हाँ, सदियों से सब जानते हैं, भारत की आत्मा माने भारत की आत्मा। हाँ-हाँ वहीं तो।
हाँ-हाँ, वही तो। सदियों से सब जानते हैं तभी अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी सांस्कृतिक परंपरा से, किसी भी जाति की व्यक्तिगत और समूहगत रचनात्मक प्रवृत्तियों के समन्वय से उत्पन्न गति से लाभ उठाने के लिए उसे नया जीवन देने के लिए उस से अनुप्राणित हो कर आगे बढ़ने के लिए, आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रश्न पूछे, उस का उत्तर अपने में पावे, उस से जो भी गत्यात्मक प्रेरणा मिल सकती हो, उसे आत्मसात करे। क्योंकि ऐतिहासिक परंपरा कोई पोटली बाँध कर रखा हुआ पाथेय नहीं है जिसे उठा कर हम चल निकलें। वह रस है जिसे हम बूँद बूँद अपने में संचय करते हैं- या नहीं करते, कोरे रह जाते है।
· और प्रश्न पूछने की आवश्यकता का सब से बड़ा प्रमाण तो वह स्वीकारात्मक औदासीन्य ही है जो इस प्रश्न पर हमें मिलता है। उसे लक्ष्य करते हुए समाकलीन भारतीय मानस की पड़ताल करें और यहाँ भारतीय मानस से अभिप्राय केवल उस के इने गिने मेधावियों का मानस नहीं, लोकमानस है, प्राकृत जन का भी मानस है तो हम कह सकते हैं कि भारतीयता का पहला लक्षण या गुण है सनातन की भावना, काल की भावना, काल के आदि हीन अंत हीन प्रवाह की भावना और काल केवल वैज्ञानिक दृष्टि से क्षणों की सरणी नहीं, काल हम से, भारतीय जाति से, सम्बद्ध विशिष्ट और निजी क्षणों की सरणी के रूप में। इस के प्रभावों की पड़ताल की जाए, इस से पहले इस की पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि और दौड़ा ली जाए। कलियुग कितने वर्षों का होगा, यह शास्त्र बताते हैं। इसी प्रकार द्वापर, त्रेता और सतयुगों के काल हैं। यों तो इतना ही मानव काल कल्पना की शक्ति से परे चला जाता है। लेकिन आगे जब हम जानते हैं कि यह ब्रह्मा का केवल एक पल है, और फिर हिसाब लगाते हैं कि ब्रह्मा का दिवस और वर्ष कैसा होगा तब हम यथार्थता के क्षेत्र से बिलकुल परे चले जाते हैं। ऋषि-मुनि साठ हजार वर्ष तक तपस्या कर लेते थे। आज साठ वर्ष को मानवीय आयु की औसत मान कर उस से हजार गुनी अवधि की कल्पना, खैर, की भी जा सकती है, लेकिन देवताओं की आयु गणना करने जाते ही फिर यथार्थता का आँचल छूट जाता है। इस प्रकार सनातन के बोध तक पहुँचते-पहुँचते हम काल की यथार्थता का बोध खो देते हैं। सनातन की भावना लंबी काल परंपरा की भावना नहीं, काल की अयथार्थता की भावना है।
· यों तो पश्चिम की युवा संस्कृतियों में पले हुए लोग प्राय: पूर्व की प्राचीन संस्कृतियों की चर्चा करते हुए ‘संस्कृति के भार’ की चर्चा किया करते हैं – बहुत लंबी सांस्कृतिक परंपरा का एक बोझ उस परंपरा में रहने वालों पर हो जाता है, जिस से वह समकालीन प्रतयेक प्रवृत्ति या घटना को सुदूर अतीत को कसौटी पर परखने लगते हैं, सामने न देख कर पीछे देखते हैं और एक प्रकार के नियतिवादी हो जाते हैं। भारत के बारे में और इसी प्रकार मिस्त्र आदि के बारे में पाश्चात्य अध्येताओं ने ऐसे विचार प्रकट किये हैं। लेकिन अगर कुछ सहस्त्र वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा का ही इतना बोझ होसकता है, तो कल्पना कीजिए उस बोझ का, जो ब्रह्मा के एक युग की उद्भावना करने से पड़ता होगा। यद्यपि यह हम कह चुके कि ब्रह्मा का युग हमारी उद्भावना की पकड़ से बाहर की चीज़ है- वह काल्पनिक यथार्थता भी नहीं हो सकती।
‘भारतीयता’ का दूसरा विशिष्ट गुण है स्वीकार की भावना। किसी हद तक यह पहली विशेषता का परिणाम ही है। हिंदू देवताओं को छोड़ कर किसी के दिन और वर्ष इतने लम्बे नहीं होते। यों अमर तो सभी देवता होते है, लेकिन दूसरी के देवताओं के दिन-रात साधारण मानवीय दिन रात ही होते हैं, और उन की जीवनचर्या की कल्पना हमें अपने यथार्थ काल से परे नहीं ले जाती। लेकिन भारत के देवताओं के जीवन की कल्पना ऐहिक काल की भावना को मिटा कर ही की जाती है। और जब हमारा काल ही यथार्थ नहीं रहता, तब उस काल में होने वाले व्यापार भी अयथार्थ हो जाते हैं। हमारे यथार्थ दु:ख क्लेश, हमारी यथार्थ आशा-आकांक्षा, मानव के उद्योग परिचय मानवी व्यापार मात्र अयथार्थ हो जाते हैं। और यथार्थता से इस स्खलन का प्रभाव मानवी संबंधों पर भी पड़ता है। हमारे लिए हमारे पड़ोसी भी यथार्थ नहीं रहते, बल्कि किसी हद तक हम स्वयं ही अपने लिए यथार्थ नहीं रहते क्योंकि जिस ब्रह्मा के एक निमिष-पात में हमारे कल्पांत विलीन हो जाते हैं, उस के सामने क्या है हमारा क्षुद्र जीवन हमारी अपेक्षा में एक रोग कीटाणु का जीवन जितना नगण्य है, उस से भी तो अधिक नगण्य हम हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा के ‘निमिष-रात’ की हम जब कल्पना करते हैं, तो ब्रह्मा की मानवाकार ही कल्पना करते हैं अर्थात एक कल्पित या कल्पनातीत अतिमानव ब्रह्मा के सामने यथार्थ ऐहिक मानव न कुछ के बराबर है। अपनी इस नगण्यता से ही स्वीकार की भावना उत्पन्न होती है दुख के प्रति स्वीकार, दैन्य के प्रति स्वीकार, अत्याचार के प्रति स्वीकार, उत्पीड़न के प्रति स्वीकार यहाँ तक कि दासता के प्रति स्वीकार, वह दासता दैहिक हो या मानसिक।
इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ‘भारतीयता’ के मूल में जो भावना या भावनाएँ है, उन से हमें मानवीय अस्तित्व की नगण्यता और जीवन के प्रति अवज्ञा का पाठ मिलता है। यह परिणाम चौंकाने वाला है। लेकिन स्वीकारी सहज चौंकता भी तो नहीं। और न चौंकने के लिए उस के पास और भी सहारे हैं-इस अस्तित्व से परे परलोक के किसी चमकीले अस्तित्व का, और जीवन के प्रति अवज्ञा के उत्तर में जीव दया के भारतीय आदर्श का। लेकिन जिस तरह चिरन्तन काल की भावना ने हमारे यथार्थ काल के बोध को मिटाया है, उसी प्रकार व्यापक जीव दया ने जीवित व्यष्टि के प्रति करुणा को भी मिटा दिया है, जीवदयावादी जीव-मात्र के प्रति दया रखता हुआ किसी भी जीव-मानव या मानवेतर का कष्ट मजे में देखता चलता है।
मैं परंपराद्रोही नहीं हूँ, न भारतद्वेषी ही हूँ। न ही मैं निराशावादी हूँ। और तात्कालिक लाभ या उपयोगिता या सफलता के नाम पर नैतिक मूल्यों की उपेक्षा मुझे कभी अभीष्ट नहीं रही मेरा आग्रह सदैव अवसरवाद के विरुद्ध और नैतिक मूल्य की रक्षा का रहा है। मुझे यही कहना है कि भारतीयता का जो रूप हमारी तत्संबंधी सहज स्वीकृति हमारे सनातन स्वीकार। में लक्षित होता है, उस कीमूल भावनाएँ स्वयं जड़ है और जाड्य उत्पन्न करने वाली हैं, और उस से परिव्याप्त संस्कृति (मैं ‘अनुप्राणित’ कहने लगा था, पर अनुप्राणित तो तब हो जब प्राण हों, जड़ता से तो विजडित ही होगी।) गतिहीन, स्थितिशील और अगतिवादी या प्रगतिवादी ही होगी।
इस से यह परिणाम नहीं निकलता कि भारतीय संस्कृति अग्राहा है, या कि भारतीय परंपरा त्याज्य है। परिणाम तक तो यह निकलता है कि उस के संबंध में हमारी धारणाएँ भ्रांत हैं और त्याज्य हैं। दूसरे यह भी परिणाम निकलता है कि जिसे हम भारत की आत्मा कहते हैं, वह वास्तव में आत्मा और अनात्म का, जीवित और जड़ का एक पुंज है, जिस की परीक्षा की आवश्यकता है, परीक्षा कर के जड़ को अलग रख देना होगा चाहे पुरातत्व संग्रहालय में ही ओर जीवित को आगे बढ़ाना होगा। और तीसरा परिणाम यह भी निकलता है कि आज बहुधा भारतीय संस्कृति के जड़ तत्वों को ही भारतीयता माना जाता है। कुछ लोग भारतीयता के समर्थन के नाम पर निरी जड़ता का समर्थन करते हैं। कुछ दूसरे जड़ता के विरोध के नाम पर संस्कृति से ही इनकार करना चाहते हैं।
हमें चाहिए वह बेलाग, सचेत, स्वाधीन जिज्ञासा जो परिवृत्ति में घिरी हुई भी आगे देखे। जो अपने देश में रह कर भी आगे देखे, आगे दूसरे देशों को नहीं, हम से आरंभ होने वाली आगे की दिशा को, आगे को। जो अपने काल में रह कर भी आगे देखे, न इधर अनादि को, न उधर अनन्त को, वरन् हम से आगे के उस काल को जो हमारे काल से प्रसूत हैं और जिस के हम स्रष्टा हैं। वह अपरिबद्ध जिज्ञासा भारतीयता है कि नहीं, इस पर विद्वान लोग बहस कर सकते हैं, मैं असन्दिग्ध भाव से इतना जानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वह भारतीयता को कल्याणकर बना सकती है।
(स्व. सच्चिनांद हीरानंत वात्सायन अज्ञेय हिंदी के जाने माने लेखक थे और विभिन्न विधाओँ पर उन्होंने कई पुस्तकें, लेख आदि लिखे)