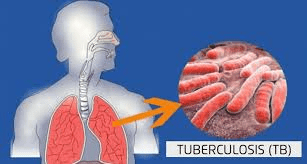संभल ही नहीं… जहाँ-जहाँ डाला डेरा, वहाँ-वहाँ मुस्लिम लगाते हैं ‘मेला’: हिंदू घृणा से सैयद सालार बना ‘गाजी’, जानिए क्यों हो रही बहराइच के ‘जेठा मेला’ को भी बंद करने की माँग
किताब में आगे लिखा है कि एक दिन पृथ्वीराज चौहान के घराने का एक राजकुमार ने उस लड़की को देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गया। उसकी बेटी भी राजकुमार से आकर्षित हो गई। इससे सैयद पचासे गुस्सा हो गया और गजनी जाकर महमूद गजनवी से सारी बात बताई। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपनी बहन के बेटे सैयद सालार मसूद गाजी के साथ एक विशाल सेना लेकर निकला।
उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले 800 सालों से विदेशी आक्रांता सालार मसूद के कब्र पर आयोजित होने वाले ‘नेजा मेले’ की अनुमति नहीं दी गई है। सालार मसूद क्रूर आक्रांता था, जिसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया और मंदिरों को ध्वस्त किया। इसी कारण उसे ‘गाजी’ (इस्लाम के लिए काफिरों से लड़ने वाला) की उपाधि मिली थी। संभल के बाद सालार के लिए बहराइच में लगने वाले जेठा मेला और बाराबंकी में उसके बाप की कब्र पर लगने वाले मेले पर रोक की माँग उठने लगी है।
संभल में सालार मसूद गाजी के कब्र पर मेला (उर्स) के इजाजत देने से इनकार करते हुए ASP श्रीश चन्द्र दीक्षित ने कहा कि किसी लुटेरे आक्रान्ता की याद में मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। यह अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था।
ASP ने कहा, “किसी भी लुटेरे के प्रति आप कहेंगे कि यह बहुत अच्छा है तो यह बिलकुल नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग अभी तक कर रहे थे तो यह कुरीति थी और आप अज्ञानता में यह कर रहे थे। अगर जानबूझ कर रहे थे तो आप देशद्रोही थे।” उन्होंने कहा कि उसने इस देश के प्रति अपराध किया था। लुटेरे की याद में कोई नेजा (झंडा-निशान) नहीं गड़ेगा। अगर ये झंडा गड़ गया तो वह देशद्रोह है।
सालार मसूद गाजी भारत में आक्रमण करने के दौरान जहाँ-जहाँ डेरा डाला था, वहाँ-वहाँ आज मुस्लिमों द्वारा उर्स मनाया जाता है। इनमें मेरठ का नौचंदी मेला, पुरनपुर (अमरोहा) का नेजा मेला, थमला और संभल के मेले प्रमुख हैं। इसके अलावा, कई अन्य स्थानों पर आज भी उर्स भी मनाए जाते हैं।
बाराबंकी में सालार मसूद गाजी के अब्बू सैयद सालार साहू गाजी उर्फ बूढ़े बाबा की दरगाह है। यहाँ भी यह सालाना उर्स हर साल के ज्येष्ठ माह (जेठ महीना) के पहले शनिवार को मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ रहने वाले मोहम्मद सिद्दीकी और अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि बूढ़े बाबा अफगानिस्तान का रहने वाले था। वह अफगानिस्तान के गजनी के शासक महमूद गजनवी का बहनोई था।
कहा जाता है कि 1400 साल पहले वह अपनी बीवी और बेटों के साथ अजमेर शरीफ आ गया था। यहीं पर सालार मसूद गाजी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी बीवी वापस अफगानिस्तान चली गई। वहीं, अबू सैयद सालार साहू गाजी बूढ़े बाबा अपने बेटे सैयद सालार मसूद गाजी के साथ बाराबंकी के सतरिख आ गया। यहाँ पर अबू सैयद मर गया और दफना दिया गया।
इसे ही आज बूढ़े बाबा की दरगाह कहा जाता है। समय-समय पर बूढ़े बाबा के कब्र को भी मजार का रूप दे दिया गया इसके बाद उसे दरगाह में तब्दील कर दिया गया। उसे गाजी के बाद बूढ़ा बाबा नाम के संत के रूप में प्रचारित किया गया। इसके कारण बड़ी संख्या में हिंदू भी इस मजार पर आते हैं। इन हिंदुओं की इन आक्रांताओं के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सैयद सालार मसूद गाजी का जन्म 11वीं सदी में सन 1014 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। हालाँकि, सालार के जन्म को लेकर भी संशय है और इतिहासकारों में एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सालार का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। खैर, उसका जन्म जहाँ कहीं भी हुआ हो, लेकिन वह बेहद ही क्रूर और हिंदुओं से नफरत करने वाला था।
यह प्रमाणित सत्य है कि अफगानिस्तान के गजनी के शासक महमूद गजनवी का भाँजा था। इसके साथ ही वह गजनवी के सेना का सेनापति भी था। यह वहीं गजनवी है, जिसने सबसे पहले सन 1001 में भारत पर हमला किया था। इसके बाद उसने एक-के-बाद एक करके लगातार 17 बार हमले किए और भारत के सोमनाथ मंदिर सहित भारत के कई मंदिरों को लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया था।
सन 1930 में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी ‘द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गाजना’ नाम की पुस्तक में इतिहासकार मोहम्मद नाजिम ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि वह गजनी के नेतृत्व में सन 1026 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी ने सबसे बड़ा हमला सोमनाथ मंदिर पर किया था। रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों, रियासतों और हिंदुओं का नरसंहार करता आया।
‘अनवार-ए-मसऊदी’ नाम की अपनी किताब में बहराइच के रहने वाले और इतिहासकार मौलाना मोहम्मद अली मसऊदी ने लिखा है कि सोमनाथ और आसपास की रियासतों पर लूटने-पाटने केबाद सैयद सालार गाजी आगे बढ़ा। वह 1030 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सतरिख पहुँचा। वहाँ से वह श्रावस्ती पहुँचा और वहाँ के राजा सुहेलदेव से उसका मुकाबला हुआ।
सन 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के पास सालार मसूद का मुकाबला महाराजा सुहेलदेव से हुआ। कहा जाता है कि महाराजा सुहेलदेव ने 21 अन्य छोटे-बड़े राजाओं के साथ मिलकर उसका सामना किया और आखिरकार इस गाजी का उपाधि धारण करने वाले इस आक्रांता को मार गिराया। इसके बाद स्थानीय मुस्लिमों ने उसके शव को दफना दिया।
पृथ्वीराज चौहान के साथ संभल में युद्ध
कहा जाता है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान का का भी सालार मसूद गाजी के साथ युद्ध हुआ था। संभल जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार, दोनों के बीच दो युद्ध हुए। इसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने सालार गाजी को करारी शिकस्त दी। वहीं, सालार के साथ दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार की बात कही जाती है। हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से इसके साक्ष्य नहीं हैं।
इतिहासकार बृजेंद्र मोहन शंखधर की किताब ‘संभल: अ हिस्टोरिकल सर्वे’ नाम की अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। इसमें उन्होंने लिखा पृथ्वीराज चौहान के संभल में रहने के दौरान एक वाकया हुआ था। किताब के अनुसार, “यहाँ सैयद पचासे नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति रहता था। इसकी कब्र फिलहाल मोहल्ला नाला कुस्साबान में है। वह सँभल के किले में रहता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी।”
किताब में आगे लिखा है कि एक दिन पृथ्वीराज चौहान के घराने का एक राजकुमार ने उस लड़की को देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गया। उसकी बेटी भी राजकुमार से आकर्षित हो गई। इससे सैयद पचासे गुस्सा हो गया और गजनी जाकर महमूद गजनवी से सारी बात बताई। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपनी बहन के बेटे सैयद सालार मसूद गाजी के साथ एक विशाल सेना लेकर निकला।
वह सिंध को पारकर मुल्तान, मेरठ और पुरनपुर (अमरोहा) होते हुए संभल पहुँचा। यहाँ पर युद्ध में दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गए। इसमें पृथ्वीराज चौहान के पुत्र भी मारे गए। बाद में सालार ने संभल के किले पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ से वह बहराइच भी गया और वहाँ मारा गया।
हालाँकि, इतिहासकारों से लेकर सत्यापित ग्रंथों में इसे एक लोककथा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में माना जाता है, जबकि मृत्यु मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में 1192 में हुई थी। वहीं, सालार मसूद ने सन 1026 में 16 साल की अवस्था में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस तरह, दोनों में 166 साल का अंतर है।
सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र
इसके बाद जिला मुख्यालय के पास पहने वाली नदी के पास चित्तौरा झील के किनारे उसे दफना दिया गया। यह भी कहा जाता है कि जिस जगह पर सालार मसूद को दफनाया गया, वहाँ बालार्क ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में सूर्यकुण्ड नाम का एक कुंड भी थी। बहराइच जिला को वेदों में गंधर्व वन बताया गया है।
बीतते के साथ, उस कब्र को मजार का रूप दे दिया गया। सालार गाजी की मौत के 200 वर्षों के बाद सन 1250 में दिल्ली का मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने कब्र को मकबरा का रूप दे दिया। आगे चलकर एक और मुगल शासक फिरोजशाह तुगलक ने इस मकबरे के बगल में कई गुंबदों का निर्माण करा दिया।
वहीं पर अब्दी गेट भी लगवाए। यही अब्दी गेट आगे चलकर सालार मसूद गाजी की दरगाह के नाम पर विख्यात हुआ। चूँकि सालार मसूद को मुस्लिम गाजी मानते थे। इसलिए मुस्लिम उसके कब्र पर सालना उर्स का आयोजन करने लगे और उसे संत ‘बाले मियाँ’ और ‘हठीला’ कहकर प्रचारित करने लगे।
संभल और बहराइच की ओर बढ़ते समय मुस्लिम आक्रांता सालार मसूद गाजी और उसके सैनिकों ने जहाँ-जहाँ डेरा डाला था, वहाँ-वहाँ आज भी मेले आयोजित किए जाते हैं। इनमें मेरठ का नौचंदी मेला, अमरोहा का पुरनपुर का नेजा मेला, थमला का मेला, संभल का मेला और बहराइच का मेला प्रमुख है। इन सभी स्थानों पर उर्स मनाए जाते हैं।
गाजी सैयद सालार मसूद का इतिहास: इस्लामी आक्रांता, जिसे दिखाया गया संत
इन आक्रांताओं की मौत के बाद उसे दरगाह का रूप दे दिया गया। इसके बाद इन्हें संत के रूप में नाम बदलकर प्रसारित किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू भी इन मजारों पर आने लगे और लाखों-करोड़ों रुपए की कमाई इन दरगाह समितियों को होने लगी। इसके लिए की तरह के अफवाह एवं भ्रांतियाँ फैलाई गईं।
कहा जाता है कि सालार मसूद ने ज़ुहरा बीबी नाम की एक लड़की से शादी की थी। उसने अपने चमत्कार से उस लड़की का अंधापन ठीक कर दिया था। इसके बाद उससे निकाह कर लिया था। इतिहासकार एना सुवोरोवा ने तो गाजी मियाँ कहलाने वाले सालार मसूद गाजी की तुलना भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम तक से कर दी है। साथ ही यह भी कहा कि हिन्दू उन्हें इसी रूप में देखते थे।
इसी तरह का चमत्कार सैयद सालार मसूद गाजी के अब्बू अबू सैयद सालार साहू गाजी को लेकर प्रसारित किया गया। उन्हें बूढ़े बाबा के नाम से प्रसारित किया गया और उनके चमत्कारिक किस्से की बात कही जाने लगी। हिंदुओं को तो ये भी नहीं पता कि ये भारत में आक्रमण करने वाले थे और मूर्तिपूजा एवं मंदिरों के सख्त विरोधी थे।
आज हालात ऐसे हैं कि उर्स लगने वाले इन सभी जगहों पर भारी संख्या में हिंदू आते हैं। ये राज्य के अलग-अलग इलाकों से आते हैं और मन्नत मानते हैं। मन्नत पूरा होने के बाद ये यहाँ फिर आते हैं। इस तरह आक्रांता को संत के रूप में प्रसारित करके उन्हें अवतार घोषित करने की कोशिश की गई, जो अब तक सफल भी रही।