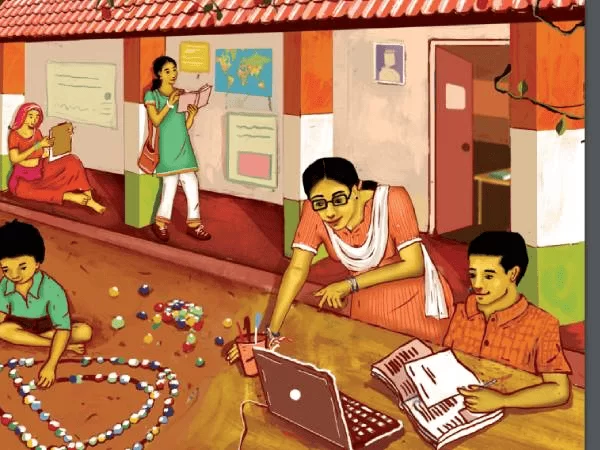राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत में 100 प्रतिशत स्कूलों में कौशल शिक्षा को जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है जिनमें से कम-से-कम 50 प्रतिशत छात्रों का नामांकन 2030 तक होगा.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 तीन आवश्यक वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करती है जिनके लिए शैक्षिक प्रतिक्रिया ज़रूरी है. सबसे पहले उभरती तकनीकें जैसे कि मशीन लर्निंग, बिग डेटा और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कल के काम करने वालों (वर्कफोर्स) में अनुकूलनशीलता (सीखने का तरीका सीखना) और बड़े स्तर के कौशल की मांग करती है. दूसरी बात ये है कि जलवायु परिवर्तन, घटते प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण की वजह से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां दुनिया में खाद्य, पानी, ऊर्जा और स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनोवेटिव और टिकाऊ समाधानों की मांग करती हैं. तीसरा, नई तरह की बीमारियों, महामारियों और संक्रामक रोगों के बढ़ते ख़तरे के कारण बेहतर चिकित्सकीय अनुसंधान और आर्थिक सामर्थ्य की आवश्यकता उत्पन्न होती है. इन चुनौतियों के लिए तैयारी के उद्देश्य से NEP शुरुआती कक्षाओं से ही नए युग की कौशल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता देती है जो अलग-अलग विषयों के दृष्टिकोण का लाभ उठाती है और सैद्धांतिक क्लासरूम के ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग के साथ जोड़ती है.
मिडिल ग्रेड्स यानी कक्षा छह से लेकर आठ के बीच CBSE ने 33 विषयों जैसे कि कोडिंग, डेटा साइंस, डिज़ाइन थिंकिंग और मास मीडिया पर 12-15 घंटे के स्किल मॉड्यूल की शुरुआत की है
शुरुआती उम्र से कौशल शिक्षा को लागू करने के लिए भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), जिसके साथ 30,634 स्कूल जुड़े हुए हैं, ने महत्वपूर्ण पहल की है. मिडिल ग्रेड्स यानी कक्षा छह से लेकर आठ के बीच CBSE ने 33 विषयों जैसे कि कोडिंग, डेटा साइंस, डिज़ाइन थिंकिंग और मास मीडिया पर 12-15 घंटे के स्किल मॉड्यूल की शुरुआत की है. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं (IX-XII) में छठे वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषय के रूप में 42 विषयों की सूची में से किसी एक कौशल वाले विषय को चुना जा सकता है. इन विषयों को भविष्य में करियर लाभ और छात्रों को रोज़गार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के अनुरूप तैयार किया गया है. 10 जनवरी 2025 के एक नीतिगत अपडेट के अनुसार अगर छात्र किसी वैकल्पिक विषय में फेल होते हैं तो शैक्षिक विषय के अंक को कौशल विषय के मार्क्स से बदल सकते हैं. इससे छात्रों को अपनी शैक्षिक यात्रा में अधिक लचीलापन मिलता है.
स्कूलों में कौशल शिक्षा को जोड़ने के CBSE के दृष्टिकोण में तीन पहलू उभर कर सामने आते हैं. पहला, ये अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि 3D (थ्री-डाइमेंशनल) प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI के साथ-साथ पारंपरिक विषयों जैसे कि कश्मीरी कढ़ाई, पॉटरी (मिट्टी के बर्तन बनाना) और हर्बल विरासत पर कोर्स की पेशकश करता है. दूसरा, ये आस-पास के संदर्भ में काम-काज की संभावना के हिसाब से स्कूलों को एक लचीला पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करके छात्रों के कौशल विकास की मांगों को स्थानीय उद्योगों की ज़रूरतों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है. तीसरा, उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मिलकर CBSE इन विषयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम का डिज़ाइन, पढ़ाई का संसाधन और मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) एवं परामर्श (मेंटॉरशिप) कार्यक्रम सक्रिय रूप से मुहैया कराता है.
अगस्त 2024 में CBSE ने ख़ुद से जुड़े स्कूलों को ज़रूरी औज़ार और तकनीक के साथ कंपोज़िट स्किल लैब (समग्र कौशल प्रयोगशाला) स्थापित करने का निर्देश दिया. तीन साल के भीतर स्थापित होने वाली इन प्रयोगशालओं का उद्देश्य छात्रों को लगातार व्यावहारिक अनुभव और उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग प्रदान करना है.
दूसरे बोर्ड जैसे कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन (CISCE) भी नए युग के विषयों की शुरुआत करके और उद्योगों के उभरते रुझानों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली जैसे संस्थानों से साझेदारी करके कौशल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं.
पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह के मिले-जुले प्रयासों ने भविष्य की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए भारत की तैयारी को बेहतर बनाया है. इस तरह QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत दुनिया में 25वें पायदान पर आ गया है जबकि “फ्यूचर ऑफ वर्क” सूचकांक में भारत उल्लेखनीय रूप से दूसरे स्थान पर है.
हर साल 97 लाख संभावित कामगारों को श्रम बल (लेबर फोर्स) में जोड़ने वाले भारत को शुरुआती स्तर पर कामगारों को हुनरमंद बनाने की पहल से बहुत अधिक सामाजिक-आर्थिक लाभ हासिल होगा. एक शुरुआती लाभ पढ़ाई के दौरान सीख और उसके व्यावहारिक, वास्तविक दुनिया में प्रयोग के बीच अंतर को पाटना है जिससे भविष्य के कामगार अधिक तैयार और रोज़गार के योग्य बन सकें. बढ़ईगीरी (कारपेंटरी), खेती, मार्केटिंग और सेल्स जैसे कौशल के विषय छात्रों को कक्षा में मिली जानकारी को ठोस तरीके से व्यवहार में लाने की अनुमति देते हैं. इस तरह एक समग्र और आकर्षक सीखने का अनुभव मिलता है.
एक शुरुआती लाभ पढ़ाई के दौरान सीख और उसके व्यावहारिक, वास्तविक दुनिया में प्रयोग के बीच अंतर को पाटना है जिससे भविष्य के कामगार अधिक तैयार और रोज़गार के योग्य बन सकें.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT 2017) के द्वारा कराए गए एक प्रभाव अध्ययन (इंपैक्ट स्टडी) में पता चला कि रोज़गार के लायक हुनर हासिल करने के अलावा कौशल शिक्षा ने छात्रों को रोज़गार में बने रहने, पढ़ाई-लिखाई में दिलचस्पी, परीक्षण के परिणामों और आत्मविश्वास के स्तर को बेहतर बनाने में मदद की. अलग-अलग करियर के रास्तों की तरफ शुरुआती जानकारी से छात्रों को अपनी दिलचस्पी और प्रतिभा का पता लगाने में मदद मिलती है. इससे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ अपने हुनर को जोड़ने का अवसर मिलता है.
वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स से पता चलता है कि भारत छात्रों को AI, ग्रीन (हरित) और डिजिटल स्किल में तैयार करने में पिछड़ रहा है. भारत में शुरुआती कौशल शिक्षा के स्तर में सुधार होने के साथ ही इस कमी का जल्द ही समाधान हो सकता है. उदाहरण के लिए, वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2024-25) में CBSE से जुड़े 4,538 स्कूलों के 8,00,000 से ज़्यादा छात्रों ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर AI कोर्स की पढ़ाई करने को चुना है जो भविष्य के हिसाब से तैयार हुनर के लिए मांग में बढ़ोतरी को दिखाता है.
तकनीकी क्षमताओं के अलावा कौशल शिक्षा संचार, रचनात्मकता, तालमेल और समस्याओं को सुलझाने जैसे जीवन से जुड़े ज़रूरी हुनर को भी बढ़ावा देती है. ये विकास की सोच को आगे ले जाती है, साथ ही अनुकूलनशीलता, सामर्थ्य और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है जो बदलते पारंपरिक नौकरी के बाज़ार और नए उद्योगों के उभरने के साथ तेज़ी से महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, कई छात्र पारंपरिक शैक्षणिक विषयों को भविष्य में अपने रोज़गार के लिए महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं लेकिन वो ऑनलाइन आवेदन जमा करने, प्रोफेशनल ई-मेल लिखने, बुनियादी हिसाब-किताब और ई-बिल तैयार करने जैसे रोज़गार के लिए आवश्यक हुनर सीखने की इच्छा रख सकते हैं.
बाज़ार के हिसाब से तैयार कामगार घरेलू रोज़गार की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ दुनिया में हुनरमंद श्रमिकों की कमी, विशेष रूप से बुजुर्ग होती आबादी से जूझ रहे विकसित देशों में, दोनों का बेहतर ढंग से समाधान करने के लिए भारत को तैयार करेंगे. ग्लोबल नॉर्थ (विकसित देश) तेज़ी से हुनरमंद पेशेवरों की सप्लाई के लिए भारत जैसे आबादी के मामले में युवा देशों पर निर्भर होता जा रहा है. अगर भारत अपने कौशल पाठ्यक्रम में वैश्विक मानकों को जोड़ता है और अपनी कौशल शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाज़ार की ज़रूरतों के अनुसार रणनीतिक रूप से बनाता है तो वो उद्योग 4.0 के युग में वैश्विक वर्कफोर्स के एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है.
समर्थ बनाने वाली नीतिगत स्थितियों के बावजूद भारत को कौशल शिक्षा के मामले में कम-से-कम तीन व्यापक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. सबसे पहले भारत में बुनियादी ढांचा और संसाधनों की कमी है. शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE+) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 57.2 प्रतिशत स्कूलों में काम करने वाले कंप्यूटर हैं, 53.9 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 55.9 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा है और मात्र 17.5 प्रतिशत स्कूलों में कला और शिल्प की सुविधाएं हैं. ये कमियां कौशल शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाने में बाधा बन सकती हैं.
दूसरा, ज़्यादातर स्कूलों में कौशल का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं. CBSE के द्वारा क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों और संसाधन विकास के बावजूद स्कूल अपने पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स या AI जैसे नए युग के कोर्स को जोड़ने में जूझ रहे हैं. उदाहरणों से पता चलता है कि छात्रों तक ये कोर्स पहुंचाने के लिए स्कूलों ने निजी वेंडर से तालमेल की तरफ रुख़ किया है. लेकिन ये वंचित क्षेत्रों के छात्रों के लिए सामर्थ्य और पहुंच का सवाल खड़ा करता है.
ज़्यादातर स्कूलों में कौशल का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं. CBSE के द्वारा क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों और संसाधन विकास के बावजूद स्कूल अपने पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स या AI जैसे नए युग के कोर्स को जोड़ने में जूझ रहे हैं.
इसके अलावा तीसरी बाधा भारत की सख्त स्कूल प्रणाली है जो शैक्षणिक विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. हो सकता है कि अभिभावक और शिक्षक कौशल शिक्षा के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाएं. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि स्कूल इस तरह की पहल के लिए पर्याप्त समय नहीं दें क्योंकि वो माध्यमिक कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा के प्रतिस्पर्धी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं. पारंपरिक रास्तों के विपरीत कौशल शिक्षा को अक्सर उन छात्रों के लिए बाद के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है जो मुख्यधारा की पढ़ाई-लिखाई में जूझते रहते हैं.
आगे का रास्ता
भारत के स्कूलों में कौशल की शिक्षा लेने वाले सिर्फ 4 प्रतिशत छात्र हैं जबकि पश्चिमी देशों के साथ-साथ दूसरे एशियाई देशों में ये अनुपात बहुत ज़्यादा है (रेखाचित्र देखें).
कौशल शिक्षा की इस स्पष्ट आवश्यकता और NEP के द्वारा निर्धारित मानदंडों को देखते हुए कई सरकारी और बहुपक्षीय एजेंसियों को भारत में कौशल शिक्षा के प्रभावी एकीकरण के उद्देश्य से सिफारिश पेश करने के लिए प्रेरित किया गया है. इनमें बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और कौशल केंद्रों के रूप में विशाल, बुनियादी ढांचे के मामले में सक्षम स्कूलों की स्थापना करके कौशल शिक्षा की पेशकश का विस्तार करने की ज़रूरत शामिल है. बाद में ये अपने आस-पास के छोटे स्कूलों के साथ हब एंड स्पोक मॉडल (एक मुख्य केंद्र और उससे जुड़े दूसरे संगठन) का पालन करते हुए जुड़ सकते हैं और सभी स्कूलों तक कौशल शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं.
इसके अलावा पाठ्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से उपकरण, संसाधन और तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराने में मदद के लिए निजी-सार्वजनिक साझेदारी (PPP) पर भी विचार किया गया है. तेज़ी से पहुंच और गुणवत्ता के भरोसे के लिए अलग-अलग हितधारकों यानी शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों, उद्योग, सिविल सोसायटी समूहों, CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) एवं बहुपक्षीय संस्थानों के बीच समन्वित कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है.
इस परिदृश्य में एक संतुलित दृष्टिकोण बरकरार रखने के लिए सतर्कता बरतना महत्वपूर्ण है. सबसे पहले, कौशल शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने और नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के अभियान में कभी-कभी क्वालिटी से जुड़े मानकों की अनदेखी हो सकती है. शिक्षकों की अपर्याप्त तैयारी, ज़रूरत से कम निगरानी और कमज़ोर मान्यता प्रणाली कार्यक्रम को प्रभावहीन कर सकती है जिसका नतीजा रोज़गार के लिए छात्रों के तैयार नहीं होने और कौशल एवं उद्योग की मांग के बीच अंतर बरकरार रहने के रूप में निकल सकता है.
एक और मुश्किल पाठ्यक्रम को गतिशील बनाए रखना और उसे उद्योग की बदलती आवश्यकता के अनुसार लगातार ढालना है. तेज़ी से बदलते दुनिया के श्रम बाज़ार और तकनीकी प्रगति के कारण ये ज़रूरी हो गया है कि कौशल शिक्षा को प्रासंगिक बने रहने के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उद्योग के हितधारकों एवं श्रम बाज़ार के विश्लेषण से मिले रियल-टाइम फीडबैक को शामिल करना चाहिए. इसके तहत पाठ्यक्रम में लगातार अपडेट के साथ लचीली कोर्स संरचना और शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योग जगत की हस्तियों के बीच मज़बूत साझेदारी शामिल है. इस तरह के उपाय सुनिश्चित करते हैं कि छात्र नौकरी के बाज़ार की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए ज़रूरी योग्यता रखते हैं.
एक महत्वपूर्ण ख़तरा गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा तक असमान पहुंच है जहां वंचित छात्र को बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल बंटवारे और ख़राब बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणित (FLN) से जुड़े परिणामों का सामना करना पड़ता है.
अंत में, एक महत्वपूर्ण ख़तरा गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा तक असमान पहुंच है जहां वंचित छात्र को बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल बंटवारे और ख़राब बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणित (FLN) से जुड़े परिणामों का सामना करना पड़ता है. इसलिए मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट, स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड और समुदाय आधारित कार्यक्रमों जैसे लक्षित हस्तक्षेप के बिना कौशल शिक्षा स्कूल की पढ़ाई-लिखाई में मौजूदा असमानताओं को दूर करने की जगह उन्हें और गहरा कर सकती है.
________________________________
अर्पण तुलस्यान ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में सीनियर फेलो हैं.