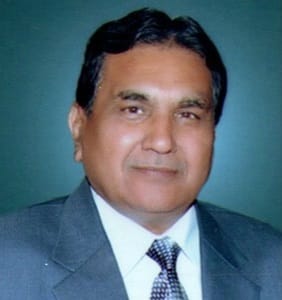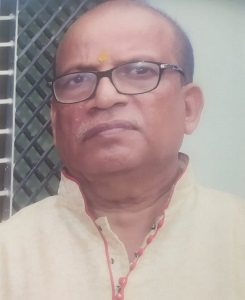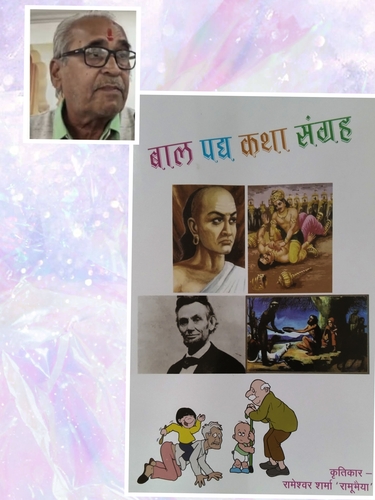बस्ती मण्डल के छन्दकारों मे कलजई कवि का परिचय डॉ मुनि लाल उपाध्याय ‘सरस’ जी के शोध प्रबंध “बस्ती के छंदकार” से सुलभ हो सका है। सुकवि चिन्ताहरण पाण्डेय “फूल” जी का जन्म बस्ती जिले के ओडवारा के पास मिटवा नामक ग्राम में 2 अक्टूबर सन 1925 ई. को तदनुसार सं० 1982 वि० में हुआ था। इनके पिता का नाम पण्डित देवशरण पाण्डेय था। फूलजी की शिक्षा- दीक्षा मेधावी माता के साहचर्य में गौरखपुर में समाप्त हुई थी। सन 1944 से फूलजी गन्ना विभाग के विविध पद पर कार्य करते हुए निरीक्षक के पद से 1983 में सेवामुक्त हुए थे। सन् 1945 से फूलजी अपने मनोहारी व्यक्तित्व और कृतित्व से बस्ती जनपद के काव्य-मंच पर छा गये थे । कवि “सनेही”जी और “हितैषी” जी से स्नेह पाकर “फूल” जी ने छन्दों के माध्यम से अपनी काव्य-यात्रा प्रारंभ की थी । फूलजी कवि “नन्दन” जी के योग्य शिष्यों में से थे। इस संदर्भ में नन्दन जी की दो पंक्तियाँ द्रष्टव्य है-
कवि फूल सुवाम मालिंद सदा
बिहरे जिसमें वह “नन्दन” हूँ।।
“नन्दन” जी के शिष्य होने के साथ-साथ फूल जी काव्य के क्षेत्र में अब्वास अली “बास” के कवि-भाई भी हैं। जिसकी पुष्टि इन पक्तियों से होती है-
“नन्दन” का नाज “फूलजी” का हमराज “बास”, नेह नागरी से गंवई में रहने लगा। – (आइना, शुभकामना से )
फूलजी की प्रारंभिक कविताएँ सुकवि, रसराज और अनुरंजिका आदि पत्रिकाओं में बड़े धड़ल्ले के साथ छपती रहीं। इनके मुस्कराते हुए अधरों से उछलते हुए गीतों के स्वर कवि सम्मेलों में हजारों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे ।
रचनाएं:-
“फूल जी का प्रकाशित साहित्य इस प्रकार हैं –
1- जवानी के गीत
2- पंचामृत
3- स्वर के तौर
4- आइना
उनकी अकाशित साहित्य की सूची इस प्रकार है –
1- साहित्य की ओर
2- डूबते स्वर
3- खामोशी
विस्तार से रचनाओं की जानकारी:-
1.जवानी के गीत :-
फूलजी की यह प्रथम रचना आग और पराग गीतो के माध्यम से जैसे ही जनपदीय छन्दकारों के सम्मुख आई उसे बहुत से लोगो ने सराहा I “अग्नि करण” शीर्षक में क्रांतिकारी गीत वर्तमान समाज पर तीखे व्यंग्य के परिप्रेक्ष्य में किया गया है-
फैलेगा अमर प्रकाश धरा में क्षण में,
फिर आंख क्रांति का सूर्य निकल जाने दो।
वह स्वर्ग धरा के चरण स्वयं चूमेगा,
चाँदी का चाँद निकल दर दर पर घूमेगा ।
यह व्यथित विश्व अलमस्त बना झूमैगा।
पर आंख जवानी के प्यालों में पहले
अभय प्रलय की मदिरा ढल जाने दो ।
निष्प्राण सभी यह जादू टोना होगा,
धरती का कण-कण सोना-सोना होगा।
जग का आलोकित कोना-कोना होगा,
उन अमर शहीदों की बेदी पर पल भर
कुछ तप्त रुधिर के दीपक जल जाने दो।
– (जवानी के गीत से।)
गीत की इन पंक्तियों में भावो का गौरवमय रूप मुखरित हो उठा है। जवानी के प्याले में त्याग और बलिदान के भावना की मदिरा ढलने से ही राष्ट्रीयता की बलिवेदी पर क्रान्ति का तुमुल बज उठता है। इस संदर्भ मै कवि का विचार उत्तम है।
2.पंचामृत :-
दूसरा काव्य-संग्रह “पंचामृत धार्मिक पृष्ठभूमि पर पाँच मुख्य आराध्य देवो के 108 नामों के पर्याय छन्दों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आस्तिकता का स्वर है और कवि के भावों का मानवीय उद्घोष ।
3.”स्वर के तीर”:-
तीसरा संग्रह “स्वर के तीर” राष्ट्रीयता से सम्वलित भावधारा में गीतों और छन्दों का पुट देकर लिखा गया है। इसके गीतों में कवि का जीवनदर्शन उभरता हुआ दिखाई पड़ता है।
4.आईंना :-
फूल जी की चौथी कृति “आईना” का प्रकाशन स्वतंत्र प्रकाशन,गौरखपुर से 1982 में हुआ है। इसमें कुल 87 पृष्ठ हैं। बाद में 9 पृष्ठ गजल के हैं। गीत, मुक्तक, गजल आदि के साथ फूलजी ने इसमें कुछ सवैया छन्दों का भी संग्रह प्रस्तुत किया है। इन छन्दों में अनेक दार्शनिक विचार सर्वत्र उभरते हुए दिखाई देते हैं। जीवन सन्ध्या पर लिखे हुए कुछ छन्द यहां प्रस्तुत हैं-
जीवन की उत्पत्ति जहा उस,
स्रोत की थाह लगाने चला हूँ।
स्वर्ग की मादक रागिनी से
अपने उर तार सजाने चला हूँ।
सैकड़ों कल्प से खोई हुई निधि
को अपने फिर पाने चला हूं।
साझ हुई उस जीवन की
उस लोक में दीप जलाने चला हूँ।।
– (आईना, पृष्ठ 76)
पुनः एक और छन्द प्रस्तुत है –
जीवन का जलता जिसमें
वह यौवन आग का फैसला होगा ।
ले चला है मजधार में जो
अपने उस भाग्य का फैसला होगा ।
जो उर सिन्धु जला चुका है
उस दीपक राग का फैसला होगा।
आज ही तो अपनाये गये
जग के अनुराग का फैसला होगा।।
जीवन की नश्वरता और अन्तिम क्षणों का चित्र कवि ने कितने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है-
दीन सभी धन धाम अरे,
बस चादर श्वेत ओढ़ाई गई है।
स्वर्ग से वैभव छोड़ के केवल,
बॉस की ठाट सजाई गई है।
लाख करोड़ की बात ही क्या,
मग के लिए दी नही पाई गई है।
जानता था जिसको अपना,
उसके कर आग लगाई गई है।।
मृत्यु के साथ जीवन की जीवन्तता और इस असार संसार की निस्तरता का वर्णन कवि ने “मानस हंस” शीर्षक से प्रस्तुत किया है। यहाँ अन्योक्ति का बडा अच्छा प्रयोग है।
मानस हंस बने अनजान
कहाँ इस विश्व को छोड़ चलोगे।
झंकृत जीवन बीन के तार
उन्हें फिर आज मरोड़ चलोगे।
सैकड़ों वर्ष से साथ से संचित
क्यों घट नेह का फोड़ चलोगे।
सांझ से जोड़ी हुई यह जीवन
डोर अचानक तोड चलोगे।।
पुनः एक और छन्द प्रस्तुत है –
आते देख के काली निशॉ
उसलोक में क्या जो अंधेरा ना होगा।
यौवन मादकता से भरा
अरे सीमित जीवन घेरा ना होगा ।
भ्रांति लिये भ्रम भेद की भावना,
भूल प्रपंच का डेरा ना होगा।
जीवन के मिटते क्षणों मे क्या
काल कराल का फेरा न होगा।।
इसी संदर्भ में पुनः एक छंद प्रस्तुत है –
बावला सा बन विश्व की आग से
बंधन नेह की जोड़ने वाले ।
जीवन सागर की लहरों में
अचेत सा हो सर फोड़ने वाले ।
भूत में भुले हुए अभिमान में
डूबे हुए दम तोड़ने वाले।
बाँधले जो कुछ बाँधना हो अरे!
वो इस विश्व को छोड़ने वाले ।।
कवि ने कबीर के जीवन दर्शन से प्राप्त विचारों को इस छंद के माध्यम से उन मनुष्यों की ओर संकेत किया है जो संसार को सब कुछ समझ कर जीते है और अपने को भूल जाते हैं। “मानव” शीर्षक कविता के छन्द अपनी मौलिकता के लिए अधिक सटीक है-
मोह के पाश में बद्ध हो बुद्धि
विवेक विसात ही भूल गया तू ।
चांदनी देख के मोहिनी ही तम
तोम की रात को भूल गया तू ।
जीवन कानन में अपने अपने
उत्पात को भूल गया तू ।
वैभव देख के स्वप्न सने उस
काल की बात ही भूल गया तू ।।
यहा” “उस काल” मे श्लेष अलंकार का प्रयोग है। इसके माध्यम से कवि ने भावी मृत्यु के क्षणो को दिखलाया है। इस जीवन का अन्तिम क्षण चिन्ताग्नि की महालीला में विलीन हो जाना है। उसे कवि उपस्थित करते हुए कहता है –
भूलता है जिस काल को तू
उसको निज बाह में भेटना होगा।
जीवन पत्र के चित्रित चित्र
तुम्हें अपने कर मेटना होगा।
प्राण से जोड़ा हुआ यह साँस
भरा ब्यवहार समेटना होगा।
ले निज कर्म की खाता बही
बस अन्त चिता पर लेटना होगा।।
रोक ली सास कनी अपनी
अपने अरमान भी मार के देखा
पी लिया है विष प्याले अनेक
कहो कितने दिन प्यार के देखा।
दे न सका प्रतिदान कोई यह
जीवन प्रान भी वार के देखा।
कोई नहीं अपना जग मे,
सपना यह आंख पसार के देखा।।
“मेरे प्रकाश” शीर्षक कविता में कवि का जीवन दर्शन प्रस्तुत है-
कभी जीवन ज्योति न मन्द हुई,
पलटा कभी भाग्य ने फेरा नही ।
सच मान ली भूल के आया कभी,
इस देश मे कोई लुटेरा नही। ।
इस जीवन चांद को आके कही,
तम तोम अभागे ने घेरा नहीं ।
अरे मेरे प्रकाश सुनो तो सही,
तुमने अभी देखा अंधेरा नहीं।।
पुन: इसी संदर्भ में सुख और दुख, प्रकाश और अन्धकार से सदर्भित दूसरा छन्द इस प्रकार है –
जिसने किया जा के रसातल वास न
न देखा कभी महाकाश न देखा ।
अपने में ही आप को देखा किया,
उसमें भगवान निवास न देखा ।
विषपान में जीवन बीता जहाँ,
जिसका उसने मधुमास न देखा ।
अपनाया अंधेरे को है जिसने,
उसने तुम्हें मेरे प्रकाश न देखा ।।
– (आइना पृष्ठ 82)
इसी संदर्भ में सुख-दुख “फूल” जी का विधवा के ऊपर लिखा हुआ गीत कितना कारुणिक है-
अपना चुकी हूँ किसी और को मै
कहा मानो मुझे अपनाओ नहीं।
सुधा छोड़ के आई हूं अरे
मुझको विष प्याला पिलाओ नहीं।
उस सुने प्रदेश में स्वप्न मे आके
सनेह की ज्वाला जगाओ नहीं ।
इन आंखों में आँखें समा चुकी हैं
इन आंखों से आंखे मिलाओ नहीं ।।
काव्य सौष्ठव :-
फूल जी के इन छन्दो मे बडी आकुलता है। जीवन की उत्कंठा और उसकेअन्तराल में दार्शनिकता की गहराई है। उनके गीतो मे भावों को तल्लीनता साधना कीउदात्तता और कल्पनाओ का स्वर है। रगीन जीवन में दुख-दर्द की झोली लिए सदैव मुस्कराते हुए रहना कवि फूल का स्वयं का जीवन- दर्शन है। फूलजी “पूर्वांचला”और “उपहार” दोनों पत्रिकाओं में अपने भाव व्यक्त करते हैं। शैली की दृष्टि से फूलजी छायावादी गीतकार, विचारों से प्रगतिवादी कविऔर विषय की दृष्टि ने परम्परावादी ठहरते हैं। जो गीत, गजल, मुक्तक, सवैया, धनाक्षरी आदि अनेक छन्द में काव्याभिव्यक्ति की है। — (पूर्वाधना, पृष्ठ 136,)
“फूल” जी सफल गीतकार और प्रगति शील कवि है। इनकी भाषा परिमार्जित और कोमल भावनाओं से ओत-प्रोत है। आप प्राचीन तथा नवीन दोनो शैलियों में कविताएँ लिखते है।
संक्षेप मे फूल जी आधुनिक चरण के उत्कृष्ट गीतकार एवं सफल छन्दकार के रूप में सम्मादृत हैं। संस्कृत के पुट में भावना प्रधान ललित भाषा का प्रवाह उर्दू मिश्रित हो करके और ही सरस बन गया है। उर्दू और हिन्दी के द्वार पर मुस्कराते हुए छन्दकार फूल का जनपदीय छन्दकारों के मंच से स्वागत होता रहा है।