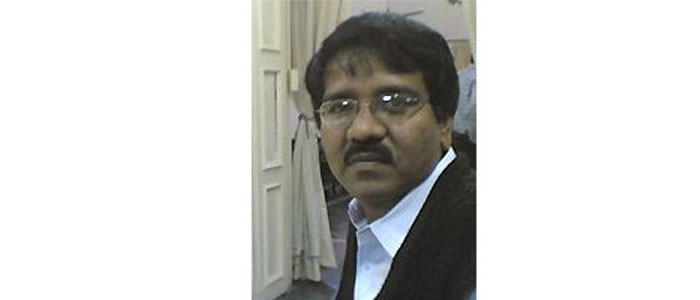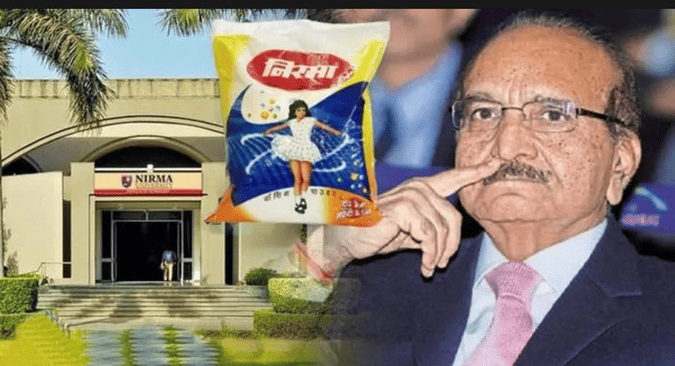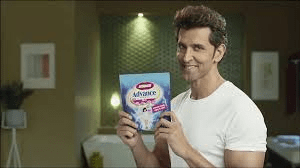प्रसिद्ध कवि माहेश्वर तिवारी’ का जन्म 22 जुलाई, 1939 को उत्तर प्रदेश के बस्ती मण्डल के जिला संत कबीर नगर के मलौली गाँव में हुआ था।जो संत कबीर नगर के घनघटा तालुका में स्थित है । यह धनघटा से 2 किमी तथा संत कबीर नगर जिला मुख्यालय से 28 किमी दूर स्थित है। हैसर धनघटा नगर पंचायत में गांव सभा मलौली शामिल हुआ है । यह एक प्रसिद्ध चौराहा भी है जो राम जानकी रोड पर स्थित है । इस गांव ने सर्वाधिक अभी तक ज्ञात आठ कवियों (सात तो चतुर्वेदी परम्परा के हैं) ,को जन्म दिया है। मलौली के मूलनिवासी तथा मुरादाबाद को अपना कर्मक्षेत्र के रूप में चयन करने वाले नवगीत के सुप्रसिद्ध कवि श्री माहेश्वर तिवारी हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनके पिता का नाम श्री श्याम बिहारी तिवारी है। वे राष्ट्रीय स्तर के गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। बस्ती जिले के महान साहित्यकार और राष्ट्रपति महोदय से शिक्षक सम्मान प्राप्त अवकाश प्राप्त स्मृति शेष प्रधानाचार्य डॉ मुनि लाल उपाध्याय ‘सरस’ ने अपने अप्रकाशित शोध ग्रन्थ बस्ती मण्डल के छन्दकार की पांडुलिपि के पृष्ठ पर “शलभ”जी को पृष्ठ 592 पर स्थान दिया है।
श्री माहेश्वर तिवारी का निधन 16 अप्रैल 2024 को हुआ था। हिन्दी अकादमी, दिल्ली के सचिव श्री संजय कुमार गर्ग द्वारा ‘शलभ’ जी के अविस्मरणीय साहित्यिक योगदान का स्मरण करते हुए इस प्रकार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया था। –
“हिन्दी की नवगीत धारा के प्रतिनिधि रचनाकार एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. माहेश्वर तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में और मुरादाबाद के साहित्यिक पर्याय थे। श्री माहेश्वर तिवारी जी का सृजन-संसार अपने समकालीन परिवेश एवं लोक मानस से निरंतर जुड़ा रहा है। उनके नवगीत अपनी विशेष रचना-दृष्टि अछूते बिम्बों और स्वस्थ कथ्यों के चलते पाठकों और श्रोताओं के मन को भीतर तक छूते हैं। माहेश्वर जी हिन्दी गीतिकाव्य परम्परा के उन गीतकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गीतों को समर्पित किया। उनके गीतों को पढ़कर, उनकी शैली से न जाने कितने कवि तैयार हुए। वे गीत को मंत्र की भांति मारक बनाने में निष्णात थे। नवगीतों का प्रकृति चित्रण इतना सजीव है कि जैसे प्रकृति स्वयं देह धारण करके वार्तालाप कर रही है। मंचों पर गीत धारा को निष्कलुष और जीवंत रखने में उनका योगदान अतुलनीय है।”
कुछ प्रमुख कृतियाँ :-
नवगीत-संग्रह
-
हरसिंगार कोई तो हो,
-
नदी का अकेलापन,
3. सच की कोई शर्त नहीं,
4. फूल आए हैं कनेरों में
“कविता कोश” से प्रकाशित गीत:-
कविता कोश असंख्य हिंदी कवियों को खोज खोज करके अपने मंच पर लाकर हिन्दी जगत को समृद्ध किया है। कोश ने ‘शलभ’ की जीवन परिचय के साथ उनके चयनित 25 गीत तथा एक बाल गीत को अपने प्रकाशन से जोड़कर आम जन मानस के करीब लाने का स्तुतय प्रयास किया है –
सोये हैं पेड़
झील का ठहरा हुआ जल
याद तुम्हारी
आओ हम धूप-वृक्ष काटें
सारे दिन पढ़ते अख़बार
गहरे गहरे-से पदचिन्ह
मन है
हसो भाई पेड़
जिन्दगी अपनी हुई है मैल कानों की
बहुत दिनों के बाद
कुहरे में सोए हैं पेड़
गर्दन पर, कुहनी पर, जमी हुई मैल सी
मुड़ गया इतिहास फिर
छोड़ आए हम अजानी घाटियों में
भरी-भरी मूँगिया हथेली पर
एक तुम्हारा होना
मुड़ गए जो
टूटे खपरैल-सी
फागुन का रथ
चिरंतन वसंत
गया साल
चिट्ठियाँ भिजवा रहा है गाँव
आज गीत गाने का मन है
याद तुम्हारी जैसे कोई कँचन-कलश भरे।
बाल कविताएं
पत्ते झरने लगे
विविध कृतियां :-
नवगीतों का विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी में अनुवाद तथा कैसेट काव्यमाला (वीनस कम्पनी)।
सम्मान:-
उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान सहित शताधिक संस्थाओं से सम्मानित।
प्रकाशन :-
प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं तथा अनेक समवेत संकलनों में रचनाओं का प्रकाशन।
प्रसारण : –
दूरदर्शन दिल्ली,लखनऊ व आकाशवाणी रामपुर व बरेली से अनेक बार कविता- कार्यक्रम प्रसारित।
व्यवसाय:-
लगभग दो दशक तक प्राध्यापन तथा पत्रकारिता से जुड़े रहने के बाद स्वतंत्र लेखन मुरादाबाद से किया।
स्थायी पताः-
1.ग्राम पोस्ट मलौली, धनघटा, जिला सन्त कबीर नगर उत्तर प्रदेश।
2.पत्राचार एवं स्थायी पताः ‘हरसिंगार’,ब/म- 48, नवीन नगर, काँठ रोड, मुरादाबाद-244001 (उ०प्र०)
माहेश्वर तिवारी की काव्य यात्रा
इस पोस्ट में प्रसिद्ध कवि ‘महेश्वर तिवारी’ को काव्य यात्रा के कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।
इस सदी का गीत हूँ मैं , गुन गुनाकर देखिए ; एक आलेख
हिन्दी नवगीत के महत्वपूर्ण और अद्भुत हस्ताक्षर श्री माहेश्वर तिवारी के सृजनात्मक उल्लेख के बिना न तो वह पूर्ण होती है और ना ही उस चर्चा का कोई महत्व रहता है। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त आंचलिक शब्द, मुहावरे और जीवन-जगत से जुड़े अनूठे प्रयोग उन्हें अन्य नवगीत- कारों में एक अलग विशेष पहचान दिलाते हैं।
उनके नवगीतों में भारतीयता की सांस्कृतिक सुगंध अपने समय के युगबोध और मूल्यबोध के साथ उपस्थित है, कथ्य और शिल्प में प्रयोगवादी स्वर है तो नवता के साथ। उन्होंने अपने नवगीतों में वर्तमान परिवेश के लगभग हर पहलू को सार्थक अभिव्यक्ति दी है, चाहे राजनीति का विद्रूप चेहरा हो, व्यवस्थाओं की अव्यवस्थित स्थिति हो, आम-आदमी की विवशताओं का चित्रण हो या फिर सामाजिक विषमताएं हों-
‘बर्फ होकर
जी रहे हम तुम
मोम की जलती इमारत में
इस तरह
वातावरण कुहरिल
धूप होना
हो रहा मुश्किल
जूझने को
हम अकेले हैं
एक अंधे महाभारत में’।
सुन रहा हूँ शेर की खालें दिखाकर
नवगीत ने हमेशा अपने समय केअधुनातन संदर्भों के यथार्थ को मुक्तछंद की कविताओं के समांतर ही उजागर किया है। कविता में यथार्थ का अर्थ सपाटबयानी या समाचार-वाचन नहीं होता, सच्ची कविता में यथार्थ की उपस्थिति भी अपनी संवेदनशीलता और काव्यत्व की ख़ुशबू के साथ होती है।
माहेश्वर तिवारी के नवगीतों में यथार्थ का चित्रण इसी काव्यत्व की ख़ूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह आम धारणा के साथ-साथ कड़वी सच्चाई भी है कि आज के समय में राजनीति के क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल है या हो सकता है जो छल-छंद, मक्कारी, दबंगई और अनैतिक चातुर्य में निपुण हो। राजनीति के ऐसे ही विद्रूप पक्ष को अपनी पंक्तियों में माहेश्वर तिवारी प्रभावी रूप से व्यक्त करते हुए मंथन करने पर विवश करते हैं-
‘सुन रहा हूँ
शेर की खालें दिखाकर
मेमने कुछ फिर किसी
मुठभेड़ में मारे गए
फिर हवा ने
मुखबिरी की चंद फूलों की
और बन आई
खड़े काले बबूलों की
कई कागज लिए बादामी
गाँव को जब
चंद हरकारे गए’
आने वाले हैं ऐसे दिन आने वाले हैं।
एक अन्य नवगीत में भी माहेश्वर तिवारी अपने मन की इन्हीं पीड़ाओं को प्रतीकों के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करते हुए साम्राज्यवादी नीतियों के ख़तरों के प्रति आगाह करते हैं-
‘आने वाले हैं
ऐसे दिन आने वाले हैं
जो आँसू पर भी
पहरे बैठाने वाले हैं
आकर आसपास भर देंगे
ऐसी चिल्लाहट
सुन न सकेंगे हम अपने ही
भीतर की आहट
शोर-शराबे ऐसा
दिल दहलाने वाले हैं’।
आज तथाकथित कुछ सुख-सुविधाओं की तलाश में आदमी का वास्तविक सुख- चैन ख़त्म हो गया है। कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से दिन-रात तनावग्रस्त रहना और चिन्ताओं की भट्टी में पल-पल गलते रहना उसकी नियति बन गई है। चिट्ठियां भिजवा रहा है गाँव
महानगरीय जीवन में व्याप्त इन्हीं विद्रूपताओं और विसंगतियों से व्यथित माहेश्वर तिवारी गांव वापस लौटने की आत्मीयता से लबालब गुहार लगाते हैं क्योंकि कवि को लगता है कि शहर की तुलना में गांव का जीवन अधिक सरल और सुकून भरा है-
‘चिट्ठियां भिजवा रहा है गाँव
अब घर लौट आओ
थरथराती गंध
पहले बौर की कहने लगी है
याद माँ के हाथ
पहले कौर की कहने लगी है
थक चुके होंगे सफर में पाँव
अब घर लौट आओ’।
माहेश्वर तिवारी हिन्दी नवगीत के एक समर्थ रचनाकार हैं। उनके रचना कर्म का कैनवास बहुत विस्तृत है, मुझे नहीं लगता कि उनकी लेखनी से कोई भी विषय छूटा हो। सामान्य सी बात है कि प्रेम का हर व्यक्ति से गहरा नाता होता है।
उन्होंने अपनी रचनाओं में जहां एक ओर अपने समय के यथार्थ को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हुए उकेरा है वहीं दूसरी ओर काग़ज के कोरेपन की तरह पवित्र प्रेम को भी मिठास की खुशबू भरे शब्द दिए हैं।
प्रेमगीतों का भी अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हिन्दी गीति-काव्य में प्रेमगीतों का भी अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, छायावादोत्तर काल में विशेष रूप से। माहेश्वर तिवारी के प्रेम की चाशनी में पगे गीतों में भी वही परंपरागत स्वर अपनी चुम्बकीय शक्ति के साथ विद्यमान है लेकिन नवता की मिठास के साथ-
‘डायरी में
उँगलियों के फूल से
लिख गया है
नाम कोई भूल से
सामने यह खुला पन्ना
दिख गया हो
कौन जाने आदतन ही
लिख गया हो
शब्द जो
सीखे कभी थे धूल से’।
माहेश्वर तिवारी का एक गीत जो रचा तो गया सन् 1964 में लेकिन आज आधी सदी बीत जाने बाद भी उतना ही ताज़गी भरा लगता है जितना रचे जाने के समय होगा। यह गीत केवल चर्चित ही नहीं हुआ बल्कि उनकी पहचान का गीत भी बना-
‘याद तुम्हारी जैसे कोई
कंचन-कलश भरे
जैसे कोई किरन अकेली
पर्वत पार करे।
लौट रही गायों के संग-संग
याद तुम्हारी आती
और धूल के संग-संग मेरे।
माथे को छू जाती
दर्पण में अपनी ही छाया-सी
रह-रह उभरे।
जैसे कोई हंस अकेला
आंगन में उतरे’।
लगभग सभी विषयों सन्दर्भों को उनके नवगीत आत्मसात करते हुए श्रोताओं से, पाठकों से सीधा संवाद करते हैं। उनके नवगीत ज़मीन से जुड़कर तो बात करते ही हैं, हमें ऐसे दिवालोक में भी ले जाते हैं –
जहां ‘खिलखिलाते हैं । नदी में/ जंगलों के गेह’, ‘दूर तक फैला हुआ तट/चाँदनी में सो गया है’, ‘डालों से उलझी है शाम/कनेरों वाली मुंडेरों पर’, ‘किसी स्वेटर की तरह/बुनकर/दिशाएं खुल गई हैं’, ‘मटर की ताज़ी फलियों से दिन’ और ‘कच्ची अमियां की फांकों-सी आँखें’ हैं।
शायद ही किसी ने पत्तियों को ताली बजाते देखा हो, माहेश्वर तिवारी के नवगीतों में पत्तियां भी ताली बजाती हैं-
‘पेड़ का
गाना सुना है क्या
पत्तियां
ताली बजाती हैं
और
सुर में सुर मिलाती हैं
यह कभी
हमने गुना है क्या’
गीतों की मिठास में हम झूम-झूम जाते हैं । विख्यात साहित्यकार दयानन्द पाण्डेय के शब्दों में कहें ‘माहेश्वर तिवारी के गीतों की मिठास में हम झूम-झूम जाते हैं। फिर जब इन गीतों को माहेश्वर तिवारी का सुरीला कंठ भी मिल जाता है तो हम इन में डूब-डूब जाते हैं। इन गीतों की चांदनी में न्यौछावर हो-हो जाते हैं। माहेश्वर तिवारी हम में और माहेश्वर तिवारी में हम बहने लग जाते हैं। माहेश्वर तिवारी के गीतों की तासीर ही ऐसी है। करें तो क्या करें?’ स्वयं तिवारी जी भी कहते हैं-
‘सिर्फ़ तिनके-सा न दाँतों में दबाकर देखिए-
इस सदी का गीत हूँ मैं, गुनगुनाकर देखिए’।।
हर नवगीत पर तैयार हो सकता है आलेख :-
श्री माहेश्वर तिवारी के रचना-संसार में नवगीतों के अनेकानेक बहुमूल्य रत्न हैं। उनके एक-एक नवगीत के संदर्भ में बात की जाए तो हर नवगीत पर एक आलेख तैयार हो सकता है। उनके रचनाकर्म के संदर्भ में कुछ भी लिख पाना विख्यात शायर स्व. कृष्ण बिहारी ‘नूर’ के इस शे’र जैसा ही है-
लब क्या बतायें कितनी
अज़ीम उसकी जात है।
सागर को सीपियों से
उलीचने की बात है।’
एक सुदीर्घ यात्रा में उन्होंने जीवन को जैसे गीत-संगीत की तरह साधा है. छोटी बहार के गीतों में भी वे जान फूँक देते हैं.
कभी जब नई कविता और गीत में फॉंक न थीं, नई कविता के साथ गीत की संगत चलती थी. अनेक नए कवियों ने गीत लिखे, सप्तवक परंपरा के कवि इस बात के प्रमाण हैं कि नई कविता के साथ नए गीतों का कोई वैर था. नवगीतों पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छंद परंपरा का वरदहस्त रहा तो प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के मन में भी गीतों को लेकर एक सकारात्मक भाव विद्यमान था. लेकिन धीरे-धीरे सप्तक के बाद गीतकारों को लगा कि एक अलग राह हमें चुननी चाहिए. नई कविता में हमारी समाई नहीं है. कभी अज्ञेय ने जिस भाव से कहा था छंद में मेरी समाई नहीं है, कुछ-कुछ उसी भाव बोध से नए गीतकारों ने अपनी राह तलाशी।
माहेश्वार तिवारी के तमाम गीत इन पत्रिकाओं में छपे. ‘धूप में जब भी जले हैं पांव घर की याद आई’ जैसे संवेदनशील गीत के माध्यम से माहेश्वर तिवारी ने गीत को नए स्थापत्य की संरचना में बांधने का यत्न किया-
आज गीत
गाने का मन है
अपने को
पाने का मन है।
अपनी छाया है
फूलों में
जीना चाह रहा
शूलों में।
मौसम पर
छाने का मन है।
नदी झील
झरनों सा बहना
चाह रहा
कुछ पल यों रहना।
चिड़िया हो
जाने का मन है।
‘
याद तुम्हारी’
उनकी सबसे प्रिय रचना है- ‘याद तुम्हारी’. उसका हर अंतरा जैसे दिल की भीतरी सतहों को छूता हुआ रचा गया है-
याद तुम्हारी जैसे कोई
कंचन-कलश भरे।
जैसे कोई किरन अकेली
पर्वत पार करे।
लौट रही गायों के
संग-संग
याद तुम्हारी आती
और धूल के
संग-संग
मेरे माथे को छू जाती
दर्पण में अपनी ही छाया-सी
रह-रह उभरे,
जैसे कोई हंस अकेला
आंगन में उतरे।
जब इकला कपोत का
जोड़ा
कंगनी पर आ जाए
दूर चिनारों के
वन से
कोई वंशी स्वर आए
सो जाता सूखी टहनी पर
अपने अधर धरे।
लगता जैसे रीते घट से
कोई प्यास हरे।
बाल गीत में भी महारत
पत्ते झरने लगे
पत्ते झरने लगे डाल से।
एक-एक कर-
दाँत गिर रहे जैसे-
बूढ़ी दादी के,
बर्फ पड़े तो लगते
जैसे, बिखरे
टुकड़े चाँदी के।
धीरे चलने वाला सूरज
राह नापता तेतज चाल से।
दिन छिलके उतारकर, लगते-
रक्खे उबले आलू से,
रातें लगतीं, जैसे हों-
निकलीं नदियों के बालू से!
मौसम से डर लगता
जैसे, इम्तहान वाले सवाल से।
(साभार: पराग, फरवरी, 1980, 54)
तीन कविताएं :-
एक
हमारे सामने
एक झील है
नदी बनती हुई
एक नदी है
महासागर की अगाधता की
खोल चढ़ाए हुए
एक समुद्र है
द्विविधा के ज्वार-भाटों में
फँसा हुआ
हमें अपनी भूमिका का चयन करना है ।
दो
आया है जबसे
यह सिरफिरा वसन्त
सारा वन
थरथर काँप रहा है
ऋतुराज भी शायद डरावना होता है
ऐसा ही होता होगा
तानाशाह ।
तीन
नया राजा आया
जैसे वन में आते हैं नए पत्ते
और फूल
पियराये झरे पत्तों की
सड़ांध से निकलकर
सबने ख़ुश होकर बजाए ढोल, नगाड़े।
अब वह ढोल और नगाड़े राजा के
पास हैं
जिनके सहारे वह
हमारी चीख़ और आवाज़ों से
बच रहा है ।
लेखक परिचय:-
(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए सम सामयिक विषयों,साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं।