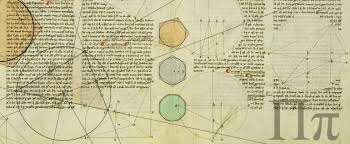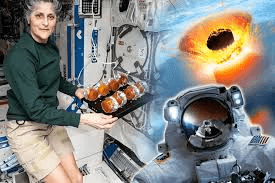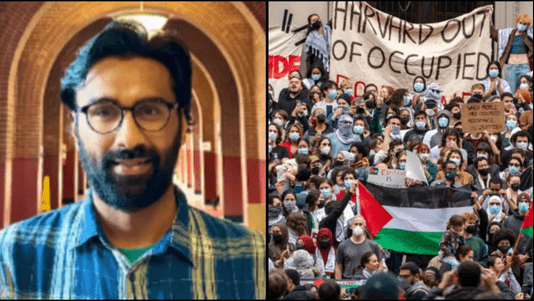बलूचिस्तान. पाकिस्तान का, फैलाव की दृष्टि से, या क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य. पाकिस्तानी जमीन का ४४% हिस्सा समेटने वाला. लेकिन सघन बसाहट नहीं. इसलिए जनसंख्या के मामले में पिछडा हुआ. सवा करोड़ के लगभग आबादी. समंदर को छूता हुआ किनारा. कुछ हिस्सा ईरान से जुड़ा हुआ, तो कुछ अफगानिस्तान से.
आज कुछ उजड़ा हुआ सा लगने वाला यह प्रदेश किसी जमाने में अत्यंत संपन्न था. विश्व में खेती करने के सबसे प्राचीन प्रमाण, इसी क्षेत्र में मिले हैं.
बलूचिस्तान का इतिहास काफी पुराना हैं. कुछ हजार वर्ष पुराना. पहले यह पूरा क्षेत्र हिन्दू था. संस्कृत के श्लोक, वेदों के मंत्र, उपनिषदों की ऋचाएँ यहाँ के दर्रे में गूँजती थी. इसी प्रदेश के मकरान क्षेत्र में, हिंगोल नदी के पास, अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पर देवी भगवती के ५१ शक्तिपीठों में से एक, ‘हिंगलाज माता का मंदिर’ हैं. अरबी समुद्र से यह मंदिर मात्र २० किलोमीटर दूरी पर हैं. चूंकि यह क्षेत्र रेगिस्तानी भाग में आता हैं, इसलिए इसे ‘मरुतीर्थ हिंगलाज’ भी कहा जाता हैं. इसी रास्ते से सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था. ऐसा माना जाता हैं, की इस स्थान पर प्रभु श्रीराम, जमदग्नि ऋषि, गुरु गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी भी आ चुके हैं.
हिंगलाज माता को चारणों की कुलदेवता माना जाता हैं. ये चारण लोग, बाद में बालूच कहलाएं. महाभारत काल में यह स्थान गांधार महाजनपद का हिस्सा था. महाभारत के यूध्द में इस पूरे महाजनपद ने कौरवों की तरफ से युध्द में भाग लिया था.
इसी बलूचिस्तान मे, बालाकोट के पास, मेहरगढ़ क्षेत्र में जो उत्खनन हुआ, उसमे हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले. इस प्रदेश में बोलन नदी के किनारे कुछ हजार वर्ष पूर्व एक विकसित सभ्यता थी, यह सिध्द हुआ हैं.
सन ७११ मे, जब मुहम्मद – बिन – कासम ने इस क्षेत्र पर हमले प्रारंभ किए, तब हिन्दू – बौध्द रहा यह पूरा इलाका, धीरे धीरे मुस्लिम होता गया. अकबर के शासन काल में, बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के आधीन था. लेकिन सन १६३८ में मुगलों ने पार्सिया (अर्थात ईरान) को यह इलाका सौंप दिया. लेकिन बाद में कलात के मीर नासीर खान ने १७५८ में अफगान शासन की आधीनता मान्य की.
प्रथम अफगान युध्द के बाद (अर्थात १८४२ के बाद), इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. अंग्रेजों ने इसे चार रियासतों में बाँट दिया – कलात, मकरान, लस बेला और खारत. लेकिन बीसवी सदी के प्रारंभ से बलुचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया. १९४१ में (जब द्वितीय विश्व युध्द अपने चरम पर था) बलूचिस्तान की आजादी के लिए ‘अंजुमन – ए – इत्तेहाद – ए – बलूचिस्तान’ का गठन हुआ. सन १९४४ मे, अंग्रेज़ जनरल मनी ने बलूचिस्तान की स्वतन्त्रता की दिशा में स्पष्ट संकेत दिये.
मजेदार बात यह, की रहमत अली ने पाकिस्तान की कल्पना करते हुए, इस मुस्लिम राष्ट्र के नाम में जो ‘स्तान’ जोड़ा था, वह बलूचिस्तान से ही लिया था. लेकिन जिस दिन पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, उस दिन उसके नक्शे में बलूचिस्तान नहीं था..! जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, या जिसका ‘पाकिस्तान’ इस प्रस्तावित नाम में भी उल्लेख नहीं था, ऐसा पूर्व बंगाल पाकिस्तान में था. लेकिन बलूचिस्तान नहीं आ सका.
वह तो पाकिस्तान को आजादी मिलने के, अर्थात १४ अगस्त, १९४७ से तीन दिन पहले ही आजाद हो गया था.
कलात…. बलूचिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक. क्वेटा से केवल नब्बे मील दूरी पर स्थित सघन जनसंख्या वाला यह शहर है. मजबूत दीवारों के भीतर बसे हुए इस शहर का इतिहास दो-ढाई हजार वर्ष पुराना है. कुजदर, गंदावा, नुश्की, क्वेटा जैसे शहरों में जाना हो तो कलात शहर को पार करके ही जाना पड़ता था. इसीलिए इस शहर का एक विशिष्ट सामरिक महत्त्व भी था. बड़ी-बड़ी दीवारों के अंदर बसे इस शहर के मध्यभाग में एक बड़ी सी हवेली थी. इस हवेली के, (गढी के) जो खान थे, उनका ‘राजभवन’ यह बलूचिस्तान की राजनीति का प्रमुख केन्द्र था. इस राजभवन में मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट और कलात के मीर अहमद यार खान की एक बैठक हुई. इनके बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके माध्यम से ११ अगस्त १९४७ से, कलात एक स्वतन्त्र देश के रूप में काम करने लगा.
ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में बलूचिस्तान के कलात का एक विशेष स्थान पहले से ही था. सारी ५६० रियासतों और रजवाड़ों को अंग्रेजों ‘अ’ श्रेणी में रखा है, जबकि सिक्किम, भूटान, और कलात को उन्होंने ‘ब’ श्रेणी की रियासत का दर्जा दिया हुआ था. अंततः ११ अगस्त को, दोपहर एक बजे संधिपत्र पर तीनों के हस्ताक्षर हुए. इस संधि के द्वारा यह घोषित किया गया कि कलात अब भारत का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया. मीर अहमद यार खान इस देश के पहले राष्ट्रप्रमुख बने.
कलात के साथ ही मीर अहमद यार खान साहब का पूर्ण वर्चस्व इस इलाके के पड़ोस में स्थित लास बेला, मकरान और खारान क्षेत्रों पर भी था. इसलिए भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान का निर्माण होने से पहले ही, इन सभी भागों को मिलाकर, मीर अहमद यार खान के नेतृत्व में बलूचिस्तान राष्ट्र का निर्माण हो गया…!
बलूचिस्तान के बलोच लोगों ने न तो पहले कभी पाकिस्तान में जाने के बारे में सोचा था, न ही आज भी उनकी वैसी मानसिकता हैं. बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बनना चाहता था, और वह बना भी.
किन्तु बलूचिस्तान की यह स्वतन्त्रता पाकिस्तान को फूंटी आँख नहीं सुहा रही थी. आखिरकार, सात महीने और सोलह दिन की बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के बाद, दिनांक २७ मार्च, १९४८ को पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अकबर खान ने इस छोटे से देश पर बलात कब्जा कर लिया. पिछले साढ़े सात महीनों में, यह छोटासा देश अपने सेना की जमावट भी ठीक से नहीं कर सका था. इसलिए प्रतिकार ज्यादा हुआ नहीं और पाकिस्तान के कब्जे में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह प्रदेश आ गया.
पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, किन्तु शासन करना कठिन था. मकरान, खारन और लस बेला तो पूर्णतः पाकिस्तान में शामिल हो गए. किन्तु कलात रियासत ने शामिल होने के बाद भी अपना अस्तित्व कायम रखा. आखिरकार, सन १९५५ में कलात रियासत भी पाकिस्तान में पूर्णतः विलीन हो गई.
मार्च १९४८ में बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा होते ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे. कलात के अहमद यार खान ने तो पाकिस्तानी कब्जे का ज्यादा विरोध नहीं किया. परंतु उनके भाई राजकुमार अब्दुल करीम ने, जुलाई १९४८ में पाकिस्तान के इस बलात कब्जे के विरोध में विद्रोह कर दिया. अपने अनुयाइयों के साथ वह अफगानिस्तान चला गया. तत्कालीन अफगान सरकार, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर के, उसे अपने कब्जे में लाना चाहती थी. क्यूंकी उन्हे समुद्री बन्दरगाह (सी पोर्ट) नसीब नही था और बलूचिस्तान के पास समंदर था.
लेकिन राजकुमार अब्दुल करीम को अफगान सरकार से वांछित समर्थन नहीं मिल पाया. अंततः लगभग एक वर्ष के बाद, राजकुमार करीम ने पाकिस्तानी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में एक जबरदस्त नाम उभरा – नवाब नौरोज़ खान. १९५५ में जब कलात रियासत को समाप्त कर, उसका पूर्णतः पाकिस्तान मे, ‘वन यूनिट’ पॉलिसी के अंतर्गत विलय किया गया, तो नवाब नौरोज़ खान ने पाकिस्तान का प्रखर विरोध किया. १९५८ में उन्होने पाकिस्तानी सरकार के विरोध में गुरिल्ला युध्द छेड़ दिया. वे नहीं चाहते थे की अन्य राज्यों की तरह बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान का नियंत्रण हो.
किन्तु कुछ ही महीनों के बाद, अर्थात १५ मई १९५९ को, नवाब नौरोज़ खान, पाकिस्तान सरकार के सामने आत्मसमर्पण को मजबूर हुए. पाकिस्तानी सरकार ने उन्हे और उनके सभी साथियों को माफी का आश्वासन दिया था. लेकिन फितरत के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने अपना ही वचन तोड़ दिया. नवाब के रिश्तेदार और १५० वफादार सैनिकों को पाक सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया. आखिरकार १५ जुलाई को इस विद्रोह के पांच नेताओं को फांसी पर लटकाकर मारा गया. नवाब नौरोज़ खान की उम्र हो चली थी, इसलिए उन्हे बख्शा गया. लेकिन पांच साल बाद, १९६४ मे, नवाब साहब कोहलू के जेल में चल बसे.
इस विद्रोह की चिंगारी भी इसी के साथ समाप्त हो जायेगी ऐसा पाकिस्तान सरकार को लगा. किन्तु ऐसा हुआ नहीं.
पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की स्थिति देखते हुए, वहां संवेदनशील इलाकों में सैनिकी अड्डे तयार करवाने का काम शुरू किया. इससे स्वतंत्र बलूचिस्तान समर्थक खौल उठे. उनके नेता शेर मोहम्मद बिजरानी ने, ७२ हजार किलोमीटर के क्षेत्र में अपने गुरिल्ला लड़कों के अड्डे खड़े किए. बलूचिस्तान में गॅस के अनेक भांडार हैं. ये विद्रोही नेता चाहते थे की पाकिस्तान सरकार इन गॅस भांडारों से मिलने वाली कुछ आमदनी इन कबाईली नेताओं से भी साझा करे. यह लड़ाई छह साल चली. किन्तु अंत में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता चाहने वाले विद्रोही सैनिक थक गए और राष्ट्रपति यांह्या खान के साथ युध्दविराम को राजी हो गए.
युध्दविराम होने के कुछ ही महीनों बाद, १९७० के दिसंबर में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए, यह आम चुनाव पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाले थे. पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल इन्ही चुनावों ने बदला.
१९७० के इन चुनावों में जहां पूर्व पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्र रहमान की अवामी लीग प्रचंड बहुमत से विजयी रही. तो यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़ीकार भुट्टो के पी पी पी की लगभग सभी प्रान्तों में जीत हुई – सिवाय बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ़्रोंटियल प्रोविन्स (NWFP) के. बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी जीती, जो की स्वतंत्रता वादी बलुचों की पार्टी थी. राष्ट्रीय असेंब्ली की ३०० में से शेख मुजीबुर्र रहमान की अवामी लीग ने जीती १६७ सीटे, तो भुट्टो की पार्टी को मिली मात्र ८१.
१९७१ यह वर्ष पाकिस्तान के इतिहास में भारी उथल पुथल वाला रहा. इस वर्ष के समाप्त होने के पहले, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और ‘बांग्ला देश’ के रूप में नए राष्ट्र का उदय हुआ, जो पहले ‘पूर्व पाकिस्तान’ था.
अब बचे खुचे पाकिस्तान मे, जनरल यांह्या खान को बलूचिस्तान में ‘नेशनल अवामी पार्टी’ की जीत बहुत अखर रही थी. उसे लग रहा था की, ‘ये बलूच लोग, ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा संघर्ष खड़ा करने वाले हैं’.
इसलिए, १९७१ के युध्द से थोड़े उबरते ही, पाकिस्तान ने १९७३ के प्रारंभ में बलूचिस्तान के प्रादेशिक सरकार को बर्खास्त किया और वहां पर ८० हजार पाकिस्तानी फौज उतार दी.
बंगला देश की गलती से सबक न सीखने वाले पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान में भी वही किया. भीषण अत्याचार…! बलूचिस्तान की तरफ जाने आले सभी रास्ते बंद कर दिये गए. बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, जहां पाकिस्तानी सेना को, बलूची विद्रोहियों के अड्डे होने की आशंका थी, वहां पर हवाई हमले भी किए. अनेक स्थानों पर बलूच विद्रोही और पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त संघर्ष भी हुआ. हजारों की संख्या में दोनों तरफ के लोग मारे गए. अनेक विद्रोही बलूच नेता, अफगानिस्तान पहुंचने में सफल रहे.
इस भयानक अत्याचार, दमन और संघर्ष के बाद, बलूच स्वतंत्रता आंदोलन में एक छोटासा ठहराव आया….
लेकिन इस ठहराव से एक सृजन हुआ – संगठित सशस्त्र आंदोलन का. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का…!
बलूचिस्तान – सतत संघर्ष / २
– प्रशांत पोळ
बलूचिस्तान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हैं. विस्तीर्ण भू प्रदेश हैं, जिसमे रेगिस्तान हैं, जंगल हैं, दर्रे हैं, समंदर हैं, बर्फ हैं…! सब कुछ हैं, इस प्रदेश में. पाकिस्तान का आधे से थोड़ा कम हिस्सा याने बलूचिस्तान. लेकिन जनसंख्या के मामले में मात्र बहुत कम. पाकिस्तान का हर पांचवा आदमी बलूचिस्तान से होता हैं.
राजधानी क्वेट्टा, बेहद खूबसूरत शहर हैं. यह फलों का शहर हैं. शहर के चारों ओर फलों के बगीचे. भरपूर फल, सूखे मेवों से सजे बाजार और शाम की ठंडी हवाएं. किसी समय क्वेट्टा ‘छोटा पेरिस’ कहलाता था. लेकिन आज नाही. आज क्वेट्टा, बमों के धमाकों से पहचाना जाता हैं.
पाकिस्तान को जो ९९० किलोमीटर का सागर किनारा मिला हुआ हैं, वह दो राज्यों के पास हैं – सिंध (२७० किलोमीटर) और बलूचिस्तान (मकरान ७२० किलोमीटर). सिंध के पास कराची जैसा विशाल बंदरगाह हैं, तो बलूचिस्तान के पास, अभी – अभी चीन का बनाया हुआ अत्याधुनिक ग्वादर बंदरगाह हैं.
कराची से ईरान की तरफ यदि हम अरेबियन समुद्र के किनारे से, ओमान की खाड़ी में बढ़ते जाते हैं, तो बलूचिस्तान राज्य के सोनमियानी, ओरमारा, कालमत, पासनी ऐसे बंदरगाह आते हैं. लेकिन ईरान की सीमा के पास, ओमान के सामने बना ग्वादर बंदरगाह भव्यतम हैं. यह बंदरगाह याने बलूचिस्तान की आजादी के रास्ते में खड़ी एक दीवार हैं…! चूंकि ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन ने किया हैं, इसलिए इस बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चीन ने ली हैं। अगले चालीस वर्षों का ग्वादर का स्वामित्व (लीज) चीन के पास हैं। इसलिए चीन वहाँ अपनी नौसेना का अड्डा बना रहा हैं। इसी संदर्भ में दो महीने पहले, पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख, अमजद खान नियाजी और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफ़ू के बीच रक्षा सहयोग पर सहमति बनी हैं। इसका अर्थ स्पष्ट हैं – ग्वादर और उसके आस पास के समुद्री इलाके में चीनी फौजों की संख्या बढ़ने जा रही हैं। बलोचिस्तान के लोगों को यह सब पसंद नहीं हैं। गुलामी की जंजीरे जकड़ती जा रही हैं, ऐसा उन्हे लगता हैं।
ग्वादर बंदरगाह यह चीन की महत्वाकांक्षी सी पी ई सी (China Pakistan Economic Corridor) परियोजना का हिस्सा हैं। ग्वादर को चीन के शिंजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए चीन, २४४२ किलोमीटर का आधुनिक रास्ता, पाकिस्तान में बना रहा हैं। चीन को लगने वाला तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) और मछली, चीन ग्वादर से, सड़क मार्ग से, अपने देश तक लेकर जाना चाहता हैं। किन्तु बलोच लोगों के विरोध से, और पाकिस्तानी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह रास्ता पूरा नहीं बन पाया हैं। बलोचिस्तान के नागरिक इस परियोजना का और चीनी नागरिकों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
बलूचिस्तान किसी जमाने में विशाल भारत का हिस्सा था. इससे पहले हमने देखा हैं की समूचा बलूचिस्तान, उन दिनों गांधार महाजनपद का हिस्सा था. किन्तु बलूचिस्तान के आज भी भारत से काफी निकट के संबंध हैं, रिश्ते हैं. एक संबंध, हजारो वर्ष पुराने रिश्तों की कड़ीयाँ जोड़ता हैं. बलूचिस्तान के कलात में जो ब्राहुई भाषा बोली जाती हैं, वह अपने दक्षिण भारत की द्रविडियन भाषा का ही एक प्रकार हैं. तमिल, कन्नड और तेलगु से बहुत कुछ मिलती – जुलती हैं. इस भाषा के अनेक शब्द तामिल, कन्नड भाषाओं से लिए गए हैं. त्रिचनापल्ली के एक मित्र ने बताया की उसने जब यह ब्राहुई भाषा की यू-ट्यूब चैनल देखी, तो उसे बहुत कुछ समझ में आया. कुछ समान शब्द –
तुम (You) – नी
आंखे (Eye) – कन
थूकना (Spit) – थुप्पू
पुत्र – लड़का (Son) – मखम यार
रोबर्ट कॉलवेल्ड (१८१४ – १८९१) ने इन दोनों भाषाओं की समानता पर बहुत अध्ययन किया हैं. उन्होने यह प्रमाणित किया हैं की ब्राहुई भाषा में तामिल एवं कन्नड के अनेक शब्द हैं. साथ ही दोनों भाषाओं की शैली भी एक जैसी हैं. किन्तु कालांतर से ब्राहुई भाषा, फारसी लिपि में लिखी जाने लगी हैं.
बलूचिस्तान से भारत का दूसरा रिश्ता पिछले ढाई सौ – पौने तीन सौ वर्ष पुराना हैं. पानीपत के तीसरे युध्द में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होने के बाद, मराठा सेना के लगभग बीस – पच्चीस हजार सैनिकों और महिलाओं को अब्दाली अपने साथ ले गया. रास्ते में पंजाब में सीख सेनानियों ने कुछ महिलाओं को तो छुड़वा लिया, किन्तु बाकी मराठों को बंदी बनाकर ले कर जाने में वह सफल रहा. अब्दाली का रास्ता बलूचिस्तान होकर जाता था. पानीपत के युध्द में, लूट और खजाना मिलने की आशा में, उसे बलूच सरदारों ने काफी सहयोग दिया था. इस पानीपत के युद्ध में मराठे हारे तो अवश्य, किन्तु उन्होंने इतना जबरदस्त संघर्ष किया, की अब्दाली के हाथ कुछ ज्यादा न लग सका. इसलिए अब्दाली ने खजाने के बदले, सभी बीस – पच्चीस हजार मराठे, गुलाम के रूप में, बलूच सरदारों को दे दिये. वस्तुतः पानीपत के युध्द में अब्दाली की हालत बहुत खराब हो गई थी. वो जीत जरूर गया था, लेकिन उसकी कमर टूट गई थी. (इसीलिए, अब्दाली के बाद, किसी ने भी खैबर के दर्रे से भारत पर आक्रमण की हिम्मत नहीं की). अब्दाली को इन बीस – पच्चीस हजार मराठा कैदियों को ढो कर अफगानिस्तान ले जाना संभव ही नहीं था.
वे बीस – पच्चीस हजार मराठा सैनिक वही बस गए. पहले बुगती और मर्री समुदाय के नौकर के रूप में रहने वाले मराठा सैनिक, बाद में अपने बलबूते पर उन्ही समुदायों के हिस्सा बन गए.
आज लगभग २५ लाख मराठा, बुगती और मर्री समुदाय में हैं. ये सब मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन अपने मूलाधार भूले नहीं. ये सब अपने नाम के आगे ‘मराठा’ लिखते हैं. उनके बहुत से रीति रिवाज, विवाह पध्दती, महाराष्ट्र की परंपरा से मिलते जुलते हैं. उनका एक संगठन हैं – ‘मरहट्टा कौमी इत्तेहाद ऑफ बलोचिस्तान’ (Marhtta Qaumii Ittehad of Balochistan). इस समुदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं – वडेरा दीन मुहम्मद मराठा (जमींदार दीन मुहम्मद मराठा). डेरा बुगती और सुई हिन्दू समुदाय, इन वडेरा दीन मुहम्मद साहब को इज्जत और सम्मान देता हैं.
इन सब की स्वाभाविक कड़ी, पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं. बहुत पहले से बलूचिस्तान अलग था. और इसीलिए आज भी इनको पाकिस्तान के साथ रहना नहीं हैं.
और भी कारण हैं.
बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार हैं. विशेषतः प्राकृतिक गॅस बड़े पैमाने पर निकलती हैं, जो पाकिस्तान सरकार के आमदनी का बड़ा हिस्सा हैं. लेकिन जहां से यह गॅस निकलता हैं, उस बलूचिस्तान के पास उस आमदनी का अत्यंत नगण्य ऐसा, छोटा सा हिस्सा आता हैं. इस कारण बलूचिस्तान प्रांत में विकास का चित्र कही दिखता नहीं हैं. अभी कुछ वर्षों में ग्वादर बंदरगाह पर जानेवाला जो एक्सप्रेस-वे चीन ने बनाया हैं, उसे छोड़ा दिया जाय, तो बलूचिस्तान में आज भी आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) की भारी कमी हैं.
और इसीलिए बलूच लोगों ने, २७ मार्च १९४८ को, जब पाकिस्तान ने उसे बलात अपने कब्जे में लिया, तब से पाकिस्तान के विरोध में विद्रोह का स्वर बुलंद किया हैं.