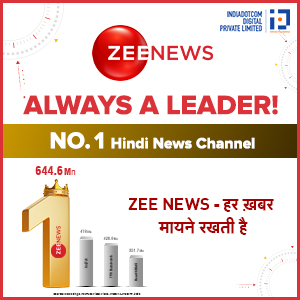पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम भाग मे उस देश का सबसे बडा प्रदेश है, बलुचिस्तान. 14 ऑगस्ट 1947 को जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब बलुचिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा नही था. वह एक स्वतंत्र राष्ट्र था. मार्च 1948 मे पाकिस्तानने इस प्रांत पर जबरदस्ती कब्जा किया. तब से पाकिस्तान के विरोध मे बलुचिस्तान मे निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता है. आज के समय में बलुचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे अधिक अशांत और विस्फोटक प्रांत है.
इस प्रांत में, सिंधू नदी की पश्चिम दिशा मे, बोलन पास के निकट, क्वेटा, कलात और सीबी इन शहरों के बीचमे, एक छोटासा गांव है – मेहरगढ. इस गांव में, सन 1974 मे, फ्रेंच खोजकर्ताओं का एक दल जा पहुंचा. उन्हे इस स्थान पर कुछ अति प्राचीन चीजे मिल सकती है, ऐसा लग रहा था. इसलिए उन्होने वहां उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया.
इस उत्खनन में उस फ्रेंच टीम को ऐतिहासिक खजाना मिला. उन्हे विश्व मे सबसे प्राचीन खेती करने के ठोस और जबरदस्त प्रमाण मिले. वह भी कितने पुराने? तो ईसा पूर्व 7000 वर्ष. अर्थात, आजसे 9000 वर्ष पूर्व, तत्कालीन अखंड भारत मे खेती होती थी, यह निर्णायक रूप से सिद्ध हुआ. उसी के साथ विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे उन्नत खेती करने की परंपरा भारत मे थी, यह भी सिद्ध हुआ.
ऋग्वेद यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है. इस ऋग्वेद में, खेती के संदर्भ में अनेक सूक्त है. इस ग्रंथ के दुसरे मंडल में वर्णन किया है की, सर्वप्रथम ऋषी गृस्मद ने रुई (कपास) का बीज बोया, और उससे उगे पौधे से रुई निकाली.
ऋग्वेद के चौथे मंडल में, 57 वें सूक्त मे सातवा श्लोक है-
इंद्रः सीतां नि गृहणातु तां पूषानु यच्छतु
स नाः परिस्वती दुहामुत्तरा मुत्तरा समाम ll7ll
यहां ‘सीता’ यह शब्द ‘भूमि’ के लिये उपयोग मे लाया है. इंद्र यह शब्द वर्षा के लिए (पर्जन्य के लिए) है. इस श्लोक का भावार्थ है, ‘हे कृषक, हे किसान, खेती का काम करते समय इस क्षेत्र के विद्वजनोंका अनुकरण कीजिए और खेती की आय बढाईये.’
ऋग्वेद के चौथे मंडल के 57 वे मे सूक्त मे आठवा श्लोक है –
शुन्य नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं की नाशां अभि यन्तु वाहैः l
शुनं पर्जन्यो मधुना पयौभिः शुनांसीरा शुनमस्मासुं धत्तम् ll8ll
अर्थात, ‘कृषी कर्म (खेती) करने वाले व्यक्तिने अच्छी गुणवत्ता के हल से जमीन को जोतना चाहिये. बारिश के पानी से या भूमिगत पानी से जमीन का सिंचन करके किसान ने और (खेती अच्छी हुई और अच्छा राजस्व मिला इसलिये) राजाने सुखी होना चाहिये’.
ऋग्वेद के कम से कम 24 सुक्तों मे कृषी का वर्णन करने वाली ॠचाएं है. अथर्ववेद मे एक सुक्त है–
व्राहीमतं यव मत्त मथो, माषमथों विलम् l
एष वां भागो निहितो रन्नधेयाय, दंतौ माहीसिष्टं पितरं मातरंच ll
इसमे जौ, तीली, चावल और दाल ये प्राचीन भारत के प्रमुख अनाज थे, यह स्पष्ट हो रहा है.
अथर्ववेद के अन्य सूक्तों मे खाद के प्रकार, जमीन के प्रकार आदि का वर्णन है.
ध्यान रहे, आज से कम से कम पांच – छह हजार वर्ष पहले, अपने देश मे व्यवस्थित और उन्नत किस्म की खेती होती थी. अकूत अनाज मिलता था. इसलिये देश मे समृद्धी थी, खुशहाली थी, संपन्नता थी. इसीके बल पर हम विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे और धन-संपत्ती भारत मे लाते थे.
विशेष बात यह है कि, दुनिया मे कही भी इस प्रकार की, वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार पर खेती करने की, इतनी प्राचीन जानकारी उपलब्ध नही है.
केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसे वैदिक साहित्य मे ही खेती से संबंधित ‘शास्त्र’ की जानकारी मिलती हैं, ऐसा नही है. इनके बाद मे उपलब्ध ग्रंथो मे भी खेती संबंधित जानकारी मिलती है.
भारतीय किसान तंत्रशुद्ध पद्धति से खेती करते थे, यह जानकारी अगले सैकडो वर्षो मे ऐसेही मिलती गई है और उसमे भी अनेक सुधार हुए है.
इन सब ग्रंथों मे हल के प्रकार, हल का फाल से होने वाला कोण, मिट्टी के प्रकार, कौनसी मिट्टी मे कौनसा अनाज बो सकते है, पर्जन्यवृष्टी (वर्षा / बारिश) और खेती का अनन्य साधारण आपसी संबंध, पर्जन्यवृष्टी और नक्षत्र, किस प्रकार की बारिश में किस प्रकार का अनाज लेना है, खेती के लिए आवश्यक गोवंश कैसे संभालना चाहिये, खेती के लिये हल जोतने वाले बैल कैसे होने चाहिये, उन्हे कैसे संजोना चाहिये, संम्हालना चाहिये….
या सब पढ़कर हम आश्चर्यचकित हो जाते है..!
कमसे कम, पाच – छह हजार वर्ष पहले की यह सब लिखित जानकारी है. भारत मे उन्नत और प्रगत खेती थी, और शायद उससे भी और पहले, कई हजार वर्षों से यह चलती आ रही होगी.
यह सब अद्भुत है. हमारे पुरखो ने कृषी के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त किया, वैसा विश्व मे कही भी उपलब्ध नही है. उस ज्ञान से, वे इतने अनाज का उत्पादन करते थे, जिससे देश मे संपन्नता आई थी.
पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जिला हैं, ‘एटा’ नाम का. गंगा जमुना के दोआब के बीचो बिच स्थित. अर्थात सभी प्रकार से उपजाऊ प्रदेश. पेशवाओं के जमाने मे इस प्रदेश को ‘अंतर्वेद’ नाम से जाना जाता था. उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, एटा जिले मे प्राचीन खेती के प्रमाण मिले है.
यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी. इसी नाम से यह नदी एटा जिले से बहती है. श्रीकृष्ण भगवान ने अपने बाल रूप में इसी कालिंदी के गहरे पानी मे कालिया नाग पर नृत्य किया था. इस कालिंदी नदी के तट पर, जखेडा नाम का एक गाँव है. यहां जो उत्खनन हुआ, उसमे हल के दो लोहे के हिस्से मिले. यह छब्बीस सौ वर्ष प्राचीन है.
इसे जखेडा से 16 किलोमीटर दूरी पर, एटा जिले मे ही ‘अतरंगी खेडा’ नाम का छोटासा गांव है. अलेक्झांडर कनिंगहम नाम के ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञ ने सन 1871 मे यहां उत्खनन किया. इस उत्खनन मे उसे भारत मे प्राचीन खेती के अनेक प्रमाण मिले. कृषी हेत बीज के लिए रखे गये चावल, गेंहू , उस जमाने के खेती के औजार, हल ऐसा बहुत कुछ… यह सब चीजे कार्बन डेटिंग के अनुसार, ईसा पूर्व बारह सौ वर्ष की है. इसका अर्थ, आज से 3200 वर्ष पहले अपने देश मे, उस जमाने की अपेक्षा कही अधिक आधुनिक पद्धति से खेती हो रही थी. इसके ये सब प्रमाण है.
शुल्बसूत्र लिखने वाले ‘बोधायन’, उनतीस सौ वर्ष पूर्व के है. उन्होने ‘कुदाली’ का उपयोग करके खेती करने वालों के लिए, ‘कौद्दालिक’ इस शब्द का प्रयोग किया है. प्रख्यात व्याकरणकार ‘पाणिनी’ का कार्यकाल ईसा पूर्व पाँचवी सदी का है. अर्थात, ढाई हजार वर्ष पहले का. उन्होंने उनके ‘अष्टाध्यायी’ ग्रंथ मे हल और लोहे के फाल के लिए ‘अमी विकार कुशी’ इस शब्द का उपयोग किया है.
ईसा पूर्व तीसरी सदी मे, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने, ‘कौटिल्य’ नाम से ‘अर्थशास्त्र’ यह प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा. अर्थतंत्र को गतिमानता देने के लिए खेती यह आवश्यक घटक / हिस्सा है, ऐसा प्रतिपादित करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ मे खेती की महत्ता का अनेकोबार उल्लेख किया है. इनमे से 2 से 14 अध्यायों के शीर्षकही ‘सीता अध्यक्ष’ है. भूमी के लिये संस्कृत में ‘सीता’ शब्द का उपयोग किया जाता है, यह हमने देखा हैं. अर्थात, यहां कौटिल्य को ‘कृषीशास्त्र के प्रमुख’ यह अर्थ अपेक्षित है. खेती और वर्षा का अनन्य साधारण संबंध होने के कारण, ‘वर्षा और वर्षा का भविष्य’ इस पर विस्तार से चर्चा की है. अच्छा बीज कैसे तयार किया जाता है, उसे कैसे जतन किया जाता है, अलग – अलग प्रकार के बीज कैसे संकलित और संग्रहित किये जाते है.. इन सब का शास्त्रशुद्ध ज्ञान भी इसी ग्रंथ मे दिया है. सरकारने कृषी उत्पादन बढाने के लिए क्या, क्या योजनाये बनानी चाहिये, इसका भी विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ मे किया है.
कौटिल्यने इस ग्रंथ के छठवे अध्याय में लिखा है कि, ‘कृषि योग्य जमीन, खदानों से अच्छी होती है. क्योंकि खदानों के कारण केवल राजकोष मे वृद्धि होती है, परंतु खेती के कारण राजकोष और भांडार, दोनों मे वृध्दि होती है.’
कौटिल्य ने ‘अर्थशास्त्र’ इस ग्रंथ मे तीन प्रकार के उर्वरकोंका (खाद का) उल्लेख किया है –
01. गोस्थी
02. गोश कृद (गाय का गोबर)
03. अशुष्क कटू मत्स्य
शाखिनां गर्तदाहो गोस्थीशकृदिभः काले दौहदंच l
प्रुरुढांश्चाशुष्ककटू मत्स्यांश्चस्नुहि क्षीरेण पायतेत ll
(अर्थशास्त्र / 2.24 / 34)
दो – ढाई हजार वर्ष पहले, अच्छी खेती का कितना गंभीरता से और गहराई से हमारे पूर्वजों ने विचार किया था, यह अर्थशास्त्र ग्रंथ पढने से समझ मे आता है.
कौटिल्यने ‘सीताध्यक्ष’ के प्रमुख कर्तव्यों मे, अच्छे बीजों का जतन और संवर्धन प्रमुखता से बताया है. कौटिल्यने तीन प्रकार के जमीन का वर्णन किया है.
01. कृष्ट भूमि (जो जोती हुई है)
02. अकृष्ट भूमि (जो जोती नही हैं, पर जोती जा सकती है)
03. स्थलभूमि (बंजर जमीन)
खेती के लिए जो जमीन उपयुक्त नही है, वह जमीन गोचर भूमि (चारागार जमीन) अर्थात, गोवंश के चारे के लिए विकसित की जाती थी. कौटिल्यने इस जमीन को ‘अदेवमातृक भूमी’ कहा है.
कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे, और (आगे चलकर लिखे गये) वराह मिहिर के ‘बृहत्संहिता’ मे, अच्छे कृषी के लिए सिंचन की आवश्यकता और सिंचन के प्रकार,
विस्तार से बताये गये है. कौटिल्यने चार प्रकार के सिंचन पद्धती का वर्णन किया है.
1. हाथों की सहायता से सिंचन
2. कंधों पर पानी लाकर किया हुआ सिंचन
3. यंत्र द्वारा सिंचन
4. तालाब के पानी से किया हुआ सिंचन
प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यकेतू विद्यालंकार ने, उनके ग्रंथ ‘प्राचीन भारत – प्रारंभ से 1200 इ.स. तक’ मे कौटिल्य के सिंचन पद्धति का और विस्तार किया है. इसमे उन्होने पांचवी पद्धती जोड दी है – बांध का निर्माण करके, उससे नहर निकाल के, उसके द्वारा सिंचन करना, यह पांचवी पद्धती है. यंत्र द्वारा किये जाने वाले सिंचन मे सत्यकेतू विद्यालंकार के अनुसार, पवनचक्की से पानी लेकर सिंचन किया जाता था. इसके अलावा सिंचन के लिए मोठ (चरसा / पुर) का भी उपयोग होता था.
छठवी सदी मे, उज्जैन के वराहमिहीरने पर्जन्यवृष्टि के संदर्भ मे, अर्थात, वर्षा के ‘पैटर्न’ के बारे मे बहुत कुछ लिखा है. ‘बृहत्संहिता’ इस ग्रंथ के 21, 22 और 23 अध्यायों मे उन्होने अंतरिक्ष से आनेवाला जल, अर्थात पर्जन्य के संदर्भ में विस्तार से लिखा है. बारिश और खेती का अनोन्य संबंध भी उन्होने रेखांकित किया है. ‘अच्छी वर्षा हुई, तो अच्छा अनाज आयेगा’ की अपेक्षा, ‘वर्षा का अनुमान लगाके, उसके अनुसार अगर बीज बोयेंगे, और अनाज निकालेंगे, तो अधिक उत्पादन होगा’, यह उनका सिद्धांत था. और इसिलिये ‘बृहत्संहिता’ ग्रंथ मे बारिश के भविष्यवाणी से संबंधित अनेक संकेत दिये है.
वराहमिहिर के पश्चात, लगभग 200 वर्षों के बाद, पाराशर ऋषि ने ‘कृषि पाराशर’ ग्रंथ लिखा. प्राचीन कृषि शास्त्र का संकलन और उस पर भाष्य, ऐसा इस ग्रंथ का स्वरूप है. यह ग्रंथ बहुत बडा नही है, परंतु जिस शास्त्रशुद्ध पद्धतीसे और अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से भारतीय कृषक खेती करते थे, उस का विस्तार से वर्णन हैं, और ठोस प्रमाण भी !
पाराशर ऋषि की दृढ़ धारणा थी की, बारिश की पूर्व सूचना, या बारिश की पूरे वर्ष की रूपरेखा, अगर वर्ष के प्रारंभ मे ही पता चलती है, तो उसके अनुसार ‘कौन सा अनाज लेना ठीक रहेगा’ यह तय कर सकते है. इसिलिये वे लिखते हैं–
वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टीमूलं च जीवनम l
तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टीज्ञानं समाचरेत् ।।
अर्थात, संपूर्ण कृषि का मूल कारण वृष्टि (बारिश) है. वृष्टी अपने जीवन का भी मूलाधार है. इसीलिए, प्रारंभ मे ही वर्षा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है.
ऋषि पाराशर के मतानुसार, दो या तीन दिन के बारिश के पूर्वानुमान का किसान को कतई उपयोग नही है. किंतु उसे पूरे वर्ष का बारिश का पॅटर्न (आकृतिबंध) अगर पता चलता है, तो किसान उस हिसाब से अपने खेती का नियोजन कर सकता है.
पूरे वर्ष के बारिश के पैटर्न का अनुमान निकालने के लिए, पाराशर ऋषि ने एक विधि विकसित की थी. इस विधि के अनुसार, पौष महीने के 30 दिन के वायू (हवा) की गति और दिशा के आधार पर, पूरे वर्ष के बारिश का पैटर्न तयार कर सकते है. 30 दिन के घंटे होते हैं, कुल 30 × 24 = 720 घंटे. इन 720 घंटों को 60 घंटो का एक भाग करके विभाजित किया, तो बारह भाग तैयार होते है. अर्थात, बारह महीने. इन बारह भागों में, प्रत्येक भाग के प्रत्येक दिन, (अर्थात तीस दिन) सुबह – शाम वायु की गति और दिशा का अध्ययन किया, तो पूरे वर्ष मे आने वाले बारिश का पैटर्न निश्चित रूप से विकसित कर सकते हैं। हर भाग को एक मास (एक महिना) माना, तब 12 भागोंका मॅपिंग बारा महाने मे कर सकते है. एक भाग के दो घंटो को एक दिन माना जायेगा. (कुल साठ घंटे अर्थात तीस दिन). उन दो घंटो मे से पहला घंटा दिन और बाद का घंटा रात.
सार्ध्द दिनद्वयं मानं कृत्वा पौषादिना बुधः ।
गणयेन्मासिकीं वृष्टिमवृष्टिं वानिलक्रमात ।।
(वृष्टिखंडः / 21)
अर्थात पौष माह के पहले ढाई दिन मे (अर्थात 60 घंटों मे), अगर हवा पश्चिम और उत्तर दिशा मे बह रही हो, तो उस कालखंड से संबंधित महीने के उस दिन बारिश होगी.
कितना अद्भुत है यह सब..!
मजेदार बात यह है कि, ‘कृषि पाराशर’ इस संस्कृत ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले रामचंद्र पांडे ने, सन 1966 मे ‘कृषि पराशर’ ग्रंथ मे दी हुई विधि से, काशी नगर मे प्रयोग किया. इस प्रयोग मे उन्हे काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह और काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर धुनीनाम त्रिपाठी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.
विश्वविद्यालय के छत पर टेंट लगाकर, प्रतिदिन उन्होने हवा की (वायु की) गति और दिशा का अध्ययन किया. ऐसा ही अध्ययन, काशी के रामनगर चौक मे रहने वाले डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्त के छत पर भी किया गया. दोनो जगह के अध्ययन के आधार पर, उन्होने पूरे वर्ष की बारीश की तालिका तैयार की. सन 1967 मे पूरे वर्ष, प्रतिदिन, उस तालिका के अनुसार ग्रहों / नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति, वृष्टि, अनावृष्टी आदि का अध्ययन किया गया. रामचंद्र पांडे लिखते है कि, ‘इसका परिणाम अच्छा मिला. सीमित संसाधनों को लेकर किये गये प्रयोग के अनुसार, वार्षिक बारिश का अनुमान 76 प्रतिशत सही रहा..!
यह सभी अर्थो मे अद्भुत है. न कोई सॅटॅलाइट, न कोई वेदर सेन्सिंग उपकरण… देढ हजार वर्ष पहले, हमारे विद्वान पुरखों ने किये हुए निरीक्षणों के आधार पर निकाला गया सटिक अनुमान..!
दुर्भाग्य से शिक्षा क्षेत्र ने यह प्रयोग आगे नही बढाया. विश्वविद्यालय के फाईलों मे कही दब गया.
पाराशर ऋषि ने बादलों के चार प्रकार का वर्णन किया है.
1 आवर्त
2 समर्थ
3 पुष्कर
4 द्रोण
आवर्तश्चैव संवर्तः पुष्करो द्रोण एव च ।
चत्वरो जलदः प्रोक्ता आवर्तादि यथा क्रमम ।।
(वृष्टीखंडः / 15)
इन बादलों से कब पानी गिर सकता है, या यूं कहे, किस प्रकार के बादल से, किस प्रकार का पानी, और कब गिर सकता, या नही गिर सकता, इसका भी विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है. किसानों ने इन बादलों का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा उन्होने लिखा है-
पाराशर ऋषि ने अधिक अनाज कब आ सकता है यह भी लिखकर रखा है.
चित्रास्वातीविशाखासु ज्यैष्ठेमासी निरभ्रता ।
तास्वेव श्रावणे मासि यदि वर्षति वासवः ।।
तदा संवत्सरो धन्यो बहुशस्य फलप्रदः ।।
(वृष्टिखंडः / 48)
अर्थात, जेठ के माह मे चित्रा, स्वाती, विशाखा नक्षत्रों के समय आसमान निरभ्र होगा, साफ होगा. इन तीन नक्षत्रों के ही समय, सावन माह मे अगर बारिश आती है, तो यह वर्ष अनाज के अधिकतम उत्पादन का वर्ष होता है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि, पाराशर ऋषि ने खेत जोतने के लिए आदर्श हल कैसा होना चाहिये, इसका शास्त्रशुद्ध वर्णन किया है. ‘कृषी पाराशर’ इस ग्रंथ का दुसरा भाग ‘कृषी खंड’ है. इसके 34 वे श्लोक मे उन्होंने हल के आठ प्रमुख अंग बताये है.
ईषायुगहलस्थाणुर्नि यौलस्तस्य पाशिकः ।
अड्डचल्लश्च शौलश्च पच्चनीच हलाष्टकम् ।।
(कृषिखंडः / 34)
अर्थात,
1.ईषा
2.युग
3.हलस्थाणू
4.निर्योल
5.पाशिकाये
6.अड्डचल
7.शौल और
8.पच्चनी
यह हल के आठ अंग है.
ग्रंथ के 35 से 42 श्लोकों मे हल के प्रत्येक अंग का आवश्यक नाप और वर्णन दिया है. आदर्श हल के ‘इंजिनिअरिंग डिटेल्स’ इसमे मिलते है.
‘सर्वोत्तम बीजों के संग्रहण’ को पाराशर ऋषि ने अधिक महत्त्व दिया है. इस ग्रंथ के 900 वर्षों के बाद, संत तुकाराम जी ने कहा है —
शुद्ध बीजापोटी। फळे रसाळ गोमटी ।।
अर्थात, शुद्ध बीज बोने से रसदार फल मिलते है और उत्तम दर्जे का अनाज प्राप्त होता है.
पाराशर ऋषि ने बीजोंसे संबंधित अनेक सूचनाएँ तथा बहुत सी आवश्यक जानकारी भी दी है.
शोषयेदातपे सम्यक् नैवाधो हो विनिधापयेत ।।
(कृषिखंडः / 77)अर्थात, माघ और फाल्गुन माह मे, सभी बीजों का संग्रहण करना चाहिये. उन्हे धूप मे व्यवस्थित सुखाना चाहिए. लेकिन उन्हे नीचे नही रखना चाहिए.
अगले अनेक श्लोकों मे बीज संग्रहण और बीज वपन (अर्थात बीजों को बोना) की शास्त्रशुद्ध जानकारी दी है. अनाज तयार होने के बाद, उसको निकालने की विधि भी विस्तार से दी है.पाराशर ऋषी लिखते है कि, ‘खेती – किसानी करने वाले व्यक्ति को खेती के साथ – साथ आसपास के प्रकृती के स्वभाव की भी पूरी जानकारी होना आवश्यक है.’
आज से 1200 वर्ष पूर्व, अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से होनेवाली खेती के तंत्र का यह डॉक्युमेंटेशन है. विश्व मे सबसे अच्छी खेती भारत कर रहा था और इसलिये समृद्ध था, संपन्न था.
ये हुआ केवल खेती के बारे मे… लेकिन खेती से संबंधित वृक्ष, फलों के पेड, आदि के बारे मे भी हमारे पूर्वजों का वैज्ञानिक ज्ञान जबरदस्त था. वह उन्होने लिखकर भी रखा है.
‘वृक्षायुर्वेद’ इस नाम से अलग अलग कालखंडो मे ग्रंथ लिखे गये है. चाणक्य के कालखंड मे तक्षशिला विश्वविद्यालय जब अपने पूर्ण वैभव पर था तब, अर्थात, आजसे 2400 वर्ष पहले, ‘वृक्षायुर्वेद’ नाम का ग्रंथ, ‘शालीहोत्र’ ने लिखा था. शालीहोत्र मूलतः आद्य पशुचिकित्सकोंमे से एक थे. उनका घोडों से संबंधित अध्ययन सबको आश्चर्यचकित करने वाला हैं. उनके ‘वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ’ मे कुल 12 अध्याय है. भूमी निरुपणा, बीजोत्पविधी, पादप विविक्षा, रोपण विधान… आदी. इसमे उन्होने जहां पेड लगाने है, उस जगह की, उस जमीन की परीक्षा, वहां के अंतर्गत जल स्त्रोतों की जानकारी, दो पेडों के बीच में कितना अंतर होना चाहिये, मृदा का, मिट्टी का वर्गीकरण और विश्लेषण, (परीक्षण और soil selection), नए वृक्षों के लिए जननतंत्र, बीजों पर प्रक्रिया (Seed Treatment), पेडोंपर होने वाले रोग, आदी विषयाोंका विस्तार से वर्णन किया है.
आगे चल कर, पाँचवी सदी मे वराहमहिरने ‘बृहत्संहिता’ मे ‘वृक्षायुर्वेद’ इसी नाम से एक अध्याय लिखा है. इस 55 वे अध्याय मे कुल 31 श्लोक है, जो वृक्ष लगाने और उद्यान के संबंधित विषय का विस्तार से विवेचन करते है.
बादमे ग्यारहवीं सदी मे सूरपाल ने ‘वृक्षायुर्वेद’ इसी नाम से ग्रंथ लिखा, जो प्रसिद्ध है. इसकी ताम्रपट पर लिखी हुई एकही मूल प्रति उपलब्ध है, वह भी ब्रिटन के ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी के बोडेलियन ग्रंथालय मे. इस ग्रंथ मे सुरपाल ने औषधीय पौधों को शास्त्रीय पद्धतीि से कैसे लगाते है, उनके क्या गुणधर्म है, इसके बारे मे विस्तार से लिखा है. इसमे उन्होने तुलसी, नीम, पलाश, जामुन, आंवला आदि अनेक औषधीय वृक्षोंकी जानकारी दी है. कौन से वृक्ष घर के आसपास लगाना चाहिए और कौन से नही लगाना चाहिए, इसकी जानकारी दी है.
मजेदार बात यह है कि, सुरपाल ने बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया कैसी होती हैं, इसका विस्तार से वर्णन किया है. यह आज से 900 वर्ष पहले का ग्रंथ है. इस ग्रंथ के बहुत बाद, पाश्चात्य जगत ने इस प्रक्रिया को ठीक से जाना. Carl Linnaeus जैसे वैज्ञानिकों ने ‘बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया पर काम किया. किंतु हमारे यहा, ग्यारहवी सदी मे, ॠषि सुरपाल ने यह पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई है..!
कुल मिलाकर, हजारो वर्षों से हमारे देश में अत्यंत वैज्ञानिक और शास्त्रशुद्ध पद्धति से खेती की जाती थी. खेती और बारिश का तालमेल उस जमाने मे खोजा गया था. उसी के अनुसार खेती होती थी. इसीलिए विपुल मात्रा मे अनाज निकलता था. आज के जैसे आधुनिक संसाधन ना होते हुए भी, हमारे पुरखोंने यह सब कैसे खोजा होगा, यह आज भी रहस्य है..!