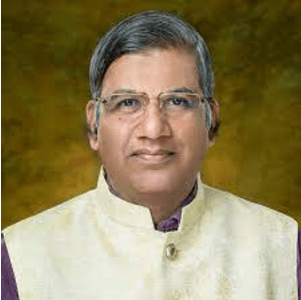भुवनेश्वर। स्थानीय जनता मैदान,जयदेवविहार में मारवाड़ी सोसायटी भुवनेश्वर ने अलग-अलग दो सत्रों में क्रमशः सुबह में होली खेली तथा शाम को होलीबंधु मिलन आयोजित किया जो हरप्रकार से यादगार रहा।आयोजन के आकर्षण का मुख्य केन्द्र मशहूर गायक आदित्य नारायण की सुमधुर गायकी रही। वहीं सम्मानित अतिथि के रुप में बीजेपी,ओड़िशा प्रदेश के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुदर्शन गोयल तथा राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार थे जिनका राजस्थानी परम्परानुसार स्वागत अध्यक्ष संजय लाठ,होली आयोजन कमेटी के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल, संरक्षकः सुरेश अग्रवाल,संरक्षकः सुरेन्द्र कुमार डालमिया,संरक्षकः चेतन टेकरीवाल,उपाध्यक्ष पवन गुप्ता,प्रकाश बेताला आदि द्वारा किया गया।
मारवाड़ी सोसायटी भुवनेश्वर का होली मिलन
हमारा प्राचीन ज्ञान, जिस पर अंग्रेज वैज्ञानिकों ने अपना नाम लिख दिया
रॉबर्ट ओपनहायमर और भारतीय दर्शन
गत वर्ष, अर्थात 2023 के 21 जुलाई को, क्रिस्टोफर नोलन का ‘ओपनहायमर’ यह चलचित्र भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुआ। जे रॉबर्ट ओपनहायमर को सारा विश्व ‘अणुबम’ के जनक के रूप में जानता है। इसलिए, इस सिनेमा के बारे में लोगों के मन में उत्सुकता थी। भारत में यह सिनेमा चर्चित हुआ, वह अलग ही कारणों से। रॉबर्ट ओपनहायमर की भूमिका करने वाला किलीयन मर्फी, फ्लोरेंस बंग के साथ एक अंतरंग दृश्य में, ‘भगवद् गीता’ की कुछ पंक्तियां बोलते हैं, ऐसा एक दृश्य सिनेमा में दिखाया गया था। इस दृश्य के कारण यह सिनेमा भारत में विवादित हुआ, और विवादित होने के कारण हिट भी हुआ। इस दृश्य को छोड़ दे, तो भी सामान्य व्यक्ति के मन में एक बात पक्की बैठ गई कि रॉबर्ट ओपनहायमर भारतीय दर्शन के प्रशंसक थे, अनुगामी थे, और भगवद् गीता का उन्हें गहरा अभ्यास था।
रॉबर्ट ओपनहायमर का जीवन परिचय
रॉबर्ट ओपनहायमर मूलतः अमेरिकी भौतिक शास्त्रज्ञ थे। धर्म से वे ज्यू थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उन्होंने भौतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय से की थी, वर्ष 1927 में। इसी समय उनका परिचय भारतीय दर्शन से हुआ। जर्मन विश्वविद्यालयों में उन दिनों में भी संस्कृत का अध्ययन करने वाले और पढ़ाने वाले अनेक थे, जिससे ओपनहायमर को भारतीय दर्शन, तत्वज्ञान और प्राचीन ग्रंथों में रुचि उत्पन्न हुई।
आगे चलकर ओपनहायमर जब अमेरिका में बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे, तब उन्होंने आर्थर राइडर, एक संस्कृत प्राध्यापक की मदद से अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी विशेष रुचि भगवद् गीता में थी। उनकी राय थी कि, “भगवद् गीता, विश्व के किसी भी भाषा के सबसे सुरीले दर्शन का गीत है”।
उनके अध्ययन टेबल पर भगवद् गीता रखी रहती थी। अपने परिचितों को वह भगवद् गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद भेंट के रूप में देते थे। आगे चलकर उन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस के निकट, अलामोगार्दो में विश्व के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। लॉस अलामोस के ब्रेडबरी साइंस म्यूजियम में, जो ‘यू एस नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर’ है, ओपनहायमर की दो व्यक्तिगत वस्तुएं रखी हैं: एक है कुर्सी, जिस पर बैठकर ओपनहायमर ने परमाणु विखंडन पर काम किया था, और दूसरी है भगवद् गीता की वह प्रतिलिपि (कॉपी), जिसके पहले पृष्ठ पर ओपनहायमर ने अपने आद्याक्षर (initials) लिखे थे।
परमाणु परीक्षण और भगवद् गीता
दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका को परमाणु बम तैयार करने की जल्दी थी। इसलिए, लॉस अलामोस में 1943 के अप्रैल माह में एक प्रयोगशाला (लैब) प्रारंभ की गई, जिसके प्रमुख के रूप में ओपनहायमर की नियुक्ति हुई थी। इस प्रयोगशाला के पास ही, अलामोगार्दो यह परमाणु परीक्षण का स्थान था। विश्व युद्ध के अंतिम चरण में, रॉबर्ट ओपनहायमर ने 16 जुलाई 1945 को, स्थानीय समय अनुसार, प्रात: 5:29 पर अलामोगार्दो में परमाणु का छोटा सा परीक्षण किया। इस परीक्षण को उन्होंने ‘ट्रिनिटी टेस्ट’ नाम दिया।
यह परीक्षण एक जबरदस्त अनुभव था। लॉस अलामोस और आलामोगार्दो यह पूरा रेगिस्तान का प्रदेश है। इस प्रदेश में परीक्षण के समय अत्यंत प्रखर, अत्यंत तेजस्वी प्रकाश और जबरदस्त ऊर्जा का निर्माण हुआ। यह दृश्य देखते ही रॉबर्ट ओपनहायमर को भगवद् गीता के ग्यारहवे अध्याय का 12वां श्लोक याद आया। अर्थात ओपनहायमर को संपूर्ण गीता कंठस्थ थी, और उनका अर्थ भी जानते थे।
ओपनहायमर को जिस श्लोक का स्मरण आया, वह था:
“दिवी सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भाः सद्रृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मा।”
बालमोहन लिमये ने इस श्लोक का अर्थ देते हुए अर्जुनवाडकर जी के ‘गीतार्थ दर्शन’ की पंक्तियाँ दी हैं:
“हजारों सूरज की रोशनी होगी यदि प्रकट आकाश में एक ही समय। तो वह होगी शायद उस रोशनी जैसी जो है उस परमात्मा की।”
ओपनहायमर का भारतीय दर्शन के प्रति आकर्षण
कौरव पांडव युद्ध में अर्जुन को उपदेश करते समय भगवान श्रीकृष्ण जिस प्रकार अपने प्रखर और तेजस्वी रूप में प्रकट होते हैं, ओपनहायमर को परमाणु परीक्षण के समय बिल्कुल वैसा ही अनुभव हुआ। ओपनहायमर भावनाओं में बहकर, कुछ भी बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह विश्व के पदार्थ विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो देखा, वही गीता के श्लोक से जुड़ा हुआ था।
आध्यात्मिक दृष्टि से ओपनहायमर का ज्ञान
ओपनहायमर केवल भगवद् गीता ही नहीं, भृतहरि के ‘शतकत्रय’ जैसे ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। भृतहरि ने सौ – सौ श्लोकों के ‘नीति शतक’, ‘श्रृंगार शतक’, और ‘वैराग्य शतक’ लिखे हैं। ये ग्रंथ जीवन से संबंधित तत्वज्ञान का, दर्शन का, सर्वांगीण विचार करने वाले हैं, और ओपनहायमर ने इन्हें संस्कृत में पढ़ा था।
प्राचीन भारतीय ज्ञान का योगदान
आधुनिक पदार्थ विज्ञान के कई सिद्धांतों के बारे में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही उल्लेखित थे। उदाहरण के तौर पर, ‘इलास्टिसिटी’ (Elasticity) का आविष्कार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1660 में किया था, लेकिन 600-700 साल पहले ‘श्रीधराचार्य’ ने अपनी रचनाओं में इसे स्पष्ट रूप से बताया था। इसी तरह, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व के बारे में भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पहले से जानकारी थी, जो बाद में पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा उद्धृत की गई।
निष्कर्ष
हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली हम ही हैं, जो इन प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को सही तरीके से पहचान नहीं पाते। ओपनहायमर जैसे वैज्ञानिकों का भारतीय ज्ञान पर विश्वास इस बात का प्रतीक है कि हमारे पूर्वजों ने वह ज्ञान प्रदान किया था, जो आज भी आधुनिक विज्ञान में प्रासंगिक है।
एशिया और यूरोप के इतिहास, वर्गीकरण और नामकरण की रोचक गाथा
एशिया और यूरोप का नामकरण कैसे हुआ?
एशिया और यूरोप के नामकरण की कहानी प्राचीन ग्रीक सभ्यता से जुड़ी हुई है।
1. यूरोप का नामकरण:
- यूरोप (Europe) नाम की उत्पत्ति ग्रीक पौराणिक कथाओं से हुई मानी जाती है। एक कथा के अनुसार, “यूरोपा” (Europa) नाम की एक फोनीशियन राजकुमारी थी, जिसे ग्रीक देवता ज़्यूस (Zeus) ने अपहरण कर लिया था और क्रेट (Crete) द्वीप पर ले गए थे। इसी “यूरोपा” नाम से “यूरोप” शब्द आया।
- कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शब्द ग्रीक शब्द “Ευρυ-ωψ” (Eurṓpē) से आया है, जिसका अर्थ है “विस्तृत दृष्टि” (wide gazing) या “चौड़ा चेहरा”।
2. एशिया का नामकरण:
- “एशिया” (Asia) नाम की उत्पत्ति भी ग्रीक सभ्यता से हुई मानी जाती है। प्राचीन यूनानियों ने अनातोलिया (वर्तमान तुर्की का हिस्सा) और उससे आगे के क्षेत्रों को “एशिया” कहा था।
- संभवतः यह नाम अक्कादियन (Akkadian) भाषा के शब्द “Asu” से आया है, जिसका अर्थ “पूर्व” (east) होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नाम ही पूरे महाद्वीप के लिए बाद में इस्तेमाल होने लगा।
एशिया और यूरोप के बीच की सीमा कैसे तय की गई?
एशिया और यूरोप के बीच की सीमा तय करना ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से एक जटिल प्रक्रिया रही है।
प्राकृतिक सीमाएं:
- उरल पर्वत (Ural Mountains) – रूस में स्थित
- उरल नदी (Ural River)
- कॉकसस पर्वत (Caucasus Mountains)
- काला सागर (Black Sea)
- बॉस्फोरस जलडमरूमध्य (Bosphorus Strait) – जो तुर्की को यूरोप और एशिया में बांटता है
ऐतिहासिक निर्णय:
- प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा था – यूरोप और एशिया।
- आधुनिक समय में, रूस और तुर्की जैसे कुछ देश ऐसे हैं, जो दोनों महाद्वीपों में आते हैं (ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश)।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से भी कुछ देशों को यूरोप या एशिया में रखा गया, जैसे कि जॉर्जिया और आर्मेनिया को सांस्कृतिक रूप से यूरोपीय माना जाता है, लेकिन वे भूगोल में एशिया में हैं।
एशियाई और यूरोपीय देशों का वर्गीकरण कैसे किया गया?
देशों का वर्गीकरण मुख्य रूप से भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक कारणों के आधार पर किया गया है।
1. भौगोलिक आधार पर:
- एशिया और यूरोप को उरल पर्वत, उरल नदी, कॉकसस पर्वत, काला सागर और बॉस्फोरस जलडमरूमध्य के माध्यम से विभाजित किया गया है।
- तुर्की, रूस, कज़ाखस्तान, अज़रबैजान और जॉर्जिया कुछ ऐसे देश हैं, जिनका भूभाग दोनों महाद्वीपों में पड़ता है।
2. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर:
- ईसाई बहुल देशों को आमतौर पर यूरोप से जोड़ा गया है, जबकि बौद्ध, हिंदू, इस्लामिक और अन्य एशियाई संस्कृतियों वाले देशों को एशिया में रखा गया है।
- हालांकि, यह विभाजन हमेशा सटीक नहीं होता, क्योंकि कई एशियाई देशों में ईसाई समुदाय भी हैं, जैसे कि फिलीपींस और लेबनान।
3. राजनीतिक आधार पर:
- संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी देशों का वर्गीकरण किया गया है।
एशियाई देश (Asia के अंतर्गत आने वाले देश)
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एशिया को पांच क्षेत्रों में बांटा जाता है:
1. पूर्वी एशिया (East Asia):
- चीन
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- उत्तर कोरिया
- ताइवान
- मंगोलिया
2. दक्षिण एशिया (South Asia):
- भारत
- पाकिस्तान
- बांग्लादेश
- नेपाल
- भूटान
- श्रीलंका
- मालदीव
3. दक्षिण-पूर्व एशिया (Southeast Asia):
- इंडोनेशिया
- थाईलैंड
- मलेशिया
- वियतनाम
- फिलीपींस
- म्यांमार (बर्मा)
- कंबोडिया
- लाओस
- सिंगापुर
- ब्रुनेई
- तिमोर-लेस्ते
4. मध्य एशिया (Central Asia):
- कजाखस्तान
- उज़्बेकिस्तान
- तुर्कमेनिस्तान
- किर्गिस्तान
- ताजिकिस्तान
5. पश्चिम एशिया (Middle East या पश्चिमी एशिया):
- सऊदी अरब
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- ईरान
- इराक
- सीरिया
- लेबनान
- जॉर्डन
- इज़राइल
- फिलिस्तीन
- यमन
- ओमान
- कुवैत
- बहरीन
- कतर
- तुर्की (तुर्की का कुछ भाग एशिया में, कुछ यूरोप में है)
- आर्मेनिया
- अज़रबैजान
- जॉर्जिया
यूरोपीय देश (Europe के अंतर्गत आने वाले देश)
यूरोप को भी भौगोलिक रूप से पाँच हिस्सों में बांटा गया है:
1. उत्तरी यूरोप (Northern Europe):
- डेनमार्क
- फिनलैंड
- आइसलैंड
- नॉर्वे
- स्वीडन
- एस्टोनिया
- लातविया
- लिथुआनिया
2. पश्चिमी यूरोप (Western Europe):
- ऑस्ट्रिया
- बेल्जियम
- फ्रांस
- जर्मनी
- लिकटेंस्टीन
- लक्समबर्ग
- मोनाको
- नीदरलैंड्स
- स्विट्जरलैंड
3. पूर्वी यूरोप (Eastern Europe):
- बेलारूस
- बुल्गारिया
- चेक गणराज्य
- हंगरी
- मोल्दोवा
- पोलैंड
- रोमानिया
- रूस (पश्चिमी भाग यूरोप में, पूर्वी भाग एशिया में)
- स्लोवाकिया
- यूक्रेन
4. दक्षिणी यूरोप (Southern Europe):
- क्रोएशिया
- ग्रीस
- इटली
- माल्टा
- पुर्तगाल
- सैन मैरिनो
- स्लोवेनिया
- स्पेन
- वेटिकन सिटी
5. दक्षिण-पूर्वी यूरोप (Balkans and Southeast Europe):
- अल्बानिया
- बोस्निया और हर्जेगोविना
- सर्बिया
- मोंटेनेग्रो
- उत्तरी मैसिडोनिया
- कोसोवो
कुछ देश जो दोनों महाद्वीपों में आते हैं (Transcontinental Countries)
कुछ देश ऐसे हैं जिनका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में आता है, जैसे:
- रूस – यूरोप और एशिया दोनों में फैला है।
- तुर्की – इसका पश्चिमी भाग यूरोप में और पूर्वी भाग एशिया में आता है।
- कज़ाखस्तान – इसका एक छोटा हिस्सा यूरोप में आता है।
- अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया – भूगोल के हिसाब से एशिया में, लेकिन संस्कृति और राजनीति के आधार पर यूरोप से जुड़े हैं।
सूरज के रहस्यों को जानने की जिद
मधुलिका गुहाठाकुर्ता नासा (नेशनल एयोरनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) मुख्यालय में प्रोग्राम साइंटिस्ट और नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के हेलियोफीजिक्स डिवीजन की नई पहलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार हैं। पिछले दो दशकों से गुहाठाकुर्ता ने हेलियोफीजिक्स के विकास को समन्वित विज्ञान विषय बनाने में किए गए प्रयासों का नेतृत्व किया है।
गुहाठाकुर्ता 16 वर्षों तक नासा के लिविंग विद ए स्टार (एलडब्लूएस) प्रोग्राम की लीड प्रोग्राम साइंटिस्ट रही जिसमें सौर विकिरण में बदलाव और पृथ्वी पर उसके असर का अध्ययन किया गया। एलडब्लूएस प्रोग्राम के लीड के नाते गुहाठाकुर्ता ने सोलर डायनमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी, जिससे सूर्य को और करीब से देखने में मदद मिली, सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी, जिसने हमें सूर्य की पहली 3 डी तस्वीर दी और हाल ही में सोलर ऑरबिटर मिशन- जो कि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिशन है, जैसे प्रमुख मिशनों के विकास कार्य पर निगाह रखी। इन सभी मिशनों से हमें सौर प्रणाली और सूर्य के उस पर प्रभाव एवं सूर्य के बारे में हमारी समझ को लेकर क्रांतिकारी जानकारियां सामने आईं।
गुहाठाकुर्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से खगोल भौतिकी विषय में मास्टर्स डिग्री हासिल की है, जबकि डेनेवर यूनिवर्सिटी, कलैराडो से उन्होंने सोलर फिजिक्स में पीएच.डी. की है।
प्रस्तुत हैं उनसे साक्षात्कार के मुख्य अंश:
क्या आप हमें अपने नासा तक पहुंचने की शैक्षिक और पेशेवर यात्रा के बारे में कुछ बताएंगीं?
यह एक लंबी यात्रा थी। भारत में बड़ी होती एक छोटी लड़की के रूप में मैंने चांद पर मानव के कदमों को पड़ते देखा। उन दिनों में मेरे मन में अमेरिका, नासा और यहां तक कि विज्ञान अपने आप में महज अवधारणाएं हुआ करते थे। अब जबकि मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं अपने आपको उस संगठन का अभिन्न हिस्सा पाती हूं। और विज्ञान के माध्यम से हम हर दिन कुछ न कुछ नई खोज करते हैं, हम अंतरिक्ष में गए हैं और सूर्य को भी हमने छू लिया है।
जो चीजें कभी स्कूल जाने वाली एक छोटी भारतीय लड़की के लिए बहुत बड़ी और अजेय दिखा करती थीं, वे अब मेरे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। मुझे ऐसा करने का सौभाग्य अपने शानदार और प्रतिभाशाली सहयोगियों के साथ की वजह से मिला- इसमें हर तरह और विभिन्न दृष्टिकोण के लोग हैं।
आपने खगोल भौतिकी के अध्ययन का विकल्प ही क्यों चुना?
बहुत पहले, शायद मेरी दादी के गुजर जाने के बाद मुझे बताया गया कि वह आसमान में एक तारा बन गई हैं, तभी से मैंने रात में आकाश को निहारना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं लगातार अपने पिता से पूछा करती थी कि, ‘‘हम कहां से आते हैं?’’ और ‘‘मरने के बाद क्या होता है?’’ मेरे पिता भरसक कोशिश करते थे कि मुंह बंद कराने के बजाए 6 साल की बच्ची को तार्किक तरीके से समझाया जा सके। उन्होंने एक गोला यानी एक वृत्त बनाया और मुझसे पूछा कि, ‘‘क्या तुम मुझे यह बता सकती हो इस गोले की शुरुआत कहां से हो रही है और यह खत्म कहां हो रहा है।?’’ बस यही बात में जहन में अटक गई।
पहेलियां सुलझाना, खेल खेलना, डायनासोर के बारे में पढ़ना, तारामंडलों की यात्रा, रात में आकाश को निहारना- मेरे आसपास की दुनिया ने मुझे वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। बड़े होने पर मुझे ब्रह्मांड विज्ञान ने भी आकर्षित किया- मुझे विज्ञान को दर्शन और अध्यात्म से जोड़ना बहुत पसंद था।
क्या आप हमें लिविंग विद ए स्टार पहल में अपने काम के बारे में बताएंगीं?
पिछले दो दशकों से, मैंने हेलियोफीजिक्स के विकास को विज्ञान के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्य कर दिया है, जिसकी वजह से अपने ब्रह्मांड के बारे में मलभूत खोजों का सीधा लाभ समाज को उपलब्ध होता है। लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम की लीड होने के कारण, मैंने, कई प्रमुख मिशनों की सफलता में योगदान दिया है। इनमें, पृथ्वी की विकिरण परिधि में खतरनाक ऊर्जा कणों से संबंधित वैन एलेन पड़ताल और पार्कर सोलर पड़ताल के माध्यम से सूर्य को छूने जैसे मिशन शामिल हैं।
नवाचार और वैज्ञानिक खोज में तेजी लाने के मकसद से, मैंने पारंपरिक अध्ययन क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों को उनके दायरे से बाहर ले जाते हुए उनके लिए फंडिंग व्यवस्था को तैयार करने में मदद दी। हमारे पास अब एलडब्लूएस सिस्टम है जिसे लक्षित शोध और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और अपने लक्ष्य पर केंद्रित वैज्ञानिकों की उस टीम के रूप में जाना जाता है जो प्रतिस्पर्धी तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक विचारों और तकनीक की साझेदारी वाले सहयोगी माहौल को प्रोत्साहित करती है।
हेलियोफीजिक्स के क्षेत्र में अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने वालों को तैयार करने की दृष्टि से मैंने जैक एडी फेलोशिप प्रोग्राम को बनाने में मदद की, जो होनहार शोधकर्ताओं के पेशेवर विकास का महत्पूर्ण चैनल बनने के साथ कई महिला वैज्ञानिकों के कॅरियर को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।
क्या आपको एक महिला होने के कारण स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स) के अध्ययन को लेकर किसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा?
मैं यह कहने में असहज महसूस कर रही हूं कि एक महिला होने के नाते मेरे साथ भेदभाव किया गया। अपने अधिकतकर जीवन में मैंने इसके बारे में सक्रियता के साथ नहीं सोचा, न ही मेरे पास इस सब के लिए वक्त है। आपके पास यह सब देखने और सोचने के लिए ठहराव होना चाहिए कि यह सब भी हो रहा है। पिछले कई सालों में बहुत-सी चीजें बदली हैं। सिर्फ नासा ही नहीं, बल्कि पूरा देश- अमेरिका ही बदल रहा है। हम उसका प्रतिबिंब नासा में भी देखते है, और यह एक सच्चाई है। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि विज्ञान और सभी जगहों पर अनजाने में ही सही लेकिन बहुत से पूर्वाग्रह मौजूद हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि, महिलाओं का सहानुभूति पक्ष उन्हें हर चीज़ की बड़ी और गहरी समझ विकसित करने में मदद देता है, चाहे बात किसी वैज्ञानिक उद्यम की हो, या फिर परिवार या दुनिया की हो।
आप उन महिलाओं और पुरुषों को क्या सलाह देना चाहेंगी, जो स्टेम क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाने के इच्छुक हैं?
मैं सोचती हूं कि, स्टेम एक विशिष्ट क्षेत्र है- यहां असंभव रोजाना हकीकत में बदलता रहता है। विज्ञान और गणित में काम करने का आनंद लें। पहेलियों, खेलों, व्यावहारिक गतिविधियों, संग्रहालयों की यात्रा और तारामंडलों के शो का आनंद लें। अपने आसपास की दुनिया में हर चीज़ को लेकर जिज्ञासु रहें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। सबसे मुश्किल काम पहला कदम उठाने का होता है, जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। छोटे-छोटे कदम उठाएं- अपने को नए माहौल में ढालें, कुछ ऐसा काम करें जिसे करने में आप घबराते हों, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए कोई सुरक्षित विकल्प न चुनें।
नतासा मिलास स्वतंत्र लेखिका हैं और न्यू यॉर्क सिटी में रहती हैं।
वीर छत्रपति शम्भा जी की गौरवगाथा
(11 मार्च को बलिदान दिवस पर विशेष )
वीर शिवाजी के पुत्र वीर शम्भा जी का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। आप वीर शिवाजी के साथ अल्पायु में औरंगजेब की कैद में आगरे के किले में बंद भी रहे थे। आपने 11 मार्च 1689 को वीरगति प्राप्त की थी। इस लेख में वीर शम्भाजी जी के उस महान और प्रेरणादायक जीवन के हमें दर्शन होते है जिसका वर्णन इतिहासकार प्राय: नहीं करते।
औरंगजेब के जासूसों ने सुचना दी की शम्भा जी इस समय आपने पाँच-दस सैनिकों के साथ वारद्वारी से रायगढ़ की ओर जा रहे है। बीजापुर और गोलकुंडा की विजय में औरंगजेब को शेख निजाम के नाम से एक सरदार भी मिला जिसे उसने मुकर्रब की उपाधि से नवाजा था। मुकर्रब अत्यंत क्रूर और मतान्ध था। शम्भा जी के विषय में सुचना मिलते ही उसकी बाछे खिल उठी। वह दौड़ पड़ा रायगढ़ की ओर। शम्भा जी आपने मित्र कवि कलश के साथ इस समय संगमेश्वर पहुँच चुके थे। वह एक बाड़ी में बैठे थे की उन्होंने देखा कवि कलश भागे चले आ रहे है और उनके हाथ से रक्त बह रहा है। कलश ने शम्भा जी से कुछ भी नहीं बोला। बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाड़ी के तलघर में ले गए। परन्तु उन्हें तलघर में घुसते हुए मुकर्रब खान के पुत्र ने देख लिया था। शीघ्र ही मराठा रणबांकुरों को बंदी बना लिया गया। शम्भा जी व कवि कलश को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर मुकर्रब खान के सामने लाया गया। वह उन्हें देखकर खुशी से नाच उठा। दोनों वीरों को बोरों के समान हाथी पर लादकर मुस्लिम सेना बादशाह औरंगजेब की छावनी की और चल पड़ी।
औरंगजेब को जब यह समाचार मिला, तो वह ख़ुशी से झूम उठा। उसने चार मील की दूरी पर उन शाही कैदियों को रुकवाया। वहां शम्भा जी और कवि कलश को रंग बिरंगे कपडे और विदूषकों जैसी घुंघरूदार लम्बी टोपी पहनाई गयी। फिर उन्हें ऊँट पर बैठा कर गाजे बाजे के साथ औरंगजेब की छावनी पर लाया गया। औरंगजेब ने बड़े ही अपशब्द शब्दों में उनका स्वागत किया। शम्भा जी के नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, परन्तु वह शांत रहे। उन्हें बंदी ग्रह भेज दिया गया। औरंगजेब ने शम्भा जी का वध करने से पहले उन्हें इस्लाम काबुल करने का न्योता देने के लिए रूह्ल्ला खान को भेजा।
नर केसरी लोहे के सीखचों में बंद था। कल तक जो मराठों का सम्राट था। आज उसकी दशा देखकर करुणा को भी दया आ जाये। फटे हुए चिथड़ों में लिप्त हुआ उनका शरीर मिट्टी में पड़े हुए स्वर्ण के समान हो गया था। उन्हें स्वर्ग में खड़े हुए छत्रपति शिवाजी टकटकी बंधे हुए देख रहे थे। पिता जी पिता जी वे चिल्ला उठे- मैं आपका पुत्र हूँ। निश्चित रहिये। मैं मर जाऊँगा लेकिन…..
लेकिन क्या शम्भा जी …रूह्ल्ला खान ने एक और से प्रकट होते हुए कहां।
तुम मरने से बच सकते हो शम्भा जी। परन्तु एक शर्त पर।
शम्भा जी ने उत्तर दिया में उन शर्तों को सुनना ही नहीं चाहता। शिवाजी का पुत्र मरने से कब डरता है।
लेकिन जिस प्रकार तुम्हारी मौत यहाँ होगी उसे देखकर तो खुद मौत भी थर्रा उठेगी शम्भा जी- रुहल्ला खान ने कहा।
कोई चिंता नहीं , उस जैसी मौत भी हम हिन्दुओं को नहीं डरा सकती। संभव है कि तुम जैसे कायर ही उससे डर जाते हो। शम्भा जी ने उत्तर दिया।
लेकिन… रुहल्ला खान बोला वह शर्त है बड़ी मामूली। तुझे बस इस्लाम कबूल करना है। तेरी जान बक्श दी जाएगी। शम्भा जी बोले बस रुहल्ला खान आगे एक भी शब्द मत निकालना मलेच्छ। रुहल्ला खान अट्टहास लगाते हुए वहाँ से चला गया।
उस रात लोहे की तपती हुई सलाखों से शम्भा जी की दोनों आँखें फोड़ दी गई। उन्हें खाना और पानी भी देना बंद कर दिया गया।
आखिर 11 मार्च को वीर शम्भा जी के बलिदान का दिन आ गया। सबसे पहले शम्भा जी का एक हाथ काटा गया, फिर दूसरा, फिर एक पैर को काटा गया और फिर दूसरा पैर। शम्भा जी कर पाद-विहीन धड़ दिन भर खून की तलैया में तैरता रहा। फिर सायंकाल में उनका सर काट दिया गया और उनका शरीर कुत्तों के आगे डाल दिया गया। फिर भाले पर उनके सर को टांगकर सेना के सामने उसे घुमाया गया और बाद में कूड़े में फेंक दिया गया।
मराठों ने अपनी छातियों पर पत्थर रखकर आपने सम्राट के सर का इंद्रायणी और भीमा के संगम पर तुलापुर में दाह संस्कार कर दिया गया। आज भी उस स्थान पर शम्भा जी की समाधि है। जो पुकार पुकार कर वीर शम्भा जी की याद दिलाती है कि हम सर कटा सकते है पर अपना प्यारे वैदिक धर्म कभी नहीं छोड़ सकते।
मित्रों शिवाजी के तेजस्वी पुत्र शंभाजी के अमर बलिदान यह गाथा हिन्दू माताएं अपनी लोरियों में बच्चों को सुनाये तो हर घर से महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महान वीर जन्मेंगे। इतिहास के इन महान वीरों के बलिदान के कारण ही आज हम गर्व से अपने आपको श्री राम और श्री कृष्ण की संतान कहने का गर्व करते है। आइये आज हम प्रण ले हम उसी वीरों के पथ के अनुगामी बनेंगे।
बोलो वीर छत्रपति शिवाजी की जय।
बोलो वीर छत्रपति शम्भा जी की जय।।
तमिल भाषा का हिंदी/संस्कृत से सम्बन्ध
केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। उस नीति के अंतर्गत त्रिभाषा का प्रावधान रखा गया था। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त मातृभाषा/प्रादेशिक भाषा का प्रावधान रखा गया। दक्षिण भारतीय प्रदेशों के कुछ अवसरवादी नेताओं ने इसे तमिलनाडु पर हिंदी थोपने के फतवा करार दिया। पूर्व में भी हिंदी विरोधी लहर तमिलनाडु में राजनेताओं ने चलाई थी। जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा था तब भी तमिलनाडु के राजनेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसका विरोध किया था। सभी जानते है कि तमिलनाडु आर्य-द्रविड़ की विभाजनकारी मानसिकता का केंद्र रहा है। वहां के राजनेता जनता को द्रविड़ संस्कृति के नाम पर भड़काते हैं। वे कहते है कि द्रविड़ संस्कृति, तमिल भाषा हमारी मूल पहचान है। विदेशी आर्यों ने अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी है। उनका यह भी कहना है कि तमिल भाषा एक स्वतंत्र भाषा है एवं उसका संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं है। संस्कृत आर्यों की भाषा है जिसे द्रविड़ों पर थोपा गया है।
एक सामान्य शंका मेरे मस्तिष्क में सदा रहती है कि तमिल राजनेता हिंदी/संस्कृत का विदेशी भाषा कहकर विरोध करते है परन्तु इसके विपरीत अंग्रेजी का समर्थन करते है। क्या अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति तमिलनाडु के किसी गाँव में हुई थी ? नहीं। फिर यह केवल एक प्रकार की जिद है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध कैसे प्रारम्भ हुआ? इस शंका के समाधान के लिए हमें तमिलनाडु के इतिहास को जानना होगा। रोबर्ट कालद्वेल्ल (Robert Caldwell -1814 -1891 ) के नाम से ईसाई मिश्नरी को इस मतभेद का जनक माना जाता है। रोबर्ट कालद्वेल्ल ने भारत आकर तमिल भाषा पर व्याप्त अधिकार कर किया और उनकी पुस्तक A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages, Harrison: London, 1856 में प्रकाशित हुई थी।
इस पुस्तक का उद्देश्य तमिलनाडु का गैर ब्राह्मण जनता को ब्राह्मण विरोधी, संस्कृत विरोधी, हिंदी विरोधी, वेद विरोधी एवं उत्तर भारतीय विरोधी बनाना था। जिससे उन्हें भड़का कर आसानी से ईसाई मत में परिवर्तित किया जा सके और इस कार्य में रोबर्ट कालद्वेल्ल को सफलता भी मिली। पूर्व मुख्य मंत्री करूणानिधि के अनुसार इस पुस्तक में लिखा है कि संस्कृत भाषा के 20 शब्द तमिल भाषा में पहले से ही मिलते है। जिससे यह सिद्ध होता हैं की तमिल भाषा संस्कृत से पहले विद्यमान थी। तमिलनाडु की राजनीती ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण धुरों पर लड़ी जाती रही हैं। इसीलिए इस पुस्तक को आधार बनाकर हिंदी विरोधी आंदोलन चलाये गए। विडंबना देखिये कि भाई भाई में भेद डालने वाले रोबर्ट कालद्वेल्ल की मूर्ति को मद्रास के मरीना बीच पर स्थापित किया गया है। उसकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।
जहाँ तक तमिल और संस्कृत भाषा में सम्बन्ध का प्रश्न है तो संस्कृत और तमिल में वैसा ही सम्बन्ध है जैसा एक माँ और बेटे में होता है। जैसा सम्बन्ध संस्कृत और विश्व की अन्य भाषाओँ में हैं। संस्कृत जैसे विश्व की अन्य भाषाओं की जननी है वैसे ही तमिल की भी जननी है। अनुसन्धान करने पर हमें मालूम चलता है कि प्राचीन तमिल ग्रंथों में विशेष रूप से तमिल काव्य में बहुत से संस्कृत के शब्द प्रयुक्त किये गए है। यहाँ तक कि तमिल की बोलचाल की भाषा तो संस्कृत-शब्दों से भरी पड़ी है। कम्ब रामायण में भी अपभ्रंश रूप से अनेक संस्कृत शब्द मिल जायेंगे। तमिल भाषा की लिपि में अक्षर कम होने के कारण संस्कृत के शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखे जाते। इसलिए अलग लिपि बन गई।
“तमिल स्वयं शिक्षक” से तमिल, संस्कृत,हिंदी के कुछ शब्दों में समानता
तमिल संस्कृत हिंदी
1. वार्ते वार्ता बात
2. ग्रामम् ग्राम: गांव
3. जलम् जलम् जल
4. दूरम् दूरम् दूर
5. मात्रम् मात्रम् मात्र
6. शीग्रम शीघ्रम शीघ्र
7. समाचारम समाचार: समाचार
इस प्रकार के अनेक उदहारण तमिल, संस्कृत और हिंदी में “तमिल स्वयं शिक्षक” से समानता के दिए जा सकते हैं।
इसी प्रकार से “तमिल लैक्सिकान” के नाम से तमिल के प्रामाणिक कोष को देखने से भी यही ज्ञात होता है कि तमिल भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द विद्यमान है। तमिल वेद के नाम से प्रसिद्द त्रिक्कुरल , संत तिरुवल्लुवार द्वारा प्रणीत ग्रन्थ के हिंदी संस्करण की भूमिका में माननीय चक्रबर्ती राजगोपालाचारी लिखते है कि ‘इस पुस्तक को पढ़कर उत्तर भारतवासी जानेंगे की उत्तरी सभ्यता और संस्कृति का तमिल जाति से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध और तादात्म्य हैं’। इस ग्रन्थ में अनेक वाक्य वेदों के उपदेश का स्पष्ट अनुवाद प्रतीत होते है। तमिल के प्रसिद्द कवि भारतियार की काव्य में भी संस्कृत शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्द संगम काल के साहित्य में संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों प्रभाव स्पष्ट रूप से मिलता हैं।
एक अन्य उदहारण देखिये। तिरुक्कुल को तमिल वेद भी कहा जाता है। इसके लेखक तिरुवल्लुवर को ऋषि कह कर सम्मानित किया जाता है।
इसे पढ़ कर लगा कि तिरुक्कुल और मनुस्मृति आदि वैदिक ग्रन्थों में बहुत अधिक समानता है। तिरुक्कुल का रचनाकाल 300 इस्वी पूर्व (300 BC) माना जाता है। कुछ लोग इसका समय इतना पुराना नहीं मानते। परन्तु इस बात पर सभी सहमत हैं कि यह तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में से एक है। मनु स्मृति इससे भी बहुत प्राचीन है। आश्चर्य है वेद की तरह इसमें भी कोई पाठभेद नहीं है।
.
मनु स्मृति और तिरुक्कुल की तुलना (कोष्ठक में संख्या तुरुक्कुल के पद्य की संख्या है)
1-
संन्यास और ब्राह्मण
तिरुक्कुल- सदाचार पर चलकर संन्यास ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ है. (21 ) मुक्ति के लिए संन्यास ग्रहण करे (22)
मनुस्मृति – सन्यासी का धर्म है कि मुक्ति के लिए इन्द्रियों को दुराचार से रोक कर सभी जीवों पर दया करे।
2- गृहस्थ
तिरुक्कुल- गृहस्थ अन्य 3 आश्रमों के धर्माकुल जीवन जीने में सहायक होता है। (41) धन करते समय पाप से बचे और खर्च करते समय बाँट कर प्रयोग करे। (44) नियमानुसार गृहस्थ जीवन जीने वाला सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है। (46)
.
मनुस्मृति- जिसके दान से 3 आश्रमों का जीवन चलता है वह गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। जैसे सभी वायु के आश्रित होते हैं वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ के आश्रित है। गृहस्थ धर्मानुकुल धन का संचय करे।
यह केवल दिग्दर्शन मात्र है। इस विषय पर पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है।
इतिहास के अनुसार पूर्वकाल में दक्षिण भारत से जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में व्यापारिक, राजनीतिक, संस्कृति एवं धार्मिक सम्बन्ध थे। भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी उन देशों की संस्कृति में स्पष्ट रूप से दीखता है। तमिलनाडु से न केवल व्यापारी उन देशों में जाते थे। अपितु संस्कृति का प्रचार बी होता था। इस सम्बन्ध के लिए प्रयोग होने वाली भाषा कोई अन्य नहीं अपितु संस्कृत ही थी। इस प्रमाण जावा देश में 1768 तक मनुस्मृति के आधार पर प्रचलित विधि-विधान से मिलता है।(सन्दर्भ- Arnold Thomas, the Preaching of Islam, p.385)। मनुस्मृति संस्कृत में है। इससे यही सिद्ध हुआ कि उस काल में तमिलनाडु में धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का व्यापक रूप में प्रचलन था।
संस्कृत भाषा और विश्व की अन्य में सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए पूर्व में कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई है जैसे पंडित धर्मदेव विद्यामार्तंड द्वारा रचित वेदों का यथार्थ स्वरुप, Sanskrit-The Mother of all World Languages, पंडित भगवददृत्त जी द्वारा लिखित भाषा का इतिहास अदि। संस्कृत को विश्व की समस्त भाषाओं की जननी सिद्ध करने के लिए अनुसन्धान कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फुट डालो और राज करो की विभाजनकारी मानसिकता का प्रतिउत्तर सम्पूर्ण देश को हिंदी भाषा के सूत्र से जोड़ना ही है। यही स्वामी दयानंद की मनोकामना थी। आर्यसमाज को भाषा वैज्ञानिकों की सहायता से रोबर्ट कालद्वेल्ल की पुस्तक की तर्कपूर्ण समीक्षा छपवा कर उसे तमिलनाडु में प्रचारित करवाना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है।

(लेखक ने हिंदी भाषी होते हुए अपने जीवन के 6 वर्ष तमिलनाडु में व्यतीत किये हैं एवं तमिल भाषा से परिचित है।)
होली का वास्तविक स्वरुप
इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासन्ती नव सस्येष्टि है अर्थात् बसन्त ऋतु के नये अनाजों से किया हुआ यज्ञ, परन्तु होली होलक का अपभ्रंश है।
यथा–
तृणाग्निं भ्रष्टार्थ पक्वशमी धान्य होलक: (शब्द कल्पद्रुम कोष) अर्धपक्वशमी धान्यैस्तृण भ्रष्टैश्च होलक: होलकोऽल्पानिलो मेद: कफ दोष श्रमापह।(भाव प्रकाश)
अर्थात्―तिनके की अग्नि में भुने हुए (अधपके) शमो-धान्य (फली वाले अन्न) को होलक कहते हैं। यह होलक वात-पित्त-कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है।
अग्निवै देवानाम मुखं अर्थात् अग्नि देवों–पितरों का मुख है जो अन्नादि शाकल्यादि आग में डाला जायेगा। वह सूक्ष्म होकर पितरों देवों को प्राप्त होगा।
साभार- https://www.
#HappyHoli
एक पूर्व मुसिल्म की नजर से इस्लाम की हकीकत
“Let us visit the mosque, see live namaz (prayer) and understand Islam” अहमदाबाद की एक मस्जिद ने गैर मुसलमानों से यह आग्रह किया है कि आप मस्जिद आईये और इस्लाम के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिये। उनका मानना है कि इस्लाम के विषय में गैर मुसलमानों में भ्रांतियां बहुत अधिक हैं। उन्हें दूर करने के लिए मस्जिदों के माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान की अत्यंत आवश्यकता है। विभिन्न मत-मतान्तर में परस्पर संवाद बहुत अच्छी परम्परा हैं। यह वस्तुत: प्राचीन दर्शन है। जहाँ पर विद्वान् आपस में शास्त्र चर्चा के माध्यम से सत्य विचारों का समर्थन और असत्य का असमर्थन करते थे। जबकि इस्लामिक परिपाटी में मज़हब के मामले में अक्ल का दख़ल नहीं जैसे विचारों को प्रमुखता दी गई है। आधुनिक भारत में परस्पर संवाद को स्थापित करने का श्रेय स्वामी दयानन्द को जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में अनेक हिन्दू पंडितों, मुसलिम विचारकों और मौलानाओं, ईसाई पादरियों से उन्हीं के धर्म/मत विशेष की पुस्तकों पर वेदों की मान्यताओं के आधार पर संवाद किया। स्वामी जी ऐसा करते हुए स्पष्ट रूप से सत्यार्थ प्रकाश में घोषणा करते है कि
-“मैं पुराण, जैनियों की पुस्तकों, बाइबिल व क़ुरान को पहले ही से कुदृष्टि से न देखकर उनके सद्गुणों को स्वीकार वह दुर्गुणों का परित्याग करता हूँ।”
-मेरी किसी नूतन विचार या मत को प्रवर्तन करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। अपितु जो सत्य है उसको मानना व मनवाना और जो जुठ है उसको छोड़ना वह छुड़वाना मेरा उद्देश्य है।
-जब तक मनुष्य सत्य-असत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य नहीं बढ़ाते तब तक स्थूल और सूक्षम खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकते।
-जो विभिन्न मत-मतान्तरों के परस्पर विरोधी विवाद हैं उनको मैं पसंद नहीं करता, क्यूंकि इन्हीं मतवादियों ने अपने मतों का प्रचार करके वह लोगों को उनमें फंसाकर एक दूसरे का शत्रु बना दिया है।
– ऐसे ही अपने अपनी मत-मतान्तरों के सम्बन्ध में सब कहते हैं कि हमारा ही मत सच्चा है, शेष सब बुरे हैं। हमारे मत द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है. अन्यों के द्वारा नहीं हो सकती। ….हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण, अहिंसा, दया आदि शुभगुण सब मतों में अच्छे हैं और शेष झगड़ा बखेड़ा ईर्ष्या, घृणा, मिथ्याभाषण आदि कर्म सभी मतों में बुरे हैं। यदि तुमको सत्य धर्म स्वीकार करने की इच्छा हो तो वैदिक धर्म को ग्रहण करो।
हम भी अपने मुसलमान भाईयों से प्रार्थना करेंगे कि वे स्वामी दयानन्द द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के 14 वे समुल्लास में इस्लाम की मान्यताओं पर उठाई गई शंकाओं का समाधान करें। तभी उनकी इस मुहीम को सार्थक प्रयास कहा जायेगा। यह शंकाएं पिछले 130 वर्षों से लंबित हैं।
1. इस्लाम में खुदा को दयालु बताया गया है जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं दीखता। देखें-
क़ुरान -सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात् पालन करनेहारा है सब संसार का।। क्षमा करने वाला दयालु है ।।
-मं० १। सि० १। सूरतुल्फातिहा आयत १। २।।
स्वामी दयानन्द इसकी समीक्षा करते हुए लिखते है- जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेहारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि “काफिरों को कतल करो” अर्थात् जो कुरान और पैगम्बर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता ? इसलिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता।
2. ईश्वर का कार्य क्या दिलों के रोगों को बढ़ाना है ? नहीं। फिर क़ुरान का खुदा ऐसा क्यों करता है? देखें-
क़ुरान-उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने उन का रोग बढ़ा दिया।।-मं० १। सि० १। सू० २। आ० १०।।
(समीक्षक) भला विना अपराध खुदा ने उन का रोग बढ़ाया, दया न आई, उन बिचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा! क्या यह शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं है? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना, यह खुदा का काम नहीं हो सकता क्योंकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है।।
3. इस्लाम की बहिश्त में ऐसा क्या विशेष था जो पृथ्वी पर नहीं है। देखें-
क़ुरान-और आनन्द का सन्देशा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे। यह कि उन के वास्ते बहिश्तें हैं जिन के नीचे से चलती हैं नहरें। जब उन में से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि यह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इस से दिये गये थे—— और उन के लिये पवित्र बीवियाँ सदैव वहाँ रहने वाली हैं।। -मं० १। सि० १। सू० २। आ० २५।।
(समीक्षक) भला! यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं। किन्तु यहाँ की स्त्रियाँ सदा नहीं रहतीं और वहाँ बीवियाँ अर्थात् उत्तम स्त्रियाँ सदा काल रहती हैं तो जब तक कयामत की रात न आवेगी तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है।
4. शैतान मनुष्यों को बहका कर काफ़िर बनाता है। ऐसा इस्लामिक मान्यता है। खुदा अगर सर्वज्ञ है तो फिर उसने फरिश्ते को आदम के समक्ष सजदा करने का हुकुम क्यों दिया। क्या वह नहीं जानता था की फरिश्ता सजदा नहीं करेगा और अवमानना करेगा। देखें-
क़ुरान-जब हमने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत् करो, देखा सभों ने दण्डवत् किया परन्तु शैतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था।। -मं० १। सि० १। सू० २। आ० ३४।।
(समीक्षक) इस से खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान की पूरी बातें नहीं जानता। जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया ? और खुदा में कुछ तेज भी नहीं है क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उस का कुछ भी न कर सका। और देखिये! एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहाँ क्रोड़ों काफिर हैं वहाँ मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या चल सकती है? कभी-कभी खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है। खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से। क्योंकि विना खुदा के शैतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता।
5. पाप क्षमा करना पाप को बढ़ाने के समान है। क़ुरान पाप का दंड देने के स्थान पर पाप क्षमा होने की बात करती हैं। देखें-
और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई करने वालों के।। -मं० १। सि० १। सू० २। आ० ५२।।
(समीक्षक) भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता। इसलिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो जाता है किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है।
6. इस्लाम मूर्तिपूजा का विरोध करता है परन्तु क्या काबा को बड़ी मूर्ति क्यों नहीं मानते। देखें-
निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुझे उस किबले को फेरेंगे कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की ओर फेर, जहाँ कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर लो।।-मं० १। सि० २। सू० २। आ० १४४।।
(समीक्षक) क्या यह छोटी बुत्परस्ती है? नहीं बड़ी।
7. क़ुरान में पशुहत्या वर्जित नहीं है। क्या यह हिंसा नहीं है। देखें-
तुम पर मुर्दार, लोहू और गोश्त सूअर का हराम है और अल्लाह के विना जिस पर कुछ पुकारा जावे।। -मं० १। सि० २। सू० २। आ० १७३।।
(समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बराबर हैं। हां! इन में कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं। और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख देके प्राणहत्या करनी? इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है। हां! ईश्वर ने विना पूर्वजन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया? क्या उन पर दयालु नहीं है? उन को पुत्रवत् नहीं मानता? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या करा कर खुदा जगत् का हानिकारक है । हिंसारूप पाप से कलंकित भी हो जाता है। ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं।
8. मुसलमान-गैर मुसलमान के चक्कर में क्या इस्लाम ने पूरी दुनिया में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है? देखें-
अल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं।। मार डालो तुम उन को जहाँ पाओ, कतल से कुफ्र बुरा है।। यहां तक उन से लड़ो कि कुफ्र न रहे और होवे दीन अल्लाह का।। उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो।। -मं० १। सि० २। सू० २। आ० १९०। १९१। १९२। १९३।।
(समीक्षक) जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है; न करते। और विना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उस को कुफ्र कहते हैं अर्थात् कुफ्र से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं। अर्थात् जो हमारे दीन को न मानेगा उस को हम कतल करेंगे सो करते ही आये। मजहब पर लड़ते-लड़ते आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये। और उन का मन अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है। क्या चोरी का बदला चोरी है? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि चोरी करें क्या हम भी चोरी करें? यह सर्वथा अन्याय की बात है। क्या कोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्या हम भी उस को गाली देवें? यह बात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है। यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है।
इस लेख में हमने केवल 8 शंकाएं प्रस्तुत की है। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास में 160 शंकाओं के माध्यम से इस्लाम मत के सिद्धांतों की समीक्षा की हैं। सभी इच्छुक पाठकों को सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हम अपने मुस्लिम भाइयों से जिन्होंने मस्जिद में आने का, नमाज़ देखने का और इस्लाम को समझने का आग्रह किया हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।
संस्कृत साहित्य, फिल्मी गीतों और लोक गीतों में होली के रंग
संस्कृत साहित्य में होली का प्रत्यक्ष उल्लेख कम मिलता है, लेकिन बसंत ऋतु, फाल्गुन मास, और राधा-कृष्ण की रासलीला से जुड़े श्लोकों में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। होली के मूल तत्व – रंग, उमंग, और प्रेम – को दर्शाने वाले कुछ संस्कृत श्लोक नीचे दिए गए हैं:
- फाल्गुन मास और वसंत ऋतु का वर्णन

“मुकुलानि पुष्पाणां जातानि च पादपे पादपे।
कुसुमैः सुसुगन्धिभिः पूरिता वसुधा किल॥”
अर्थ: प्रत्येक वृक्ष पर फूलों की कलियाँ खिल रही हैं, सुगंधित पुष्पों से पूरी पृथ्वी भर गई है।
- राधा-कृष्ण की होली (रासलीला का वर्णन)

“रङ्गबिन्दुं राधया, श्रीकृष्णस्य च लीलया।
फाल्गुने हर्षयुक्ताः, खेलन्ति सखिभिः सह॥”
अर्थ: फाल्गुन मास में राधा और श्रीकृष्ण प्रेमपूर्वक सखाओं के साथ रंगों की होली खेल रहे हैं।
- होली में हंसी-मजाक और मस्ती

“रक्तपीतसितैः वर्णैः, प्रक्षिपन्ति परस्परम्।
हसन्ति गायन्ति चापि, होलिकायां जनाः सुखम्॥”
अर्थ: लोग लाल, पीले, और सफेद रंगों को एक-दूसरे पर डालते हैं, हँसते हैं, गाते हैं, और होली में आनंद लेते हैं।
- भक्तिमय होली

“स्नेहं कुरु जनानां, रागं कुरु केशवे।
होली क्रीडा यस्यां, भक्तिरेकं मनोरथः॥”
अर्थ: लोगों से स्नेह करो, केशव (श्रीकृष्ण) में अनुराग रखो, होली केवल रंगों की नहीं बल्कि भक्ति की भी क्रीड़ा है।
- प्रेम और रंगों की महिमा

“रागरञ्जितवर्णानि, यत्र हर्षप्रसङ्गिताः।
होलिकायां जनाः सर्वे, सम्मिलन्ति परस्परम्॥”
अर्थ: रंगों से रँगे हुए लोग होली के अवसर पर हर्ष और प्रेम के साथ एक-दूसरे से मिलते हैं।
0हिंदी फिल्मों में होली के गाने बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि वे रंग, मस्ती और उमंग से भरे होते हैं। होली के इन गीतों ने न केवल फिल्मों को यादगार बनाया है, बल्कि हर साल होली के मौके पर इन्हें सुनना और इन पर नाचना भी एक परंपरा बन गया है।
कुछ प्रसिद्ध होली गीत:
“होली के दिन दिल खिल जाते हैं” – शोले (1975)
गायक: लता मंगेशकर, किशोर कुमार
यह गाना होली के जोश और प्यार को दिखाता है।
“रंग बरसे भीगे चुनरवाली” – सिलसिला (1981)
गायक: अमिताभ बच्चन
यह गाना आज भी हर होली पार्टी का सबसे बड़ा आकर्षण होता है।
“आज ना छोड़ेंगे बस हमजोली” – कटी पतंग (1970)
गायक: किशोर कुमार, लता मंगेशकर
इसमें रोमांस और मस्ती का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है।
“अरे जा रे हट नटखट” – नवरंग (1959)
गायक: आशा भोसले, महेंद्र कपूर
यह गाना पुराने जमाने की होली के रंग को दर्शाता है।
“होली आई रे कन्हाई” – मदर इंडिया (1957)
गायक: शमशाद बेगम
इस गाने में ग्रामीण भारत की होली की झलक देखने को मिलती है।
“बलम पिचकारी” – ये जवानी है दीवानी (2013)
गायक: विशाल ददलानी, शाल्मली खोलगड़े
यह मॉडर्न होली सॉन्ग में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक है।
“डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली” – वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम (2005)
गायक: अनुराधा श्रीराम, सुनिधि चौहान
यह गाना एक मस्ती भरा डांस नंबर है।
“होली में उड़ गए रंग” – बागी 2 (2018)
गायक: मीका सिंह, नेहा कक्कड़
यह हाल के वर्षों का एक हिट होली गीत है।
विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख होली लोकगीत
- ब्रज की होली (मथुरा-वृंदावन)
ब्रज की होली राधा-कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी होती है और यहां “लठमार होली” भी प्रसिद्ध है। यहां के लोकगीत रसिया और फाग गीत कहलाते हैं।
प्रसिद्ध गीत:


- अवध और भोजपुरी क्षेत्र की होली
यहां की होली में मस्ती और हंसी-ठिठोली होती है। भोजपुरी लोकगीतों में रंग, भांग, प्रेम और हंसी-मजाक का भरपूर मिश्रण होता है।
प्रसिद्ध गीत:



- उत्तर प्रदेश और बिहार की होरी
यहां के गीतों में कृष्ण, राम और शिव की होली का वर्णन होता है, साथ ही हंसी-मजाक भी खूब रहता है।
प्रसिद्ध गीत:


- राजस्थान की होली
राजस्थान में होली के गीतों में राजस्थानी संस्कृति, मीरा के भजन और मीराबाई की कृष्ण भक्ति की झलक मिलती है।
प्रसिद्ध गीत:


- मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र की होली
यहां के होली गीतों में आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है।
प्रसिद्ध गीत:

- हरियाणा और पंजाब की होली
यहां के होली गीतों में तेज धुन और भांगड़ा की झलक होती है।
प्रसिद्ध गीत:


- बंगाल की होली (दोल पूर्णिमा)
बंगाल में होली को “दोल जात्रा” कहा जाता है और यहां रवींद्र संगीत में होली के गीत लोकप्रिय हैं।
प्रसिद्ध गीत: