भारत की प्राचीन गौरव-गाथा को सम्पूर्ण विश्व मानता है। किन्तु दुःख की बात तो यह है कि हम भारतीय ही अपनी प्राचीन सभ्यता, जीवन और परिपाटी को भूल चुके हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व पंजाब का आविष्कार और संस्थापन करने वाले आर्यों की उन असाधारण विजयों के संस्कार क्या हमें याद हैं? मैं उन्हीं आर्यों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भारत की शश्य-श्यामला भूमि में प्रबल राज्यों की स्थापना की थी। उन्हीं आर्यों ने भारत के प्रशान्त वातावरण में अगम्य-अगाध अध्यात्मतत्व को खोज निकाला था जो कि अत्यन्त प्राचीन होते हुए भी आज तक ताजे और बहुमूल्य बने हुए हैं।
क्या हम जानते हैं कि कुरुओं और पांचालों की प्राचीन राजधानियाँ कहाँ थीं? क्या हमें पता है कि मगध के राजसिंहासन पर बैठ कर कब-कब किन-किन हिन्दू सम्राटों ने शासन किया था? हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे किन पूर्वजों ने विशाल महासागरों को अतिक्रान्त करके चीन, अरब, यवद्वीप और पाताल में अपने उपनिवेश कायम किए थे। क्या हमें आन्ध्र, गुप्त, नाग आदि महाराज्यों के विषय में जानकारी है? शकों ने किस प्रकार से भारत को आक्रान्त किया था और विक्रम ने उन्हें कैसे पददलित किया था? एलोरा और अजन्ता की गुफाएँ, साँची के स्तूप, भुवनेश्वर और जगन्नाथ के मन्दिरों का निर्माण किस-किस ने किया था?
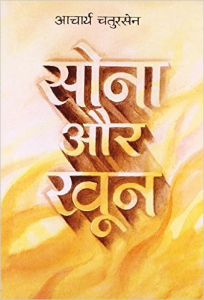 इस उद्देश्य से कि हम भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, गौरव को भूल जाएँ, एक सुनियोजित शिक्षा-नीति के तहत भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देने का आरम्भ सन् 1835 में आरम्भ किया गया, जो कि कमोबेश आज तक चली आ रही है। इस शिक्षा-नीति का निर्माण लॉर्ड मैकॉले ने किया था जिसने सन् 1833 में चार्टर पर पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था, “मैं चाहता हूँ कि भारत में यूरोप के समस्त रीति-रिवाजों को जारी किया जाए, जिससे हम अपनी कला और आचारशास्त्र, साहित्य और कानून का अमर साम्राज्य भारत में कायम करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भारतवासियों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करें जो हमारे और उन करोड़ों के बीच में, जिन पर हमें शासन करना है, दुभाषिए का काम दें; जिनके खून तो हिन्दुस्तानी हों, पर रुचि अंग्रेजी हो। संक्षेप में अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय तन से भारतीय, पर मन से अंग्रेज हो जाएँ, जिससे अंग्रेजों का विरोध करने की उनकी भावना ही नष्ट हो जाए।”
इस उद्देश्य से कि हम भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, गौरव को भूल जाएँ, एक सुनियोजित शिक्षा-नीति के तहत भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देने का आरम्भ सन् 1835 में आरम्भ किया गया, जो कि कमोबेश आज तक चली आ रही है। इस शिक्षा-नीति का निर्माण लॉर्ड मैकॉले ने किया था जिसने सन् 1833 में चार्टर पर पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था, “मैं चाहता हूँ कि भारत में यूरोप के समस्त रीति-रिवाजों को जारी किया जाए, जिससे हम अपनी कला और आचारशास्त्र, साहित्य और कानून का अमर साम्राज्य भारत में कायम करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम भारतवासियों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करें जो हमारे और उन करोड़ों के बीच में, जिन पर हमें शासन करना है, दुभाषिए का काम दें; जिनके खून तो हिन्दुस्तानी हों, पर रुचि अंग्रेजी हो। संक्षेप में अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय तन से भारतीय, पर मन से अंग्रेज हो जाएँ, जिससे अंग्रेजों का विरोध करने की उनकी भावना ही नष्ट हो जाए।”
परन्तु, जिन दिनों मैकॉले ने अपने उपरोक्त विचार व्यक्त किए थे, उसी काल में अनेक पाश्चात्य विद्वानों की नजर भारतीय सांस्कृतिक सम्पदा पर भी पड़ रही थी। उन दिनों के पहले तक यूरोप भारत को धन-धान्य से भरा-पूरा, नवाबों और मुग़लों का देश समझता था और उसकी दृष्टि लूट-खसोट पर थी, सभ्यता और संस्कृति के उद्गम के सम्बन्ध में यूरोप का विश्वास था कि उसका आरम्भ यूनान और फिलिस्तीन से हुआ है; वे यह भी समझते थे कि वही देश संसार में सबसे प्राचीन सभ्यता वाले हैं। भारत को तब तक यूरोप के लोग एक अर्द्धसभ्य देश समझते थे। परन्तु जब यूरोप के निवासियों ने संस्कृत सीखी तो उनका परिचय उपनिषद् तथा कुछ जैन और बौद्ध ग्रन्थों से हुआ।
जिन दिनों प्लासी का युद्ध हो रहा था, उन्हीं दिनों दुपरोन नामक एक फ्रेंच नवयुवक भारत में प्राचीन पाण्डुलिपयाँ यत्नपूर्वक खोजता फिर रहा था। वह भारत से लगभग अस्सी पाण्डुलिपयाँ अपने साथ फ्रांस ले गया। इन पाण्डुलिपियों में एक पाण्डुलिपि दाराशिकोह द्वारा फारसी-अनूदित उपनिषदों की भी थी। दुपरोन ने लैटिन में इसका अनुवाद करके ‘औपलिखत’ नाम से प्रकाशित किया, जिसे पढ़कर जर्मन का प्रसिद्ध दार्शनिक शॉपेनहार आश्चर्यविमूढ़ हो गया और उसके मुँह से ये उद्गार निकले कि ‘इसने मेरी आत्मा की गहराई को हिलकोर दिया है। इसके प्रत्येक शब्द से मौलिक विचार ऊपर उठते हैं जिससे भारतीय विचारधारा का वातावरण आप ही उठ खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानों ये विचार हमारे अपने आत्मिक बन्धु के विचार हों। हमारे मनों पर जो यहूदी-संस्कारों की रूढ़ियाँ और अंधविश्वास छाए हुए हैं, वे इन विचारों के स्पर्श-मात्र से एकबारगी ही गायब हो जाते हैं। सारे संसार में इसके जोड़ का कोई और ग्रन्थ नहीं हो सकता। जीवन-भरफ में मुझे यही एक आश्वासन प्राप्त हुआ है और मृत्युपर्यन्त यह मेरे साथ रहेगा।’
जर्मनी में उपनिषदों के अध्ययन से विचारों का जागरण उसी प्रकार से हुआ जैसे रिनासां के समय में प्राचीन यूनानी साहित्य के सम्पर्क से सारे यूरोप में हुआ था। इसके बाद जोहान फिक्टे और पॉल दूसान ने वेदान्त के सत्य को संसार का सबसे बड़ा सत्य माना, और नीत्शे ने मनुस्मृति को पढ़ा तो उसने उसे बाइबिल से कई गुना श्रेष्ठ कहा।
न्याय के क्षेत्र में हिन्दुओं पर शासन उन्हीं के धर्मशास्त्रो के अनुसार करने के विचार से वारेन हेस्टिंग्ज ने पहले-पहल धर्मशास्त्रों का अनुवाद फारसी और अंग्रेजी भाषा में कराया। इसके अतिरिक्त विलायत से आए हुए जजों और वकीलों को उसने संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यद्यपि कचहरी की आवश्यकता के लिए संस्कृत पढ़ी, पर जब उन्होंने वहाँ का भाव-गाम्भीर्य और विचारों का मार्दव देखा तो वे एकबारगी अभिभूत हो उठे। इसके बाद सन् 1784 में सर विलियम जोन्स ने, जो उन दिनों कलकत्ता के प्रधान न्यायाधीश थे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तथा स्वयं कालिदास की ‘शकुन्तला’ का अनुवाद किया और ‘ऋतुसंहार’ का एक सम्पादित संस्करण प्रकाशित कराया।
इसके एक बरस बाद सर चार्ल्स विलिकिन्स ने ‘भगवद्गीता’ का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। सर जोन्स संस्कृत पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सन् 1784 में मानव-धर्मशास्त्र नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया और जब सन् 1786 में एशियाटिक सोसाइटी का अधिवेशन हुआ तो यह घोषणा कर दी कि संस्कृत परम अद्भुत भाषा है, और लैटिन और ग्रीक से अधिक सम्पन्न है। उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि गोथिक और केल्टिक भाषा-परिवार का उद्गम संस्कृत ही है। आगे इसी बुनियाद पर फ्रांजवाय, मैक्समूलर और ग्रिम ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का महल खड़ा किया। इसके तत्काल बाद यूरोप के पण्डितों ने निरुक्त और व्याकरण का मनन किया और फोनेटिक्स लिखना आरम्भ किया।
विलियम जोन्स की मृत्यु के बाद उनके कनिष्ठ सहकारी हेनरी टॉमस कोलब्रुक एक महान प्राच्यविद्या-विशारद प्रसिद्ध हुए। इन्होंने हिन्दू-धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष और धर्म का बड़ा ही गम्भीर अध्ययन एशियाटिक रिसर्चेज में प्रकाशित किया। वेदों का भी एक प्रामाणिक विवरण ‘आन द वेदाज’ सबसे प्रथम उन्होंने निकाला।
मैक्समूलर, जो कि एक जर्मन होने के बावजूद अंग्रेजी शासन का एक स्तम्भ था, ने सायण के भाष्य पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया और उसके बाद उसने वेदों का भाष्य किया, जिसने पूरे यूरोप की आँखें खोल दीं। वेदभाष्य से बढ़कर एक काम उसने यह किया कि तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन की परम्परा स्थापित की। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के मोह-अन्धकार का पर्दा फट गया। अब तक वे जो यह मानते आ रहे थे कि फिलिस्तीन और यूनान सबसे पुराने देश हैं, और हिब्रू भाषा सबसे पुरानी है, ये सब मान्ताएँ बिखर गईं। मैक्समूलर ने प्रमाणित कर दिया कि संसार की प्राचीनतम जाति आर्य है और प्राचीनतम साहित्य वेद है। इस प्रकार जर्मन विद्वानों ने भारतीय साहित्य, दर्शन और धर्म का जो बखान किया, उसने ईसाइयों के उस प्रचार को भी मिथ्या कर दिया जो वे भारत से बाहर करते थे कि भारत अर्द्ध-शिक्षित देश है।
श्लीगल बन्धुओं ने जर्मन भाषा के द्वारा यूरोप में भारतीय ज्ञान का काफी विस्तार किया। वेद, उपनिषद, भगवद्गीता, मनुस्मृति, शकुन्तला और वेणीसंहार को देखकर जर्मन कवि और विद्वान विस्मय से मूढ़-मुग्ध हो गए। इस साहित्य के भाव और विचार नये क्षितिज के थे। श्लीगल ने गीता की प्रशंसा पागलों की भाँति की और कहा, “ओ ईश्वरत्व के व्याख्याता, तुम्हारी वाणी के प्रभाव से मनुष्य का हृदय ऐसे अकथनीय आनन्द की भूमि में पहुँच जाता है, जो अत्यन्त उच्च, सनातन और ईश्वरीय है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे चरणों में अपना अभिनन्दन भेंट करता हूँ।” भारतीय काव्यों की विलक्षणता पर सकर्ट ने प्रकाश डाला। गेटे ने शकुन्तला पर प्रशस्ति लिखी। गेटे आदि ने संस्कृत-परम्पराओं को अपनाया और श्लीगल से हाइने तक जर्मन कविता में भारतीय भाव फैलत ही रहे।
यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि हम समस्त संसार द्वारा स्तुत्य अपनी ही संस्कृति, सभ्यता, और गौरव को निरन्तर रूप से भुलाते ही चले जा रहे हैं।
टीपः इस पोस्ट में विचार, भाव तथा सामग्री आचार्य चतुरसेन के उपन्यास “सोना और खून” से लिए गए हैं।
***
साभार- http://agoodplace4all.com/ से



बिलकुल सही हमारे pyare bharat ka naam hi badal dala inn British logo neBHARAT ko INDIA kar diya …..
….. bharat ek mahan desh hai …aur hame garv hona chahiye ki hum hindustani hai ………hame hamari bhasha Sanskrit or hindi per garv hona chahiye……jai Bharat