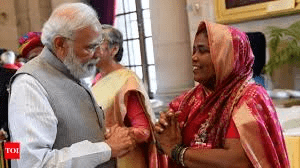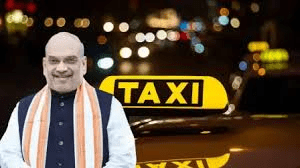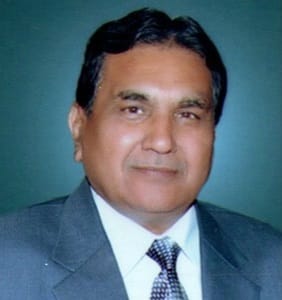त्रेता युग से ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भारत की आत्मा तथा भारतीय अस्मिता के जीवंत प्रमाण हैं। श्रीरामचन्द्र भारतवर्ष के एकमात्र तपस्वी राजा हैं। वे करुणा के सागर हैं। वे श्याम सुंदर छवि वाले हैं। श्रीराम का शरीर जितना ही मोहक और भव्य है, उतना ही उनका शील उदात्त गुणों से विभूषित है। उनकी कांति मनमोहक है। उनके कंधे सिंह के जैसे बलिष्ठ एवं ताकतवर हैं। वे धीर, वीर और गंभीर हैं। वे महान बलशाली योद्धा हैं। उनकी आंखें कजरारी और बड़ी-बड़ी हैं। उनकी चाल हाथी के जैसी मतवाली है। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक हैं। वे एक पत्नीव्रतधारी हैं। वे सत्य, न्याय और धर्म के रक्षक हैं। वे नवधा भक्ति के जन्मदाता हैं। वे सगुण-निर्गुण समन्वय के साकार स्वरुप हैं।
वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय, लोक रक्षक, आज्ञाकारी, दृढ़ निश्चयी, जनमत का सम्मान करने वाले और कठोरव्रती हैं। वे भारतीय वन संस्कृति के पालक हैं। श्रीराम सगुण-निर्गुण साकार हैं। वे धर्मपरायण, न्यायपरायण, लोक रक्षक, आज्ञाकारी, दृढ़ निश्चयी, कठोरव्रती श्रीराम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 16 अलौकिक गुणों से सम्पन्न हैं। वे चरित्रवान हैं। वे मानवीय मूल्यों के पारावार हैं। वे पतितपावन हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के इन सभी विलक्षण गुणों की पुष्टि हमारे सभी महाकवियों ने की है।
महाकवियों द्वारा श्रीराम के गुणों का चित्रण
आदिकवि वाल्मीकि जो ब्रह्माजी के दसवें पुत्र प्रचेता के पुत्र हैं, वे सम्पूर्ण विश्व में पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय समन्वय के यथार्थ आदर्श हैं। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भारतवर्ष के भावपुरुष हैं। कालिदास ने अपनी अमर रचना ‘रघुवंश’ के 10वें सर्ग से लेकर 15वें सर्ग तक में श्रीराम को तेजस्वी और पराक्रमी राजा बताया है। उन्होंने श्रीराम को धर्मपरायण और न्यायप्रिय बताया है। उन्हें लोकरक्षक, आज्ञापालक, दृढ़निश्चयी और कठोरव्रती बताया है।
महाकवि भवभूति तथा जैन महाकवि स्वयंभू आदि ने भी स्पष्ट रूप से अपनी-अपनी अमर रचनाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के मानवीय गुणों की कुल 16 विलक्षण प्रतिभाओं का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं-
“तुम ही जग हौं, जग तुमही में।
तुमहि विरचि मरजाद दुनी में।।”
स्वयंभू ने अपने जैन रामायण में श्रीराम को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित करते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति की अस्मिता का प्रतीक बताया है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ लिखते हैं-
“रघुनंदन हैं धीर दुरंधर, धर्मप्राण भव-हित रत हैं।”
केशवदास ने अपनी रचना ‘रामचंद्रिका’ में श्रीराम को सत्यस्वरूप, गुणातीत और मायातीत बताया है।
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं-
“हो गया निर्गुण-सगुण साकार है,
ले लिया अखिलेश ने अवतार है।”
ठीक इसी प्रकार की बात गुप्तजी स्वयं राम से कहलवाते हैं-
“संदेश नहीं स्वर्ग का लाया,
भूतल को स्वर्ग बनाने आया।”
हिन्दी के अमर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं-
“रोम-रोम रम रहे कैसे तुम राम हो।”
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी अमर रचना ‘राम की शक्ति पूजा’ में श्रीराम को अपराजेय योद्धा बतलाते हैं।
सूफी संत कवि कबीरदास कहते हैं-
“कबीर वन-वन में फिरा, कारनि अपने राम।
राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम।।”
स्वर्गीय राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के राम स्वयं कहते हैं-
“संदेश नहीं मैं स्वर्ग का लाया,
भूतल को स्वर्ग बनाने आया।”
गुप्तजी के राम ब्रह्म अवतारी होते हुए भी आधुनिक युग के अनुरूप आदर्श पुरुष हैं।
20वीं सदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं-
“जीवन जगत् के, विकास विश्व वेद के हो,
परम प्रकाश हो, स्वयं ही पूर्णकाम हो…
रोम-रोम में रम रहे कैसे तुम राम हो।”
गीता में श्रीकृष्ण और रामायण में श्रीराम का समर्पण
सच तो यह है कि जिस प्रकार महाभारत में जो सम्मान शांतिदूत श्रीकृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को दिया था, वहीं संदेश श्रीराम ने शबरी को नवधा भक्ति प्रदान कर दिया है। सापेक्ष रूप में, श्रीराम का मर्यादित चरित्र भारत की आत्मा तथा भारतीय अस्मिता का जीवंत प्रमाण है।