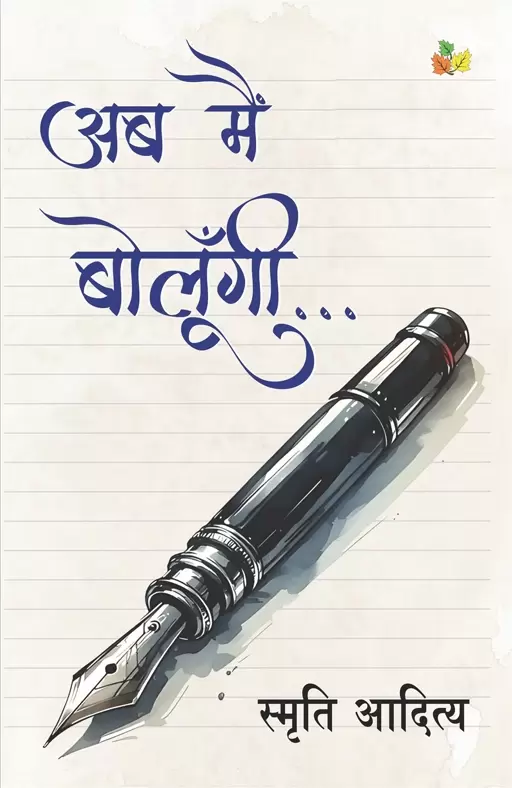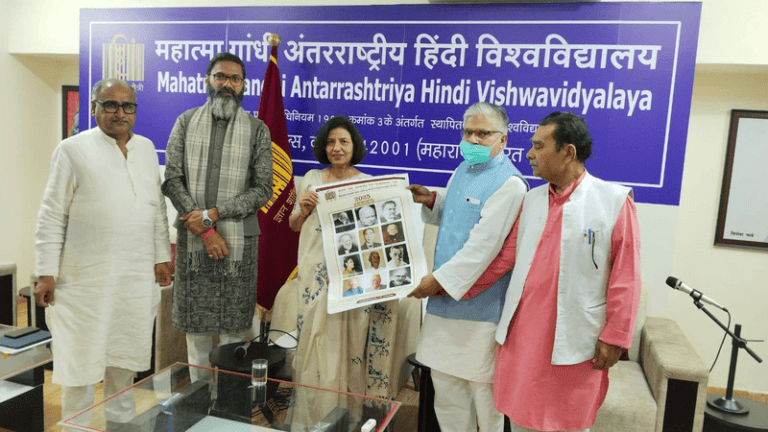(जन्म १८९२- निधन १९७७)
हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में, जयपुर घराना, राग को अत्यधिक जटिल और कठिन पद्धति द्वारा विस्तृत करते हुए, अपने स्वर और लय के संतुलित समाकलन के लिए जाना जाता है। यह वही चुनौतीपूर्ण जटिलता है जिसमें गायन की जयपुर शैली के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक, केसरबाई केरकर, ने अच्छी तरह निपुणता हासिल की और निर्विवाद प्रमाण की छाप सहित अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत की। १९०० के दशक के पूर्व में वह देवदासी परंपरा से अलग हो गईं और अपने समय की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रख्यात कलाकार बन गईं।
केरी (गोवा) में जन्मी, केसरबाई का परिवार जब कोल्हापुर में स्थानांतरित हुआ तब उन्होंने दस साल की उम्र में उस्ताद अब्दुल करीम खान के निचे संगीत प्रशिक्षण शुरू किया। यह सिर्फ़ कुछ महीनों तक ही जारी रहा जब तक उनका परिवार १९०१ में गोवा वापस आ गया, जहाँ उन्होंने पं. वाज़ेबुआ से सीखना शुरू कर दिया। जब १९०९ में उनका परिवार बॉम्बे स्थानांतरित हुआ, तो उन्होंने लगभग एक साल तक उस्ताद बरकतुल्लाह खान (बीन वादक) से सीखा। उन्होंने कुछ महीनों तक पं. भास्करबुआ बखले से भी सीखा। अब तक उनका प्रशिक्षण अनियमित था और १९२० से ही उनकी तालीम, अगले पंद्रह वर्षों के लिए, उस्ताद अल्लादिया खान के साथ शुरू हुई। हमें उपाख्यानों से पता चलता है कि १९१८ में बॉम्बे में एक दोस्त के यहाँ आयोजित संगीत सभा में उन्होंने अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से अल्लादिया खान के अलावा किसी और के साथ न शुरू करने का निर्णय लिया।
केसरबाई की अपनी साँस को दीर्घ अंतराल तक बनाए रखने की क्षमता, जो एक महिला के स्वर के लिए असामान्य मानी जाती थी, ने श्रोताओं और संगीतकारों को अक्सर प्रभावित किया है। उनका उन्मुक्त कंठ और भारी-भरकम स्वर अपनी दृढ़ता एवं स्पष्टता के द्वारा आपको छू लेता है। ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि के इस प्रक्षेपण को व्यवधान से बचाने के लिए उन्होंने जान-बूझकर संगीत कार्यक्रमों में माइक्रोफ़ोन के उपयोग से परहेज किया। जटिल और असामान्य या दुर्लभ (अप्रचलित) राग में निपुणता प्राप्त करना जयपुर घराने की एक विशिष्ट विशेषता है। केसरबाई के रंगपटल में खोखर, कान्हड़ा, बधंस-सारंग, हिंडोल-बहार, जौन-बहार जैसे विभिन्न प्रकार के राग सम्मिलित हैं। उन्हें १९३८ में ‘सुरश्री’ की उपाधि, १९५३ में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पत्र और १९५९ में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। जब १९६५ के आसपास उन्हें एहसास हुआ कि उनका स्वास्थ्य उनकी अटूट संगीतकारिता में बाधा उत्पन्न करेगा तब उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन बंद करने की घोषणा की।
उनका प्रभावशाली स्वर श्रोताओं को निरंतर प्रभावित करता है और यह केवल पृथ्वी पर ही नहीं गूँजता है। नासा के अंतरिक्ष-खोज यान वायजर १ के लिए साउंड्स ऑफ़ अर्थ नामक एक एल्बम संगृहित किया गया था और बीथोवेन, मोज़ार्ट और बाख के बीच बाह्य अंतरिक्ष में केसरबाई का राग भैरवी में ‘जात कहाँ हो’ का प्रस्तुतिकरण अनंतकाल के लिए गुंजायमान है।