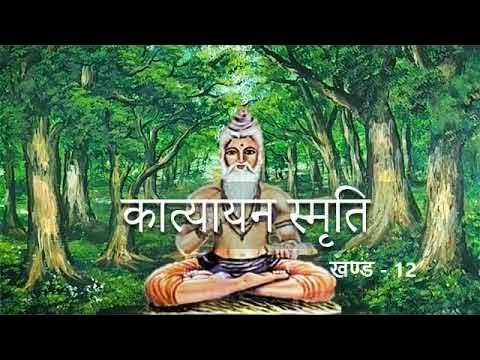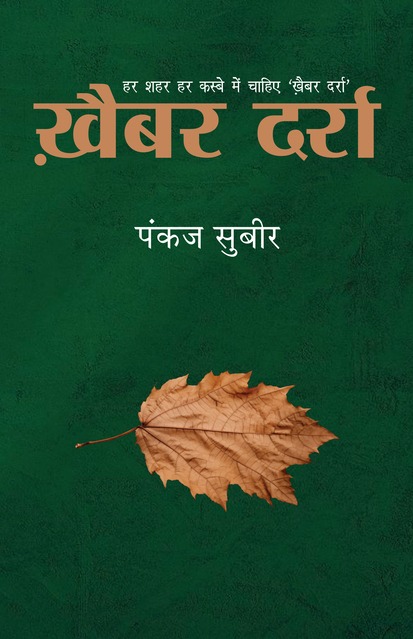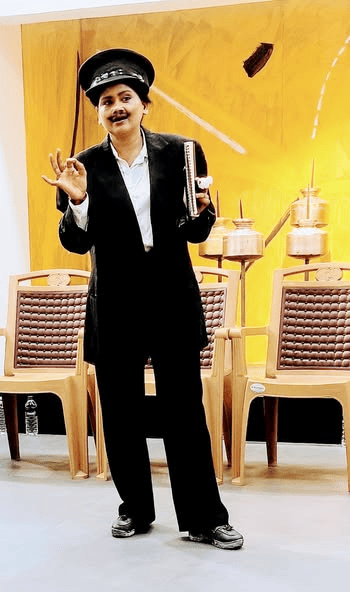सामान्यतः ऐसा माना जाता है (और जो शालेय / महाविद्यालयीन शिक्षा से और दृढ होता गया है) कि, न्याय प्रणाली, न्यायालय, न्यायमूर्ती, वकील…. यह सब व्यवस्थाएं अंग्रेजो ने भारत मे लायी। अंग्रेज आने से पहले भारत मे यह कुछ भी नही था। यदि जनता की कोई शिकायते होती थी, तो वह सीधे राजा के सामने रखी जाती थी। राजा उसके मनमर्जी से, या उस समय उसकी जो मनस्थिती रही होगी, उस प्रकार निर्णय देता था।
परंतु वास्तविक चित्र क्या है?
हजारो वर्षों से अपने देश मे सुव्यवस्थीत न्यायप्रणाली कार्यरत थी। इस न्यायप्रणाली का आधार था – धर्मशास्त्रों का,अलग-अलग स्मृतियों का। इस न्यायव्यवस्था को समाज मान्यता थी। इस व्यवस्था के कारण उस समय के अखंड और विशाल भारत देश में स्वस्थ, सुदृढ और सशक्त समाज व्यवस्था का अस्तित्व था। महेश कुमार शरण ने उनके पुस्तक ‘कोर्ट प्रोसिजर इन एन्शंट इंडिया’ मे लिखा है –
‘It is just possible that elements of Hindu law were adopted by Romans thourgh Greek and Egyptian channels’
अर्थात, विश्व मे परिपूर्ण न्यायव्यवस्था सर्वप्रथम भारत मे ही विकसित हुई है। यह न्याय व्यवस्था ग्रीक और मिस्त्र देश के माध्यम से रोमन्स (युरोपियन्स) ने अपनायी होगी।
महेश कुमार शरणने आगे लिखा है –
‘It should be a pride and satisfaction to a Hindu to know that his / her ancestors had scaled great heights not only in literature, philosophy and religion, but had advanced very farin the domain of law’ – (Court procedures in Ancient India)
(अर्थात, एक हिंदू के लिए इसकी जानकारी होना अत्यंत गर्व और समाधान की बात है कि उसके पुरखों ने केवल साहित्य, दर्शन और धर्म मे ही अपनी कीर्ती ध्वजा फहराई थी, ऐसा नही है। तो न्याय के क्षेत्र में भी उन्होने कीर्तीमान रचा था।)
आगे लिखा है-
‘The rule and evidence were as complete and perfect, as we can find them today. The administration of justice was regular and the system was well defined, as no aspect was left arbitrarily, capricious or uncertain. Judiciary had the highest regard and supreme position.
(अर्थात, ‘नियम’ और ‘प्रमाण’ इन की परिभाषा इतनी परिपूर्ण और निर्दोष थी, जितनी आज है। न्याय प्रणाली एक नियमित व्यवस्था थी। परिभाषा सुस्पष्ट थी। इसमे कोई भी अनियंत्रितता नही थी, अनिश्चितता नही थी। न्यायव्यवस्था सर्वोच्च स्थान पर थी और उस व्यवस्था को सर्वाधिक आदर और सम्मान मिलता था।)
इसी पुस्तक में महेश कुमार शरण ने आगे लिखा है –
Besides this, the whole procedure is completely indigenous and nothing has been imported into it from any other system, whatsoever.’
(अर्थात, इस न्याय व्यवस्था की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः स्वदेशी थी। इसमें कोई भी बाहरी (देशों से) बिंदु या व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था।)
————– ————-
भारत की यह संपूर्ण न्याय व्यवस्था, स्मृतियों के आधार पर खड़ी थी। कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति आदि प्रमुख स्मृतियां थी।
यह स्मृति क्या होती है? यह कितनी पुरानी है?
एक सुव्यवस्थित समाज रचना निर्माण करने के लिए, हजारों वर्षों से अपने पूर्वजों ने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया हैं। इन ग्रंथो के अनुसार ही अपने समाज में प्रथा, परंपरा, व्यवस्थाएं निर्माण हुई। इन ग्रंथों के आधार पर अपना समाज चल रहा था। इसलिए, इतने सारे आक्रमणों के बाद भी हमारी पहचान कायम रही, बनी रही।
इन ग्रंथो में वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने, समाज महर्षियों ने, जिस ज्ञान का संचय किया है, वह संचय यानी स्मृतियां। एक प्रकार से परंपराओं का संकलन होने के कारण इन्हें ‘स्मृति’ यह नाम दिया गया है। यह स्मृति मानो हमारा धर्मशास्त्र है। भारत का और पौर्वात्य प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने वाले जो पाश्चात्य विद्वान है, उनके अनुसार इन स्मृतियों की रचना ईसा पूर्व 500 वर्षों से लेकर तो ईसा के बाद पांचवें सदी तक हुई है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में जिस काल खंड में आर्य चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहे थे, उसी कालखंड में स्मृतियों की रचना हुई है, ऐसा पश्चिम के विद्वानों का मत है। परंतु उपलब्ध संदर्भों के अनुसार स्मृतियों का कालखंड इससे भी बहुत प्राचीन है।
इन स्मृतियों में से ‘कात्यायन स्मृति’ यह ऋषि कात्यायन द्वारा लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। कात्यायन यह याज्ञवल्क्य ऋषि के पुत्र थे। इनका कार्यकाल ईसा पूर्व कुछ हजार वर्ष माना जाता है। अर्थात ‘कात्यायन स्मृति’ यह ग्रंथ, कात्यायन ऋषि ने लिखे हुए सूत्र और उनके अन्य शिष्यों के साहित्य का संकलन है। इसलिए कात्यायन स्मृति में केवल ऋषि कात्यायन के श्लोक नहीं है। देवल पितामह, प्रजापति, वशिष्ठ, मनु आदि ॠषियोंका सहभाग भी इस कात्यायन स्मृति में है।
इस स्मृति में कात्यायन ऋषि ने उनके पहले, इस न्याय के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया था, उनका उल्लेख किया है। भृगु, बृहस्पति, गार्गीय, तम, कौशिक, लिखिता, मनु, मानव आदि..! प्राचीन भारत में जो न्याय प्रणाली विकसित हो रही थी, उसमें कात्यायन ऋषि के बाद, लगभग 1000 वर्ष तक, इसमें विशिष्ट सुधार होते रहे। कात्यायन स्मृति में उसका प्रभाव दिखता है। इस स्मृति में प्रत्यक्ष कात्यायन ऋषि ने लिखे हुए श्लोक अंत में दिए हुए हैं।
महामहोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे (1880 – 1972) ने प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र के क्षेत्र में, अत्यंत गहन शोध और भरपूर लेखन किया है। ‘भारतीय धर्मशास्त्र का इतिहास’ इस विषय पर उनका 6500 पृष्ठोंका का, पांच खंडो में लिखा हुआ साहित्य प्रकाशित हुआ है। स्वयं न्याय शास्त्र के विद्वान तो थे ही, साथ मे उन्होंने संस्कृत ग्रंथोका का गहन अध्ययन किया। वर्ष 1963 में महामहोपाध्याय काणे जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान, ‘भारत रत्न’ दिया गया।
ऐसे पां. वा. काणेजी ने, कात्यायन स्मृति के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। वे लिखते हैं – ‘कात्यायन स्मृति में न्याय प्रणाली के संदर्भ में जो विषय आएं है, वह अद्भुत और आश्चर्य जनक है। क्योंकि आज के आधुनिक न्याय शास्त्र जैसी पद्धति और नियम, कात्यायन स्मृति में हैं।’
[Some of his (sage Katyayan’s) rules, such as those about the contents and characteristics of good points and written statements, about the evidence of witness and about documents, about constructive res judicata are startling in their modernity].
कात्यायनी स्मृति में आए हुए विषय –
– न्यायालय, न्यायालय की प्रक्रिया / पद्धति
– कागजात
– परिक्षण (बहस)
– शपथ लेकर दी हुई साक्ष्य / बयान
– भागीदारी
– भेंट वस्तु (gift)
– अनुबंध तोड़ना
– जो मालिक नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति ने की हुई वस्तुओं की बिक्री
– परंपराओं का / नियमों का उल्लंघन
– विवादों की सीमा
– पैतृक संपत्ति का बंटवारा / विवाद
– वाकपारुष्य (आज की भाषा में ‘हेट स्पीच’)
– दंड पारुष्य (कठोर सजा)
– प्रकीर्णक (विविध / अनेक प्रकार के यम-नियम)
– प्रशांत पोळसंपूर्ण कात्यायन स्मृति में, न्यायालय की परिभाषा से लेकर, विविध प्रसंगों में किस प्रकार से न्यायदान करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की है।न्यायालय की परिभाषा-
धर्मशास्त्र विचारेण मूलसार विवेचनम्
यत्राधिक्रियते स्थाने, धर्माधिकरणम् हितत् ।।52।।
[The place, where the decision of the truth of the plaint, i.e. lit, the cause or root of the dispute, is carried on by a consideration of the (rules of the) sacred law is (called) the Hall of Justice]
धर्माधिकरण याने न्यायालय.
मजेदार बात यह है कि, कात्यायन स्मृति में फिर्यादी को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए इसका भी विस्तार से वर्णन किया है,।

प्रश्न प्रकार –
काले कार्यार्थिनं पृच्छेत प्रणतंपुरतःस्थितं ।
किं कार्य का च ते पीडा मा भैषीब्रूहि मानव ।।86।।
केन कस्मिकंदाकस्मातपृच्छे देवं सभागतः I
एवं पृष्ठः सयद्ब्रूयात्तत्सभ्यै ब्राह्मणैः सहः ।।87।।
विमृश्य कार्यं न्यायंचेदाव्हानार्थमतः परम्
मुद्रां वा निक्षेपेत्तस्मिन्पुरुषं वा समादिशेत ।।88।।
अर्थात, न्यायाधीश ने पक्षकार को (जो फरियाद लेकर आया है), न्यायालय के उचित समय पर, प्रश्न पूछना चाहिए। यह पूछते समय, पक्षकार ने न्यायाधीश के सामने आदब से खड़ा रहना है। न्यायाधीश पूछेंगे, “आपकी शिकायत क्या है? आपको कहीं चोट तो नही आई हैं? डरिए मत…” आदि।
इसके बाद न्यायाधीश ने पूछना है, “किसके कारण, कहां, कब, (दिन के किस समय) और क्यों ?आपको तकलीफ हुई, या आप क्यों शिकायत कर रहे हैं?” इन प्रश्नों पर पक्षकार जो कहता है, वह न्यायालय ने शांति से सुनना है। उस न्यायालय में उपस्थित मूल्यांकन कर्ताओं की (आज की भाषा में ‘जूरी सदस्य’) मदद से, उनकी सलाह पर, न्यायमूर्ति ने यह तय करना है कि यह शिकायत / यह प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने योग्य है या नहीं? अगर है, तो न्यायमूर्ति ने संबंधित गुनहगार को हाजिर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आज्ञा देनी है।
कितना अद्भुत है यह सब..! पां. वा. काणे के कहे अनुसार, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यह सब पढ़कर! कितने विस्तार से पूरी न्याय प्रणाली (न्याय की पद्धति / प्रक्रिया) समझायी है। सनद रहे, कम से कम दो – ढाई हजार वर्ष पूर्व, अपने देश में इतनी व्यवस्थित, और ठीक से दस्तावेजीकरण (Well documented) की हुई, न्याय व्यवस्था अस्तित्व में थी।
और हमें पढ़ाया गया कि भारत में न्याय व्यवस्था लायी, वह अंग्रेजों ने..!
एक हजार से अधिक श्लोक कात्यायन स्मृति में है। यह ग्रंथ विस्तृत धर्मशास्त्र का एक हिस्सा है। इस का अर्थ है, हमारे पूर्वजों ने एक सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली विकसित करके उसका उपयोग किया था।
इसीलिए समाज में किसी पर भी अन्याय नहीं होता था, और कानून व्यवस्था सही रूप में लागू की जा रही थी।
धर्मशास्त्र का (अर्थात न्याय शास्त्र का), विस्तृत विवेचन करने वाला कात्यायन स्मृति यह एकमात्र ग्रंथ नहीं था। साधारणत: ढाई हजार वर्ष पुराना, या उससे भी प्राचीन, ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ यह ग्रंथ भी, भारतीय न्याय पद्धति की विस्तृत विवेचना करता है। इस ग्रंथ में कुल 1003 श्लोक है, जो तीन खंडों में विभाजित है।
01. आचार कांड – इसमें तेरा अध्याय है। ब्रह्मचारी, विवाह, गृहस्थ, भक्ष्याभक्ष्य, द्रव्यशुद्धी, दान, श्राद्ध, राज धर्म इत्यादि विषयों पर इसमें विवेचन किया है।
02. व्यवहार कांड – 25 अध्याय के इस कांड में सीमावाद, स्वामीपालवाद, अस्वामी विक्रम, दत्तक प्रधानिक (गोद लेना), वेतन, दान, वाकपारूष्य आदि विषय और उनके यम-नियम का वर्णन है।
03.प्रायश्चित कांड – इसमें 6 अध्याय है। शौच प्रकरण, आपधर्म प्रकरण, वानप्रस्थ, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण जैसे विषय इसमें आते हैं।
अंग्रेजों का शासन भारत में जब तक अच्छी तरह स्थिर नहीं हुआ था, तब तक, मुख्य रूप से ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ के आधार पर न्यायदान के काम चलते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि मिथिला के थे। शुक्ल यजुर्वेद और ‘शतपथ ब्राह्मण’ उपनिषद के रचयिता थे।
याज्ञवल्क्य स्मृति मे, पंचायत समिति (ग्राम पंचायत) में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस विवेचन से लेकर, राज्य के मुख्य न्यायाधीशने, या राजा ने, किस प्रकार से न्याय देना चाहिए, इसकी विस्तार से चर्चा की है।
पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में ‘मनुस्मृति’ की बहुत चर्चा हुई है। ‘भारत की प्राचीन समाज व्यवस्था और न्याय व्यवस्था मनुस्मृति के ही आधार पर चलती थी’ ऐसा चित्र निर्माण किया गया हैं। यह गलत है।
भारत के न्याय व्यवस्था के संदर्भ में मनुस्मृति यह मुख्य संदर्भ ग्रंथ कभी नहीं था। अनेक संदर्भ ग्रंथो में से एक था, यह सच है। ‘दंड विधान’ मे, अर्थात सजा देने मे मनुस्मृति का कुछ अंशों मे उपयोग होता था, यह भी सच हैं। किंतु केवल इतना ही..! जो महत्व कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति को था, उतना महत्व मनुस्मृति को निश्चित रूप से नहीं था।
किंतु ‘इन दो – ढाई हजार वर्ष पुरानी स्मृतियों के आधारपर ही, भारत की न्याय व्यवस्था चलती थी’ यह विधान पूर्ण सत्य नहीं है। यह अर्ध सत्य है।
– प्रशांत पोळ
प्राचीन भारत के न्याय व्यवस्था की चर्चा करते हुए पिछले भाग में हमने कुछ ‘स्मृतियों’ की चर्चा की। कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथ अपने प्राचीन न्याय व्यवस्था के आधार स्तंभ थे।मात्र इन दो – ढाई हजार वर्ष पुराने ग्रंथों के आधार पर भारत में न्याय होता था, यह कहना पूर्ण सही नहीं है। भारतीयों की, अर्थात हिंदुओं की, विशेषता है कि वह देश – काल – परिस्थिति अनुसार अपने व्यवस्थाओं और नियमों को युगानुकूल परिष्कृत करते जाते हैं। ‘जो पुराना है, प्राचीन है, वही सब अच्छा है’ यह कुएं के मेंढकों की मानसिकता अपनी (हिंदुओं की) नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में ‘भाष्य’ यह समयानुसार, लिखे गए वेदों को / उपनिषदों को / स्मृतियों को परिष्कृत करने की एक सर्वमान्य पध्दति थी।इसी कारण धर्मशास्त्र पर (अर्थात न्याय प्रणाली पर) लिखे गए लगभग सभी ग्रथोंपर, समय-समय पर भाष्य लिखा गया। इस्लामी आक्रांता भारत में आने तक यह परंपरा कायम थी। आगे चलकर वह कम होती चली गई।
याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिथिला नगर के वाचस्पती मिश्र ने भाष्य लिखा। सन 900 से 980 यह उनका कार्यकाल था। उनके अनेक ग्रथोंमें से ‘न्याय सूचि निबंध’ और ‘न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका’, यह दो ग्रंथ न्याय व्यवस्था पर है। इनमें से पहला ग्रंथ अर्थात, ‘न्यायसूचि निबंध’ यह, अक्षय पद गौतम के ‘न्याय सूत्र’ इस ग्रंथ पर प्रमुखता से भाष्य करता है। अक्षयपद गौतम का कालखंड यह ईसा पूर्व 200 वर्ष का था। इसी ‘न्याय सूत्र’ पर, आगे चलकर उद्योतकर, भविविक्त, अविधा कर्ण, जयंत भट आदी अनेक विद्वानों ने भाष्य लिखे हैं।
ग्यारहवी सदी मे, दक्षिण मे चालुक्योंके राज्य मे, ‘विज्ञानेश्वर’ नाम के न्यायाधीश ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखा है। यह भाष्य ‘मिताक्षरा’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ‘मिताक्षरा’ ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ ही, ‘जन्म के साथ मिलने वाला उत्तराधिकार’ (Inheritance by birth) इस विषय पर विस्तृत विवेचन है।
विज्ञानेश्वर ने लिखे हुए इस ग्रंथ के लगभग 100 वर्षों के बाद, बंगाल के ‘जीमूतवाहन’ इस परिभद्र कुल के व्यक्ति ने ‘दायभाग’ यह ग्रंथ ‘उत्तराधिकार’ इसी विषय पर लिखा।
अगले 800 वर्ष, बृहद बंगाल (आज के बांग्लादेश सहित) और असम प्रांत में, उत्तराधिकारी संबंधित सभी न्याय दान में ‘दायभाग’ यह ग्रंथ प्रमाण माना गया है। लेकिन शेष भारत के उत्तराधिकार संबंधित मामलों में, ‘मिताक्षरा’ इस ग्रंथ के आधार पर न्याय दिया जाने लगा। आगे चलकर पन्द्रहवीं सदी में, चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी रह चुके, बंगाल के ही रघुनंदन भट्टाचार्य ने ‘दायभाग’ पर भाष्य लिखा। कई स्थानों पर यह भाष्य प्रमाण माना जाता था। अंग्रेजों के शासन के प्रारंभिक काल खंड में, न्याय देते समय हिंदू विधि का उपयोग किया जाता था। अंग्रेजों की पहली सत्ता बंगाल में स्थापन होने के कारण देश का पहला हाई कोर्ट, वर्ष 1862 में कोलकाता में स्थापना हुआ। इस कोलकाता उच्च न्यायालय ने, उत्तराधिकार इस विषय में रघुनंदन भट्टाचार्य के ‘दायभाग’ पर लिखा गया भाष्य प्रमाण माना था।

1. काशी 2. मिथिला 3. मद्रास 4. मुंबई 5. पंजाबसन 2005 में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने ‘मिताक्षरा का आज के संदर्भ में महत्व’ इस विषय पर एक दीर्घ लेख लिखा। इसमें वह कहते हैं कि, ‘पचास के दशक में भारतीय संसद ने सब पुराने हिंदू कानून रद्द करके नए कानून तैयार किये। इसलिए दैनंदिन न्याय प्रणाली में मिताक्षरा के संदर्भ समाप्त हुए। फिर भी, भारतीय न्यायालय व्यवस्था समझने के लिए मिताक्षरा आज भी उपयुक्त है।’अर्थात इन स्मृतियाओ॔ का, या उन पर लिखे गए भाष्य का, विचार किया तो साधारणतः ढाई से तीन हजार वर्ष पहले के ग्रंथो से हमें सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। यह न्याय व्यवस्था केवल कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा, दायभाग ऐसे ग्रंथो तक सीमित नहीं थी, तो प्रत्यक्ष समाज में इसका उपयोग होता था। इस्लामी आक्रांताओं ने जो विध्वंस किया, उसके कारण हमारे पास पुराने आलेख, पुराने कागजात उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो मिले हैं, जो शिलालेख, ताम्रपट मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि, भारत में एक परिपूर्ण सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था थी। सत्ता किसी की भी हो, राजा कोई भी हो, परंतु धर्मशास्त्र ने दी हुई यह न्याय व्यवस्था सर्वमान्य थी और सबके लिए बंधनकारक थी।
विजयनगर साम्राज्य (वर्ष 1336 -1646) के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य में और आगे चलकर, पेशवा के राज्य में भी, न्याय व्यवस्था अच्छी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो पांडुलिपियां मिली है, उनसे उस समय की समाज व्यवस्था, न्याय पद्धति, दंड शासन आदि बातों का स्पष्ट चित्र हमारे सामने आता है। विजयनगर साम्राज्य के आदि गुरु विद्यारण्य अर्थात माधवाचार्य ने पाराशर स्मृति पर ‘प्रसार माधवीय’ ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के ‘व्यवहार कांड’ प्रकरण में न्याय व्यवस्था के यम – नियम विस्तार से दिए हैं। मंगलौर के भास्कर आनंद सालटोर की, विजयनगर साम्राज्य की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में एक अच्छी पुस्तक उपलब्ध है, – ‘Justice System of Vijaynagara’। इसमें उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के न्याय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। साथ ही विजयनगर साम्राज्य में घटित अनेक महत्वपूर्ण न्याय दानों की, अर्थात, कानूनी मामलों के निर्णयोंकी, जानकारी भी दी है।
– प्रशांत पोळ जाने माने इतिहासविद हैं और भारतीय इतिहास , प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक भारत से जुडे़ विषयों पर खोजपूर्ण पूस्तकें लिख चुके हैं)