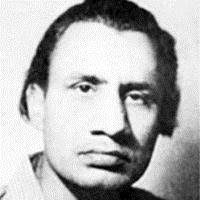सुकवि कन्दर्प नारायण शुक्ल “कन्दर्प” जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा सं०1988 वि०मे सन्त कबीर नगर के धनघटा तहसील के पास मुंडेरा शुक्ल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जी का नाम पण्डित उमा शंकर राम शुक्ल था। इनका सम्पूर्ण परिवार का पंक्ति पावन ब्राह्मण होने के कारण संस्कृत साहित्य से विशेष रूप से जुड़ा रहा। इनकी शिक्षा- दीक्षा साहित्य-शास्त्री और साहित्यरत्न तक सम्पन्न हुई थी। ये स्वतंत्र विचारक के रूप मे अध्ययन-अध्यापन में अपना समय बिताए हैं। कन्दर्प जी बस्ती मण्डल के छंदकारो के चतुर्थ चरण के उन उच्च कोटि के छन्दकारों में अपना स्थान रखते हैं जिन पर बस्ती मंडल को गर्व है। इन्होंने व्रज भाषा में लिखित रीति ग्रन्थों के अध्ययन के साथ-साथ मण्डल के वर्चस्वी छन्दकारों के छन्दों का भी अच्छा अध्ययन किया है। सवैया, घनाक्षरी के उत्कृष्ट कवि होने के साथ-साथ इन्होंने खडी बोली के आधुनिक छन्दो पर भी अपनी लेखनी चलाई है। खड़ी बोली के इनके तीन प्रबंध- काव्य बड़े ही उच्चस्तरीय है। भाव-भाषा के दृष्टिकोण से इनके छन्द-विधान को उत्कृष्टम रूप से देखा जा सकता है।
प्रकाशित पुस्तकें :-
1. निर्वाण (खण्डकाव्य)
2. वेणु गीत
अप्रकाशित पुस्तकें:-
1. मृत्युंजया (खण्डकाव्य )
2. दु:शासन (खण्डकाव्य )
3.कैकेई (प्रबंध काव्य )
4.भ्रमर गीत
5. युगल गीत
6.गौपिका गीत
7. अन्य फुटकर छन्द
रचनाओं का संक्षिप्त परिचय:-
1- निर्वाण ( खण्डकाव्य):-
यह गान्धी जी के ऊपर लिखा गया खण्ड काव्य है। इसमें 12 पृष्ठ है। इसकी चार पंक्तियां प्रस्तुत हैं –
स्व कर्तव्य से नही चूकता
सपने में भी यह इन्सान।
क्योंकि देखता अखिल विश्व में
अपना व्याप्त राम रहमान ।।
2- वेणु गीत:-
वेणु गीत भागवत का पद्यानुवाद है।इसमे कवि भागवत के कृष्णगोपी से सम्वन्धित रासलीला को बहुत मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है। रासलीला की कुछ पक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत है-
जल निर्मल कमल जलाशय में,
मुख देख गर्व से थे फूले।
गुन गुन गाते थे गान मधुर,
जिन पर भौरे भ्रम में भूले ।
यों वर्णन करते गृह प्रिय के प्रेम विभोर ।
गुजरिया सब लेने लग गयी स्नेह हिलोर।
बन गयी भिलानियां फिर श्यामा श्याम ।
उभयस्थिति में लीन तनिक मन में विश्राम।
इस भांति नित नवप्रेम प्रिय के पगी सप्रेम।
करकर मनोहर गान पानी स्व पद निर्वान।।
खड़ी बोली के खण्ड काव्य:-
कन्दर्प जी के प्रौढ खंड काव्य तो विशुद्ध रूप में खड़ी बोली में लिखे गये हैं। उनको पाण्डुलिपिया देखने को मिली। जिनके माध्यम से इस खण्ड काव्य पर प्रकाश डाला जाएगा।
अप्रकाशित मृत्युंजया (खण्ड काव्य):-
इसकी रचना कन्दर्प जी सम्बत 2003 में किया । इस पाण्डुलिपि में 45 पृष्ठ हैं जो बड़े आकार में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 6 सर्ग हैं। इसकी भाषा खड़ी बोली है।
संक्षिप्त कथावस्तु:-
मृत्युंजया की कथावस्तु का प्रारम्भ राजा अश्वपति के तपस्या मे किया गया है।पुत्र प्राप्ति हेतु राजा ने कठोर तपस्या किया किन्तु इनको पुत्र की जगह पुत्री प्राप्त हुई। इस पुत्री का नाम सावित्री रखा गया और सावित्री तथा सत्यवान की चिर-परिचित कथा को उपजीव्य बना करके सम्पूर्ण कथावस्तु को विस्तृत आकार दिया गया है।
प्रथम सर्ग –
प्रथम सर्ग का प्रारम्भ भारतीय गरिमा के गुणगान से हुआ है। यथा-
उस काल के जितने पुरुष थे,
शिष्ट थे नव निष्ट थे।
सारी कलाओ में कुशल थे,
अति महान वरिष्ठ थे ।
उस काल का मानव समाज
दयालु हिंसा विरत था।
नात्सये, दम्भ विहीन धर्म
विकास ही में निरत था।।
– (मृत्युंजया प्रथम सर्ग पृष्ठ 1)
तपस्यारत राजा को काम विचलित करता चाहता था। कवि ने उसका चित्रण बड़ा सुन्दर ढंग से किया है। काम की दशा देखिये –
जो वृक्ष पत्रविहीन थे
उनमे सरसता आ गयी।
नवपत्र पुष्पों से मनोहरता
अलौकिक छा गयी।
नदियाँ चली कलनाद करती
उदाधि और उमंग में।
भौरे चले कुछ गुनगुनाते
आ कमल ढींग रंग में।
मधु प्रेम में पागल वना
दक्षिण पवन चलने लगा।।
– (मृत्युंजया प्रथम सर्ग पृष्ठ 3)
द्वितीय सर्ग –
द्वितीय सर्ग का प्रारम्भ उषा कालीनचित्रण से होता है। उसके बाद किशोरावस्था में पहुँचती हुई सावित्री का वीणा वादन के मनोहर प्रसंग का वर्णन किया गया है–
अरे कौन यह छेड़ सप्त स्वर
निज मानस में लीन।
भाव हृदय में उठा रही है
जग के मधुर नवीन ।
अहद केश कैसे काले हैं
सजल पयोध समान ।
कैसी इस कमनीय कान्ति पर
लज्जित स्वर्ण विहान ।
पटतल भी लज्जित हो जाता
अरुण कपोल निहार।
भुज मृणाल पर कैसा पुलकित
सरसि रुह अविकार ।
अंचल देख चला जाता है
मदन केतु झकमार ।
लच जाती कटि वच जाती
पर पीन पयोधर भार।।
– (मृत्युंजया द्वितीय सर्ग पृष्ठ 5)
तृतीय सर्ग –
तृतीय सर्ग में सावित्री पिता के आदेश से तपभूमि में तप हेतु जाती है। प्राकृतिक छटा के बीच रूपवती सावित्री का सौन्दर्य द्रष्टव्य है-
राजकन्या रथ पर लामोद ,
चन्द्र ज्यों नील गगन की गोंद ।
देखती हुई दृश्य कमनीय
जा रही थी भर सुषमा हीय ।
+ + + +
कहीं नदियों का कलकल नाद ,
न जीवन में जिनके अवसाद।
कहीं निर्झर की झर झर तान,
दे रही जो मानस सुखदान ।
– (मृत्युंजया तृतीय सर्ग पृष्ठ 8)
यात्रान्त में सत्यवान तपोवन में रूपवती सावित्री से मिल ही जाता है। उसके सौन्दर्य पक्ष को दोनों के राग से जोड़ते हुए कवि ने बड़े उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया है-
तप्त हेमाभ गात की कान्ति,
देखकर दिनकर की ही भ्रान्ति।
बड़े दृग थे अरविन्द समान,
अधर के पटल थे उपगान।
शान्त रस से था भरा शरीर,
धरा पर ज्यों सागर गंभीर ।
वीचियो सा प्रलम्ब युग वाह,
भरा था जिसमें अति उत्साह।
लहराती शीश जटाएं लोल,
दिखाती थी सौंदर्य अमोल।
अरुण चन्दन से शोभित भाल,
उदित ज्यों प्राची ने रविवाल।
भरा था अंग-अंग में ओज,
प्रफुल्लित करता मन सरोज ।।
– (मृत्युंजया तृतीय सर्ग पृष्ठ 10 )
सावित्री सत्यवान के इस रूप पर मोहित हो गई। सत्यवान भी उसके रूप पर मोहित हो गया। सत्यवान का परिचय देते ही सावित्री के पूर्वराग का चित्रण कवि ने बड़े उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया है-
राज कन्या उस क्षण अनिमेष
सौम्य उस आगन्तुक का वेष ।
देखती थी हो प्रेम विभोर
मयूरी ज्यो सावन घन ओर ।
कर रही थी न्योछावर प्राण
दे रही थी निज मानस दान ।।
– (मृत्युंजया तृतीय सर्ग पृष्ठ 11 )
सावित्री के साथ आमात्य ने उसके पिता अश्वपति का परिचय दिया। सत्यवान ने भी अपने पिता द्युमत्सेन (भूतपूर्व शाल्व नरेश) का परिचय दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सावित्री केअभिवादन के साथ दिवसावसान हो गया। कवि ने इस प्रसंग का चित्र आश्रम के अंचल से प्रस्तुत किया है-
इस तरह हुआ दिवस अवसान
सुनाये चिडियों ने कल गान ।
मधुर सन्ध्या से पा अनुराग
श्रवण कर सामवेद का राग ।
पद्मिनी का संकोच निहार
स्पर्श कर शीतल मन्द बयार ।
हवन की धूम घटाएँ धूम
रही थी दशो दिशाएँ चूम ।
स्वस्ति स्वाहा ध्वनि का उच्चार
कर रहा था जीवन संचार।।
– (मृत्युंजया तृतीय सर्ग पृष्ठ 13 )
रात्रि में सावित्री और सत्यवान का मिलन प्रणय का उपहार बन करके दोनों के अन्तस्पटन को चन्द्रधनुषी कल्पनाओं से अनुरंजित करने लगा। स्नेह के लालित्य ने माधुर्य भरी उत्कंठा का सृजन कर प्रणयानुभुति की ओर अभिप्रेरित किया। पर प्रेरणा में रागानुरक्त उभय किशोर और किशोरी में आनन्द की भावभूमि पर प्रणय का सम्वर्द्धनात्मक सृजन हुआ।
चतुर्थ सर्ग-
राजा अश्वपति की सभा में सभा के सम्मुख सावित्री द्वारा प्रणय प्रस्ताव रखने पर नारद ने रहस्य को खोलते हुए कहा सत्यवान तो केवल एक ही वर्ष जीवित रहेगा। किन्तु राजा ने सावित्री के अटल प्रेम को देखते हुए उसे पाणिग्रहण की स्वीकृति प्रदान कर दी।
पांचवां सर्ग –
पाँचवे सर्ग में राजा अश्वपति अपने धर्मपत्नी मालवी के साथ तपोभूमि ये जाकर कन्या दान करते हैं। सावित्री के प्रवेश से वनभूमि मंगलमय हो गई। उसने राजसी परिवेश को त्याग करके आश्रम व्यवस्था में परिवार की सेवा-सुश्रुषा का भार संभाला। उसके गार्हस्थ्य जीवन का चित्रण अत्यन्त ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है-
बेला प्रभात बन के जगती जगाती ।
आमोद कन्ज मन मानस में खिलाती।
गार्हस्थ्य जीवन प्रसन्नतया चलाती ।
थी राजती उटज मध्य कोमलांगी।।
– (मृत्युंजया, पचम सर्ग, पृष्ठ 28)
षष्ठ सर्ग-
बसन्ततिका छन्द का प्रयोग बढ़ा उत्तम है। षष्ठ सर्ग सावित्री के स्वप्न से प्रारंभ होता है। वह अनिष्टकर स्वप्न देख करके कॉप- सी उठती है क्योंकि एक वर्ष बीत चुके हैं और उसके पति के मृत्यु के दिन सन्निकट आने वाले हैं। उसे नारद का कथन स्मरण हो आता है। वह अपने बचपन कीस्मृतियों से तन्वंगी लतिका के समान अनिष्ठ के झंझावातों से थरथरा उठती है। बचपन के सुख के दिन स्मरण हो आते हैं। उसका चित्रण कवि ने बड़ा की मार्मिक प्रसँग के संदर्भ में किया है-
मोतियाँ निष्प्रभ दतुलिया जब दिखाती खोल।
बोल मिश्री घोलती या बोलती तूं बोल ।
लटपटी सी चाल अति बिखरा हुआ सा बाल।
देवता किसको फसाने का रचा यह जाल।
धूल से हो धूसरित माँ की मनोरम गोद।
दौड़ना पीछे द्विजों के आमुदित सविनोद।
तितलियों को दौड़ धरना और करना खेल।
कभी आपस में झगड़ना कभी करना मेल।
क्या कभी मैं भी रही शिशु बोल नभ क्यो मूक!
आह! आज पपीहरी क्यो दे रही उर हूक।।
इसी मार्मिक प्रसँग को वर्षा के मार्मिक चित्र के माध्यम से कवि ने और मार्मिक बना दिया है –
आह!सावन मास वह घिरनाघनों का ब्योम
गर्जना के साथ बूंदों की झड़ी सुकुमार ।
देखना दिन में न दिनमणि रात्रि तारकसोम
चंचला की चमक इन्द्र वधूटियों का प्यार ।
कलितनृत्य कलापियोंका ललितपंख पसार
लहरना हरियालियों का ले पवन का प्यार
झूलना अलि संग में अति मंद झूले डाल।
प्रेम से गाना मुदित हो मधुर गीत रसाल ।
हाय!अब ये क्षण कहां सामने कर्म क्षेत्र ।
आलियाँ ससुराल में हैं जलसे भरे हैं नेत्र।
सोचते ही गिरे लोचन सुक्त मौलिक विन्दु।
मनो अम्बर से गिरे दो झलमलाते इन्दु ।।
– (वही, षष्ठ सर्ग, पृष्ठ 31.)
बनाली के रात्रि पर लिखी गई पंक्तिया द्रष्टव्य हैं-
जुगुनुओं के दीप ये कैसे हवा मे अड़े हैं।
उस अनन्ताकाश में नक्षत्रनभ जैसे जड़े हैं।
– (वही, षष्ठ सर्ग, पृष्ठ 33 )
उपमा अलंकार का बड़ा सुन्दर प्रस्तुतीकरण किया गया है। सत्यवान कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसके लकड़ी का काटना बन्द होते ही यमराज एक तप:पुंज के रूप में अवतरित हुए। सावित्री ने यमराज को कैसे देखा-
अकस्मात सुधांश सी किरणें चतुर्दिक शुभ्र फ़ैली।
धुल गई हो गई निर्मल पूर्वमा जो थी रात्रि मैली ।
आह यह क्या स्वप्न या सच द्यौतिता क्यो दिशा सारी ।
सामने तब तक वहीं अति सौम्य प्रतिमा वह निहारी ।।
– ( वही , अष्ठ सर्ग, पृष्ठ 35)
तप:पुंज यम को देख करके और उनका परिचय पा करके सावित्री काप उठी। उसने उनके पधारने का कारण पूछा-
यम ने कहा कि पापात्माओं के लिए हमारे दूत जाते हैं, किन्तु पुण्यात्माओं के लिए मैं स्वय आता हूँ। सावित्री का विक्षुब्ध मन डबडवी आखो से भय से प्रश्न कर उठता है –
देव तो बताइये यह पुण्य क्या है पाप क्या है।
जल रहा जिससे जगत एसा भयंकर ताप क्या है।
कर्म वह कैसा कि कर नर स्वर्ग या अपवर्ग पाता।
कौन सा दुष्कर्म कर वह नरक का चक्कर लगाता ।।
यम ने कहा कि शुभ कर्म के कारण ही मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसा कहता हुआ सत्यवान के प्राणों को लेकर ज्यो-ज्यों यम ऊपर बढ़ने लगा त्यो-त्यो तपोधना सावित्री
भी ज्योतिर्मयी हो उसके पीछे-पीछे चलने लगी। यम ने पीछे घूमकर जब सावित्री को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गये।
यम ने कहा कि शुभे, सत्यवान के अत्तिरिक्त तुम्हें जो भी प्रिय हो मांग लो। सावित्री ने अपने सास-ससुर के नेत्र की रोशनी पुन. वापस मांगा। यम ने वरदान देकर जैसे कदम बढ़ाया पुन: पीछे लौट कर देखा-
देखते नारी वही युग हाथ में संसृति संभारे।
है खड़ी उस शून्य पथ पर एक तीव्र प्रकाश डारे।
यम आवेश में बोल उठा-
किस प्रबल बल पर हमारा अनुसरण तू कर रही है।
मानवी होकर अरे जो देव के सँग अड़ रही है।
सावित्री ने निर्भीकता से उत्तर दिया-
पति जहाँ को जा रहे पत्नी वहीं की जा रही है।
धर्म क्या इसमें विलक्षणता तुम्हें दिखला रही है।
व्रत नियम शुभ आपके आशीष का ही है सहारा ।
तब भला क्यो कर कहाँ अवरुद्ध मेरी प्रगति धारा।
यम ने पुन वर मांगने को कहा।
सावित्री ने कहा कि मेरे पुत्रहीन पिता के सौ पुत्र हो जाय।
यम ज्यों आगे बढ़े, अनन्त आकाश की छाती को चीरती हुई सावित्री यम के अन्त:मन को झकझोरने लगी। पुन: यम ने वर मांगने को कहा।
सावित्री ने कहा कि मेरे पिता को उनका सम्पूर्ण राज्य मिल जाय। यम वरदान देकर अदृश्य होना चाहते थे। सावित्री ने उनसे कहा –
धर्मराज अदृश्य हो जाओ न मैं कुछ रोकती हूँ।
किन्तु कुछ बाते थी जिससे आप को अब टोकती हूं।
यम दुविधा में पड़ जाते हैं। यम को द्विचित देख करके पति विहीन सावित्री का मन करुणार्द्र हो जाता है। वह कहती है-
हाय जीवन का हमारे कौन होगा जब सहारा ।
हिचकियों के साथ आंखों से चली वह अश्रुधारा ।।
सावित्री के इस करुणाजन्य मार्मिक प्रसँग को कविवर कन्दर्प जी ने बड़े ही कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। भावों की गहराई में उतर करके पूर्व परिचित कथायें रोचकता का सृजन करके उसे नवीनता के कलेवर में बाँधने का सफल प्रयास किया गया है। सावित्री के करुण दृश्य को देख करके यम ने सौहार्द्र भरे स्वर में कहा कि जाओ तुम्हें एक वर्ष के अंदर पुत्र-रत्न प्राप्त हो। यह सुनकर सावित्री का मन आह्लाद से भरने लगा। तब तक बैतरिणी नदी निकट आ जाती है।
सावित्री ने यम से पूछा कि भगवन मुझे आप पुत्रवती का वरदान दे करके मेरे पति के प्राणो को छीनकर करके ले जा रहे हैं। क्या यह न्याय है? यम का अन्तर्मन सावित्री के इच्छाओं से आह्लादित हो करके बोल उठा-
जो तुम्हें स्वीकार मुझको भी वही स्वीकार।
मृत्यु की गति है अकथ यह दूर-दूर विचार।
देवि, तेरे नाथ को अब प्राप्त जीवन दान ।
सुन हमारी ओर से अब और कुछ वरदान।
यम ने कहा –
रिद्धियां तुम्हारा मुख जोहती रहेंगी सदा,
सिद्धियां भरी उमग चंवर डुलाएंगी।
नर नाग किन्नरों की बातें ही चलानी वृथा
जातियाँ सुरो की सब गुणगान गायेगी ।
अलग विभूति जिसकी न अनुभूति जग,
सतत विनीत नत नम्रता दिखायेंगी।
दुख बिनसायेगी प्रमोद उपजायेगी वे,
तेरे भाल भाग्य चार चाँद चमकायेगी ।।
– ( वही, षष्ठ सर्ग, पृष्ठ 43)
कन्दर्प जी का “मृत्युंजया” खण्ड- काव्य कथावस्तु के दृष्टिकोण से पूर्व परिचित होते हुए भी अपने में मौलिक और नवीन है। सती सावित्री के आदर्श प्रेम को कवि ने भारतीय नारी के बाद परम्परा के लिए मौलिकता के साथ सर्वजनीनता प्रदान किया है। मार्मिक प्रसगों की अभिव्यक्ति ने रसानुभूति का सिलसिला बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाषा में लालित्य के साथ प्रवाह है। कन्दर्प जी की यह कृति खण्ड काव्य को सभी विशेषताओं से पूर्ण है। यदि उसे आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ खण्डकाव्य कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। अपने संशोधित रूप में प्रकाशित होते ही “मृत्युंजया” खण्ड-काव्य का काव्य सुधी अवश्य समादर करेगे।
दु:शासन (खंड काव्य) :-
यह कन्दर्प जी का खड़ी बोली का उत्कृष्ट खंड-काव्य है। इनकी पाण्डुलिपि देखने को मिली। इसमें कुल 50 पृष्ठ हैं। एक से 6 पृष्ठ तक प्रस्तावना लिखी गई है। 6 से 50 पृष्ठ तक महाभारत की चिर-परिचित कथा विविध संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 सर्ग है जिनका नाम कवि ने यथोचित रूप से प्रस्तुत किया है
1.निर्देश पर्व। 2. सुषुप्ति पर्व। 3. अंतर्द्वंद्व पर्व। 4.उद्बोधन पर्व और 5.ऐन्द्रजालिक पर्व ।
1.निर्देश पर्व –
इसकी कथा को कवि ने दुर्योधन के क्रोधावेश को चित्रित करते हुए द्रौपदी के चीरहरण के लिए दु:शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। कवि ने इस प्रसंग का वर्णन बड़े ही सशक्त भाषा में किया है-
तर्जनी उठाकर बोल उठा
यों छूता उसका मन क्षेत्र ।
उन बंकिम भृकुटि कमानो पर
थे चढ़े हुए आग्नेय नेत्र।
तड़ तड़ा उठा वर वर्म मर्म,
कड़ कड़ा उठा मन अतुलनीय।
विहवल सा चरणो के आगे
झुक पड़ा हुआ सा उत्तरीय ।।
– (दु:शासन, प्रथम सर्ग, पृष्ठ 11)
निर्देश पर्व नाम यहाँ सार्थक हो जाता है। सम्राट दुर्योधन के क्रोधावेश को देख कर दु:शासन कह उठता है-
कुछ चिन्ता करें न महाराज !
यह समुपस्थित सर्वदा दास ।
अरुणोदय के ही साथ साथ ।
देखेंगे मैरा अटटहास ।।
– (दु:शासन, प्रथम सर्ग, पृष्ठ 11)
कवि ने दु:शासन को अनीति का पक्षधर न दिखा करके उसे नैतिकता का पक्षधर दिखाया है। किन्तु राजाज्ञा का
पालन उसका प्रधान धर्म था। इसलिए इस पर्व की सम्पूर्ण कथा निर्देश पर्व से सबंधित है।
2. सुषुप्ति पर्व –
इसमें कवि ने दु.शासन को सोते हुए स्वप्नावस्था में दिखाया है। वह स्वप्न में ही जिस समय द्रौपदी के पास पहुंचता है, वहाँ का चित्र कवि ने द्रौपदी के सौन्दर्य के माध्यम से बड़ा सुन्दर प्रस्तुत किया है-
छवि पर इन्दीवर का विलास
मुस्कान उषा की ललित भाल।
यह देख खेलने लगा मुग्ध
भौरों सा भूषित चिकुर जाल।
जगमगा उठे कर में कंकन
कानों में चंचल कर्ण फूल।
पद में नूपुर की क्वगन मधुर
तन पर शोभित स्वर्णिम दुकूल ।
पदिटका निवेष्ठित गर्वोन्नत
उभरे अंगों का था निखार।
जिस पर त्रिवली चुम्बन करता
मणि माल लगा करने विहार।
नासा पुट पर था झलक रहा
मानो तारा बन स्वयं इन्दु ।
हस रहा विवुक के कोने में
छोटा सा तिल का एक विन्दु ।
देखा दु:शासन ने सम्मुख
वह पावन पेसल रचिर रूप ।
मन चित्र आप बन जाता था
चित्रित कर जिसकी छवि अनूप ।
स्वप्निन सा जीवन झांक उठा
अन्तर मन से होकर विभोर ।
मानो भावों का वातायन
दे रहा नवल सदेश भोर ।।
– (दु:शासन, पृष्ठ 15)
द्रौपदी के पास दु:शासन पहुंचा ही नहीं थाअपितु उसे स्वप्नावस्था में राजसदन का सम्पूर्ण चित्र चल चित्रवत दिखायी पड़ रहा था। इस छन्द को कवि ने बड़े कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है-
नूतन रसाल के पत्रों पर,
लिख मंजरियों का मधुर प्यार।
वर वदनवार हस रहा ज्यो
माधव महीप के खड़ा द्वार ।
पोहित मुक्ता कंचुकी मध्य,
उद्भावित जैसे वक्ष द्वीप ।
वैसे मंगल घट पर जगमग
मंगल ग्रह में मांगलिक दीप।
नाचती मुदित हो सुमनो पर
फूलों सी फूलों की परिया ।
मधु घोल घोल कर नयन बीच,
मानो आई हो किन्नरिया ।
उसमें था एक विशाल कक्ष,
वह शान्ति सदन कहलाता था।
डरते-डरते सुरभित समीर
जिसमें पद पदम बढ़ाता था।
प्रात:रवि रश्मि उतर जिसमें
मनचाही करती रंग रेली।
रावा की मन्द हँसी जिसमें
भर रजनी करती अठखेली।
डरते करते सुरभित समीर
जिसमें पद पदम बढ़ाता था।
प्रात: रवि रश्मि उतर जिसमें
मनचाही करती रंग रेली।
रावा की मन्द हंसी जिसमें
भर रजनी करती अठखेली।।
– (वही, पृष्ठ16)
स्वप्न के इस प्रसग में कवि ने सौन्दर्य पक्ष को उभारा ही नहीं है,अपितु अत्यन्त ही उत्कृष्ट बना दिया है। छन्दों में सौन्दर्य का उल्लास है। रवि रश्मियों का मनचाहे ढंग से रंगरेलिया करना और शान्ति कक्ष में डरते-डरते सुरभित समीर का पद पदम बढ़ाना मानवीयकरण के पक्ष को अत्यन्त उभार देता है। यहाँ कवि की समर्थता बड़ी सशक्त हो जाती है। इसी ही पर्व में कवि ने दु.शासन को स्वप्न में जिस समय द्रौपदी के सम्मुख पहुंचाया है, इसका चित्रण देखिये-
दु:शासन के मुखमंडल पर
चिन्ता की खचित मलिन रेखा ।
यह भावअलक्षित रह न सका,
कृष्णा ने निज आंखों देखा।।
– (वही, पृष्ठ19)
दुःशासन को दुर्योधन का आदेश याद हो जाता है। अन्तत: जब वह अपनी बात प्रस्तुत करता है तो द्रौपदी चौंक पड़ती है-
एसा सह सहसा चौंक पड़ी
वह डोली या धरती डोली।
तत्क्षण सांस भर कर उर में
धीरे-धीरे कृष्णा बोली ।
कृष्णा अनुमोदिता वाणी को
कृष्णा से अनुमोदित माना ।
सच होता द्वेष दोष धरती
अब हमने जाना पहचाना।।
– (वही, पृष्ठ 22)
यहाँ पर कवि ने द्रौपदी और दु:शासन के कथनोपकथन को बड़ा व्यावहारिक रूप दिया है। दु:शासन अपनी मजबूरी व्यक्त करता है। यह कहता है कि मैं राज- आदेश के कारण यह दुष्कर्म कर रहा है। द्रौपदी दु:शासन को धिक्कारते हुए कहती है-
देखा कुसँग का ही फल था
सागर जैसा जीवनाधार ।
बन्धन में बांधा गया कही
कोई न मिला साथी उदार ।।
निज हित की नहीं सोचती मैं
सोचती नहीं मानापमान ।
यह भी न सोचती जीवन का
कैसे रक्षित हो स्वाभिमान ।।
सौचती नहीं यह जन समक्ष,
जो आज हो रहा नग्न नृत्य ।
सोचती नहीं बस कुरुपति के
कुत्सित शासन का यह कुकृत्य ।।
सोचती नही वैभव सारा,
क्या से क्या अब हो गया हाय ।
रह गया न जीने का चारा
सोचती नहीं हूँ नि:सहाय ।।
सोचती नही पाँचो रक्षक
कौरव नरेश के बने दास ।
सोचती नहीं हो खेल-खेल
सामने नियति का व्यंग्य हास ।।
सोचती नहीं भी सारे जो
हो रहे कर्म हैं अति मलीन ।
सोचती नहीं यह भी न यहां
कोई न सोचता समीचीन।।
सोचती किअब यह आर्य भूमि
बन जायेगी मरघट मसान ।
सोचती कि अब यह सुनने को
हा मिल न सकेंगे साम गान ।।
सोचती कि अब यह भारत में
आयेगा कभी न स्वर्ण काल।
सोचती किअब यह शोषित सी
हो जाएगी बसुमती लाल।।
मैं नहीं चाहती वसुधा में
कटुता का चलित रहे चक्र।
जन अहंमन्यता में समझे
अपने को ही सुरराज शक्र।।
मैं नहीं चाहती धरती पर
घन अंधकार का हो प्रसार ।
मैं नहीं चाहती धरती से
पावन प्रकाश का बहिष्कार ।।
मैं नहीं चाहती जन जन में
छिड़ जाये यह गृह दाह युद्ध ।
मैं नहीं चाहती ईर्ष्या में लुट
जाये निज संस्कृति विशुद्ध ।।
मैं नहीं चाहती धरती का
हो जाये यह स्तमित भानु।
मैं नहीं चाहती बुझ जाये
प्रज्ज्वलित स्वजीवन का कृशानु।।
मैं नहीं चाहती वाणी का
जन – जन पाए न सुधा दान।
मैं नहीं चाहती विग्रह का कुछ
भी न हो सके समाधान ।।
मैं नहीं चाहती भरत खण्ड
कट-कट हो जाये खण्ड- खण्ड ।
मैं नहीं चाहती मिट जाये ये
अगणित नभ के मार्तण्ड ।।
चाहती कि फूले फले विश्व
चिर हरे भरे ये रहें क्षेत्र ।
चाहती कि करुणा वरुणी की
प्रवरों से पूरित रहे नेत्र।।
चाहती कि भावी पीढ़ी का
सर नीचा हो न सके ललाम ।
चाहती कि जन के रोम रोम
रम रहे सुधा सा राम राम ।।
कामना किशोरी के उर का
टूटे न कही बहुमूल्य तार ।
भावना विभोरी के पुर भी
लूटे न कही दस्यु ज्वार ।।
– (वही, पृष्ठ 28)
द्रौपदी साधारण नारी ही नहीं अपितु कवि के संदर्भों में वह चण्डी है, महामाया है। स्वप्न में द्रौपदी दु:शासन को उसके काल के समान लगी। उसने कहा –
यो तो मेरा वह नग्न रूप
तुम देख नही सकते किशोर ।
कुसुमादप कितनी कोमल हूं
बज्रादप कितनी हूं कठोर ।।
– (दु:शासन, पृष्ठ 29)
और महाभारत की अन्य घटनाएं, कृष्णा का विलाप, साड़ी का ढेर, धनंजन तप के साथ अन्तत: दुर्योधन का वह स्वप्न के अन्तिम क्षणों में जब यह देख रहा था तो उसकी नींद सहसा खुल गयी –
झटका सा सहसा लगा उसे
संछिन्न हुआ मन का सितार।
स्वप्नों के मोती विखर उठे
सुनकर कुल हू की पुकार ।
सुषुप्ति पर्व के अन्त का यह छन्द कवि ने बड़े को मनो वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है।
3.अंतर्द्वंद्व पर्व-
प्रात: काल होते ही दु:शासन कृष्णा के पास पहुंच जाता है। यह मन ही मन सोचता है-
क्या सपना सचमुच सच होगा
होगा सचमुच क्या अंधकार
क्या देश डूब ही जायेगा
कोई न मिलेगा कर्णधार ।।
दु:शासन के मन का द्वंद उसे विकल किये हुए है किन्तु अंततः राजाज्ञा पालन हेतु कर्तव्यनिष्ठ होना ही था। दु:शासन के रौद्र रूप को देखकर कृष्णा भयभीत हो गई-
देखा कृष्णा ने आगत की
आँखें थीं दोनो लाल लाल।
भौहें मौर्वी ही झुकी हुई
कंधे पर थी गुरु गदा लाल।।
– (वही पृष्ठ 38)
4.उद्बोधन पर्व-
इस पर्व में कृष्णा राजसभा पहुँच जाती है। दु:शासन से बार-बार दुर्योधन कहता है कि इसे भरी सभा में नचाओ। आज यह दासी मेरे जंघे पर आकर बैठेगी। कृष्णा दुर्योधन के उस अनाचार से क्रुद्ध हो जाती है। वह अत्याचार को ललकारती हुई भरी सभा को चुनौती देती है-
आक्रोश अमर्ष व्यथा लेकर
युग आंखों में लेकर पानी ।
उद्बोधन देती सी कृष्णा
बोली नय नीति भरी वाणी ।
कोमल कठोरता का मिश्रण
देख ना देख बस नारी है।
नारी फूलो की क्यारी है
नारी उड़ती चिनगारी है।
अतएव मान जा अभिमानी
तुमसे यह प्रश्न हमारा है।
वह क्या सचमुच है अधिकारी
तो पूर्व स्वयं ही हारा है।।
नारी के स्वत्व की रक्षा पुरुष के साथ होती है। किन्तु यदि पुरुष स्वय नाकाम हो जाता है जो उसे अपनी रक्षा के लिए रणचंडी बनना पड़ता है। दुर्योधन के अनाचार को चुनौती देती कृष्णा ने भारतीय नारियो को मर्यादा की रक्षा की शंखध्वनि किया, उसको कवि ने बड़े ही आधुनिक संदभाँ मैं प्रस्तुत किया है। पंक्ति पंक्ति नारी जागरण के आयामी को अग्रसारित करने में सबल और सक्षम है।
5.ऐन्द्रजालिक पर्व-
कवि ने दु शासन को ऐन्द्रजालिक के रूप में चित्रित किया है। एक तरफ कृष्णा करुण क्रंदन कर रही थी, दूसरी तरफ दु:शासन न्याय और अन्याय के चक्कर में पड़ा हुआ अपने को समक्षने में असमर्थ पाता है। वह मन ही मन कह उठता है –
अपने हाथो कब अपनो का
सम्मान उतारा जाता है।
अपने हाथो कब अपनों का
परिधान उतारा जाता है।।
दु:शासन यह जानता था कि नटवर नागर कृष्ण के रहते कृष्णा की लाज कभी नहीं जा सकती। कवि ने इस प्रसग को एक नया मोड़ दिया। यहाँ स्वयं दु:शासन इन्द्रजाल करने में लग गया है । उसके इन्द्रजाल से सारी सभा चकित हो गई। दु:शासन अपनी माया से द्रौपदी का चीर ही हरण नहीं कर रहा था अपितु अम्बर का अम्वार लगाता चला जा रहा था। लोगो को देखने में वह चीरहरण कर रहा था लेकिन उसने वस्त्रों से द्रौपदी के तन की हो ढक दिया। वह दुर्योधन से कहता है कि-
भैया यह कैसे चीर खिंचे
सामने छा रहा अंधियारा।
अम्बर के है अम्बार लगे
कुछ नहीं सूझता है चारा ।।
दुःशासन के उस वधन पर सारा जन समूह बोल उठा-
कह उठा उपस्थित जनसमूह
यह बड़ी कठिन प्रभु माया है।
देखो कैसे उस अबला का
ईश्वर ने चीर बढ़ाया है।
कवि ने काव्य के अन्त में दु:शासन को एक कर्तव्यरत एक आदर्श सेवक माना है। चीरहरण का कारण दुर्योधन है न कि दु:शासन। अन्त में कवि कहता –
दुर्योधन के संकेतों पर
जब तक दु:शासन नाचेगा।
उत्पीड़न की अन्याय कथा
तब विवश मनुज ही बाँचेगा।
दुर्योधन के आदेशों को
गुरजन जब तक दुहरायेगे ।
हर दु:शासन को विवस विकल
वे भरी सभा में पायेंगे ।।
दु:शासन खण्ड-काव्य अपने में पूर्ण सफल है। भाषा, रस छंद और अलंकार के दृष्टिकॉण से उसमें प्रयुक्त छन्द भावों के अनुकूल है। छन्दों में प्रवाह है, लालित्य है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से अर्थ गाम्भीर्य के साथ-साथ विषय वस्तु नै निरूपण में सफलता मिली है। कवि ने दु:शासन को एक आज्ञाकारी सैनिक का रूप दिया है। उसके अनुचित चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। साथ ही साथ दुर्योधन के अनाचार को चुनौती देने में कृष्णा का स्वरूप भारतीय नारी की शक्ति सामर्थ्य को उद्द्घाटित करता है। अनाचार का विरोध करना और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना कृष्ण जैसी भारतीय नारिया जानती हैं।
कैकेयी प्रबंध काव्य :-
कन्दर्प जी का यह तीसरा प्रबंध काव्य है जो अभी अपूर्ण है। यह आठ सगों तक लिखा गया है। इसमें अभी तक 86 पृष्ठ थे । भाषा खड़ी बोली है। कैकेयी के कथा-शिल्प को साकेत के उर्मिला के आधार पर किया गया है। कैकेयी के चरित्र को कवि ने एक आदर्श क्षत्राणी के रूप में चित्रित किया है। इस खण्ड-काव्य की भाषा सस्कृतनिष्ठ है। कहीं-कहीं तो छन्दों मे अत्यंत लालित्य है, कहीं-कहीं बड़ी भी शिथिलता और अप्रवाह है। दु:शासन और मृत्युंजया की तुलना मे “कैकेयी” प्रबन्ध काव्य शिथिल सा लगता है। सम्पूर्ण कथा की विषय-वस्तु को अव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किये जाने के कारण रोचकता कम है। इस काव्य छन्दों में सुधार की अपेक्षा है।
भ्रमरगीत, युगल गीत और गोपिका गीत कन्दर्प जी की लघु काव्य कृतियां है। इन सभी पुस्तकों के प्रसँग को राधा-कृष्ण के जीवन से जोड़ा गया है। इसमें भक्ति की भावुकता और आनन्द की रसानुभूति कवि ने अधिक संजोने का प्रयास किया है।
कन्दर्प जी की समस्या-पूर्तिया :-
कन्दर्प नारायण जी सवैया और घनाक्षरी के अच्छे कवि हैं। “रसराज” कानपुर में इनके कई छन्द छप चुके हैं। यहा कुछ प्रस्तुत है-
चार वर्ष से बाढ़ आ रही समस्त प्रजा
अन्न कीतबाही से रही न किसी काम की ।
पूजा के किए भी नहीं अक्षत हुआ है कहीं
मन्द को चली है मुख प्रतिमा तमाम की।
कैसे हो जुताई और खेत की बोवाई जब
वैल की दिखाती मूर्ति मात्र अस्थिचाम की।
मिलती तकाबी जो लुटेरे लूटते हैं बीच
नाजुक समस्या है बड़ी हमारे ग्राम की ।।
– (रसराज, नवम्बर, 1956)
कितने कल कंज हंसे विहरें
झड़के पल में पग धूरि हुए ।
कितने अति मोद प्रमोद बने
बन के घर के घर घूर हुए।
कितने धन धाम निकाम भरे
निज जीवन से मजबूर हुए ।
अनुराग को राग सुना करके
जब से हमसे तुम दूर हुए।।
– (रसराज, नवम्बर, 1959)
इसी क्रम में पूर्ति पटल का एक छन्द द्रष्टव्य है-
पैर सड़ जाते कीच काच से यह मानता हूँ
दुर्दशा भी होती मच्छरों से मृदुगात की।
पंखियों के भय से प्रकाशहीन कमरे मे
जेई नहीं जाती है रसोई बनी रात की।
दुख में अवश्य पर निहित इसी में दिव्य
भव्य शुभ कामनाएँ मनुज जमात की।
होती न उपज नर मरते क्षुधा से क्षत
जो पे यह आती न बहार बरसात की ।।
पुनः”छवि है” की पूर्ति देखें –
मुस्काती हुई कलियों में छिपी
किसकी क्या टटोलती सी छवि है।
कुहूं तो कुहूं की मधुबोलियों ने
किसकी रस घोलती ती छवि है।
हिय के पट खोलती डोलती सी
जिसकी मन बोलती सी छवि है।
किसके रंग में सराबोर सभी
किसकी अनबोलती सी छवि है।।
– (रसराज, अगस्त , 1958)
“किसान” की पूर्ति द्रष्टव्य है –
कभी ईंधन लाने की चिन्ता चढ़ी
कभी चिन्ता चढ़ी सर धान पिसान की।
कभी चिन्ता चढ़ी कही तेल की तो
कभी चिन्ता चढ़ी गृह के परिधान की।
जिसे देखिए चिन्ता विभूत वही
अधरों पे ना रेखा है मुस्कान की।
सुनता हूँ किसानों का राज्य हुआ
पर आंसू बहाती हैआंखे किसान की ।।
– (रसराज, जून , 1958)
समीक्षा: डा. मुनि लाल उपाध्याय ‘सरस’ जी द्वारा –
कन्दर्प नारायण जी चतुर्थ चरण के वरिष्ठ कवि हैं। इनकी साहित्यिक उपलब्धि इस चरण के लिए गौरव की वस्तु है। इनका दु:शासन और मृत्युंजया खण्ड काव्य उन्हें प्रबन्ध काव्य के रूप में उत्कृट सम्मान दिलाने में सक्षम है। खड़ी बोली के बहुशांसित कवि, छन्दकार , कन्दर्प जी के छन्दों में संस्कृत के तत्सम शब्दावली का एक और गांभीर्य है तो दूसरी और भावों का सरस प्रवाह । राष्ट्रसेवी व्यक्तित्व होने के कारण कविवर कंदर्प जी के सम्पूर्ण साहित्य में मानवीय संवेदनाएं अधिक उभरी हैं। यह जनपद के आधुनिक काव्य- धारा में वर्चस्वी छःन्दकार और सम्मानित कवि के रूप में प्रसंशित है।
(बस्ती के छंदकार भाग 3 से साभार)
लेखक परिचय:-
(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए सम सामयिक विषयों,साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं।
(मोबाइल नंबर +91 8630778321)
(वॉर्ड्सऐप नम्बर+919412300183)