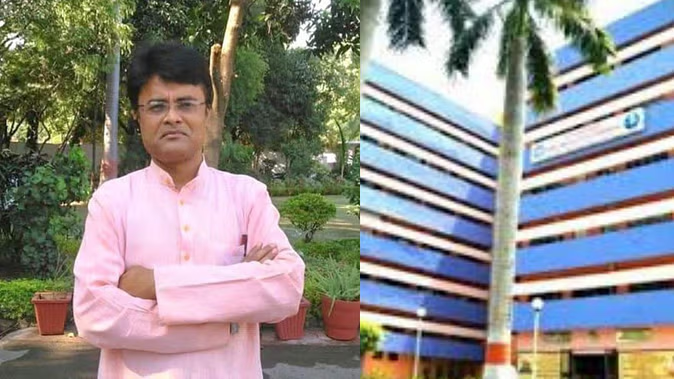कैलिफ़ोर्निया की एक कंपनी के एक ही स्रोत से लिए गए सुगंधित मसाले सदाजीविता के साथ ही भारतीय भोजन पाक कला और संस्कृति के बारे में समझ को विस्तार दे रहे हैं।
सना जावेरी कादरी द्वारा शुरू की गई डायस्पोरा कंपनी (इनसेट) गुलाबी लहुसन (ऊपर चित्र) जैसे खास स्वाद वाले मसालों के लिए सीधे किसानों के साथ काम करती है। कैलिफोर्निया में मुख्यालय वाली इस कंपनी द्वारा अमेरिका और अन्य स्थानों पर इन मसालों को उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाता है। (फोटोग्राफः साभार डायस्पोरा कंपनी)
सना जावेरी कादरी के लिए- प्रगति हल्दी, बिंदु काली सरसों और नंदिनी धनिया और अन्य दक्षिण एशियाई मसाले भोजन में स्वाद का तड़का लगाने भर वाले स्वादिष्ट पाउडर से बढ़कर हैं। कादरी मसालों की इस दुनिया को शानदार अंतरराष्ट्रीय कारोबार के अवसर के रूप में देखती हैं। कादरी डायस्पोरा कंपनी की संस्थापक और सीईओ हैं। इस कंपनी का मुख्यालय कैलिफ़ोर्निया में है और यह पूरे अमेरिका और उससे आगे, स्वादिष्ट मसालों को किसानों से सीधे खरीद कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है।
डायस्पोरा कंपनी हानिकारक रसायनों से रहित मसालों की बिक्री में निपुण है और कंपनी को इस बात का गर्व है कि वह बाजार में जाने से पहले हर फसल में संदूषण की सावधानी से जांच करती है।
इस कंपनी के मसाले एक ही स्रोत के होते हैं, जिसका मतलब है कि डायस्पोरा कंपनी की पैकेजिंग में आने वाली सभी धनिया, मिर्ची और सरसों की उपज एक ही खेत में हुई है। इस तरह से मसालों की खरीद से कादरी और उनकी टीम को हर मसाले की गुणवत्ता केअलावा यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि किसानों को उनके काम के लिए उचित भुगतान मिल सके। हर साल अपनी भारत यात्रा के दौरान कादरी निजी तौर किसानों से अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए हर उस खेत पर जाती हैं जिनके साथ उनकी कंपनी काम करती है। वह उनके खेतों की उपज के कारोबार के काम में उनके साथ निकटता से काम करती हैं और बिना कीटनाशकों के इस्तेमाल के मसालों के उत्पादन के तरीके खोजने में उनकी मदद करती हैं।
डायस्पोरा कंपनी के लिए मणिपुर में शिवथेई मिर्च उगाने वाले जिनोरिन एंगकांग ने 2021 में वोग पत्रिका के एक लेख में कहा, ‘‘सना ज्यादा लाभ का मार्जिन देती हैं। वह हमें एकमुश्त भुगतान करती हैं और साथ ही वह मिर्च के बीच रतालू, सोया और धान जैसी स्वदेशी खेती के तरीकों को भी अपनाती हैं।’’
डायस्पोरा कंपनी पूरे भारत से अपने मसाले मंगवाती है। कश्मीरी मिर्च और केसर उत्तर भारत से आते हैं, जबकि भारत के पूर्वी इलाकों से शिवथेई मिर्च और नगा पहाडि़यों से गुड़हल और दूसरी चीजें आती हैं। बिंदु काली सरसों देश के मध्य क्षेत्र से, बराका इलायची दक्षिण से जबकि नंदिनी धनिया पश्चिम से आता है।
इनके प्रयासों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और बड़े पैमाने पर प्रसंशा प्राप्त की है। फूड और वाइन ने डायस्पोरा कंपनी के बारे में लिखा है, ‘‘राशन की दुकानों में मिलने वाली हल्दी की तुलना अगर इस हल्दी से की जाए तो फर्क दिन और रात का है। आपको इस जैविक रूप से और एक ही स्रोत से ली गई हल्दी के बारे में जानने की जरूरत है।’’ वोग पत्रिका में तमार एडलर ने लिखा है, ‘‘डायस्पोरा कंपनी की प्रगति हल्दी इतनी सुगंध वाली है कि आप पर इसका नशा छा जाए। अरण्य कालीमिर्च पके हुए फल की तरह महकती है और स्वाद धुएं, चॉकलेट और संतरे की तरह महसूस होता है।’’ द इनफेचुएशन फूड वेबसाइट की समीक्षक डायना त्सुई लिखती हैं, ‘‘इन मसालों और आमतौर से सुपरमार्केट से खरीदे गए मसालों के स्वाद में बहुत अंतर होता है। इनका जायका यकीनन तेज होता है और बहुत कुछ उन पौधों जैसा ही होता है जहां से वे लाए जाते हैं।’’
कादरी ने स्पैन को बताया कि अहम प्रशंसा उत्साहवर्धक होती है सकारात्मक प्रचार के बिना कंपनी वहां नहीं होती, जहां आज खड़ी है- लेकिन कंपनी की उपलब्धियों की व्यापक प्रशंसा का गहरा महत्व भी है। वह कहती हैं, ‘‘अब हम अपने को संस्कृतियों के रुपातंरक, एक शिक्षक और दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम उत्पादक किसानों के प्रवक्ता के रूप में देखते हैं। यह सब हमारे मिशन की सेवा का हिस्सा है।’’ उनका कहना है, ‘‘अधिक दिखने का मतलब और अधिक बेहतर मसाले, अपने किसानों की और प्रभावी सेवा और यह हमारे लिए नॉर्थ स्टार है।’’
कादरी का जन्म मुंबई में हुआ और वह वहीं पली-बढ़ीं। 2012 में वह कैलिफोर्निया के पोमोना कॉलेज में फूड और विजुअल आर्ट के अध्ययन के लिए अमेरिका गईं। चार साल बाद, सैन फ्रांसिस्को स्थित एक ग्रॉसरी स्टोर में काम करते हुए कादरी को अमेरिकी खाद्य संस्कृति में हल्दी के इस्तेमाल के बढ़ते चलन का अहसास हुआ- खासतौर पर एक लोकप्रिय कॉफी पेय में इसके इस्तेमाल का। उनका ध्यान अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली हल्दी में मुंबई के मुकाबले बहुत कम खुशबू की तरफ भी गया। इस बारे में और जानकारी के लिए कादरी ने भारत लौटने का फैसला किया।
उन्होंने भारतीय खेतों में घूमते हुए महीनों बिताए और केरल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च में बातचीत की। वह इस मुलाकात को जीवन बदलने वाली घटना मानती हैं। उन्होंने 2017 में सिर्फ एक उत्पाद- प्रगति हल्दी के साथ डायस्पोरा की शुरुआत की -जिसे उन्होंने प्रभु कासरनेनी के एक ही खेत से लिया था।
कादरी लिखती हैं, ‘‘बड़ा स्वप्न अब निश्चित रूप से नए, स्वादिष्ट और वाकई उचित मसाला कारोबार के रूप में आगे बढ़ने लगा था।’’
डायस्पोरा कंपनी का विकास और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अपने आप में एक बानगी है। आज कंपनी में भारत के अलावा, अमेरिका, इंगलैंड और सऊदी अरब के एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। वे 150 से अधिक खेतों में उत्पादित दर्जनों किस्म के मसाले बेचते हैं।
कंपनी का जोर सदाजीवी एवं जैविक कृषि और किसानों से सीधा संपर्क बढ़ाने के अलावा रासायनिक प्रदूषण और मसाला कारोबार से आमतौर पर संबद्ध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर है। डायस्पोरा कंपनी की अमेरिका में बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय भोजन पकाने की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी और समझ को विकसित किया है। अमेरिका, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है।
कादरी के लिए, डायस्पोरा कंपनी की व्यापक सफलता एक खंडित अतीत के ज्ञान और एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ शुरू हुई। वह कंपनी की वेबसाइट पर लिखती हैं, ‘‘इस समुदाय में रहने का मतलब अपने उस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत के साथ गहराई से जुड़ना है, जहां से हम अपना उत्पाद मंगाते हैं और समय के साथ सीख हासिल करते रहे हैं।’’ वह लिखती हैं कि, ‘‘इससे मेड इन साउथ एशिया का मतलब जटिल और कहीं गहरा बन गया है, यह हमें तय करना है कि हम अपनी आजादी, अपने संघर्ष और भोजन के जरिए अपने डायस्पोरा की कहानी कैसे बयान करते हैं।’’
माइकल गलांट एक लेखक, संगीतकार और उद्यमी हैं और न्यू यॉर्क में रहते हैं।